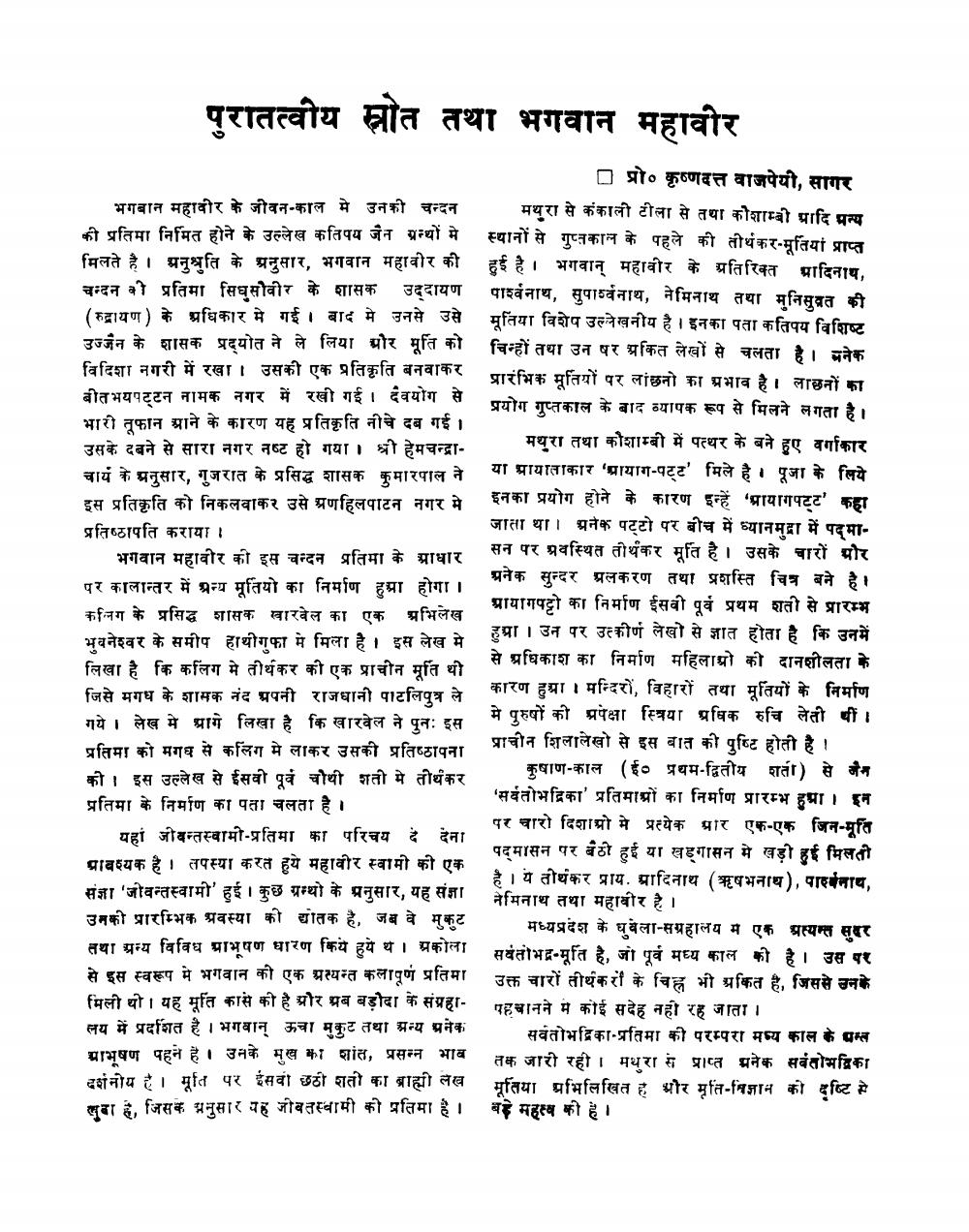________________
पुरातत्वीय स्रोत तथा भगवान महावीर
0 प्रो० कृष्णदत्त वाजपेयी, सागर भगवान महावीर के जीवन-काल में उनकी चन्दन मथुरा से कंकाली टीला से तथा कौशाम्बी प्रादि अन्य की प्रतिमा निर्मित होने के उल्लेख कतिपय जैन ग्रन्थों मे स्थानों से गुप्तकाल के पहले की तीर्थकर-मूर्तियां प्राप्त मिलते है। अनुश्रुति के अनुसार, भगवान महावीर की हुई है। भगवान् महावीर के अतिरिक्त प्रादिनाथ, चन्दन की प्रतिमा सिघसौवीर के शासक उद्दायण पार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ, नेमिनाथ तथा मनिसुव्रत की (रुद्रायण) के अधिकार मे गई। बाद में उनसे उसे मूर्तिया विशेष उल्लेखनीय है । इनका पता कतिपय विशिष्ट
शासक प्रदयोत ने ले लिया और मूर्ति को चिन्हों तथा उन पर अकित लेखों से चलता है। अनेक विदिशा नगरी में रखा। उसकी एक प्रतिकृति बनवाकर
प्रारंभिक मूर्तियों पर लांछनो का प्रभाव है। लाछनों का बीत भयपट्टन नामक नगर में रखी गई। देवयोग से
प्रयोग गुप्तकाल के बाद व्यापक रूप से मिलने लगता है। भारी तूफान आने के कारण यह प्रतिकृति नीचे दब गई। उसके दबने से सारा नगर नष्ट हो गया। श्री हेमचन्द्रा
मथुरा तथा कौशाम्बी में पत्थर के बने हुए वर्गाकार चार्य के अनुसार, गुजरात के प्रसिद्ध शासक कुमारपाल ने
या पायाताकार 'प्रायाग-पट्ट' मिले है। पूजा के लिये इस प्रतिकृति को निकलवाकर उसे अणहिलपाटन नगर मे
इनका प्रयोग होने के कारण इन्हें 'पायागपट्ट' कहा प्रतिष्ठापति कराया।
जाता था। अनेक पट्टो पर बीच में ध्यानमुद्रा में पदमाभगवान महावीर की इस चन्दन प्रतिमा के आधार
सन पर अवस्थित तीर्थंकर मूर्ति है। उसके चारों और
अनेक सुन्दर प्रलकरण तथा प्रशस्ति चित्र बने है। पर कालान्तर में अन्य मूर्तियो का निर्माण हुआ होगा।
प्रायागपट्रो का निर्माण ईसवी पूर्व प्रथम शती से प्रारम्भ कन्निग के प्रसिद्ध शासक खारवेल का एक अभिलेख
हुमा । उन पर उत्कीर्ण लेखो से ज्ञात होता है कि उनमें भुवनेश्वर के समीप हाथीगुफा में मिला है। इस लेख मे
से अधिकाश का निर्माण महिलामो की दानशीलता के लिखा है कि कलिंग मे तीर्थकर की एक प्राचीन मूर्ति थी जिसे मगध के शामक नंद अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले
कारण हया । मन्दिरों, विहारों तथा मूर्तियों के निर्माण गये । लेख मे आगे लिखा है कि खारवेल ने पुनः इस
मे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रिया अधिक रुचि लेती थीं।
प्राचीन शिलालेखो से इस बात की पुष्टि होती है। प्रतिमा को मगध से कलिंग मे लाकर उसकी प्रतिष्ठापना की। इस उल्लेख से ईसवी पूर्व चौथी शती मे तीर्थकर
कुषाण-काल (ई० प्रथम-द्वितीय शती) से जैन
'सर्वतोभद्रिका' प्रतिमानों का निर्माण प्रारम्भ हमा। इन प्रतिमा के निर्माण का पता चलता है।
पर चारो दिशामो मे प्रत्येक प्रार एक-एक जिन-मूर्ति यहां जीवन्तस्वामी-प्रतिमा का परिचय दे देना
पदमासन पर बैठी हुई या खड्गासन मे खड़ी हुई मिलती प्रावश्यक है। तपस्या करत हुये महावीर स्वामी की एक
है। ये तीर्थकर प्राय. प्रादिनाथ (ऋषभनाथ), पारनाथ, संज्ञा 'जीवन्तस्वामी' हुई। कुछ ग्रन्थो के अनुसार, यह संज्ञा
नेमिनाथ तथा महावीर है। उनकी प्रारम्भिक अवस्या को द्योतक है, जब वे मुकुट
मध्यप्रदेश के धुवेला-सग्रहालय में एक अत्यन्त सुबर तथा अन्य विविध प्राभूषण धारण किये हुये थे । अकोला
सर्वतोभद्र-मूति है, जो पूर्व मध्य काल की है। उस पर से इस स्वरूप में भगवान की एक अत्यन्त कलापूर्ण प्रतिमा उक्त चारों तीर्थकरी के चिह्न भी अकित है, जिससे उनके मिली थी। यह मूति कासे की है और प्रब बड़ौदा के संग्रहा- रचानने में कोई मटेड लय में प्रदर्शित है । भगवान् ऊचा मुकुट तथा अन्य अनेक
सर्वतोभद्रिका-प्रतिमा की परम्परा मध्य काल के पल माभषण पहने है। उनके मुख का शांत, प्रसन्न भाव तक जारी रही। मथरा से प्राप्त अनेक सर्वतोभद्रिका दर्शनीय है। मृति पर ईसवी छठी शती का ब्राह्मी लेख मतिया अभिलिखित है और मृति-विज्ञान को दष्टि से लवा. जिसके अनुसार यह जीवतस्वामी की प्रतिमा है। बड़े महत्व की है।