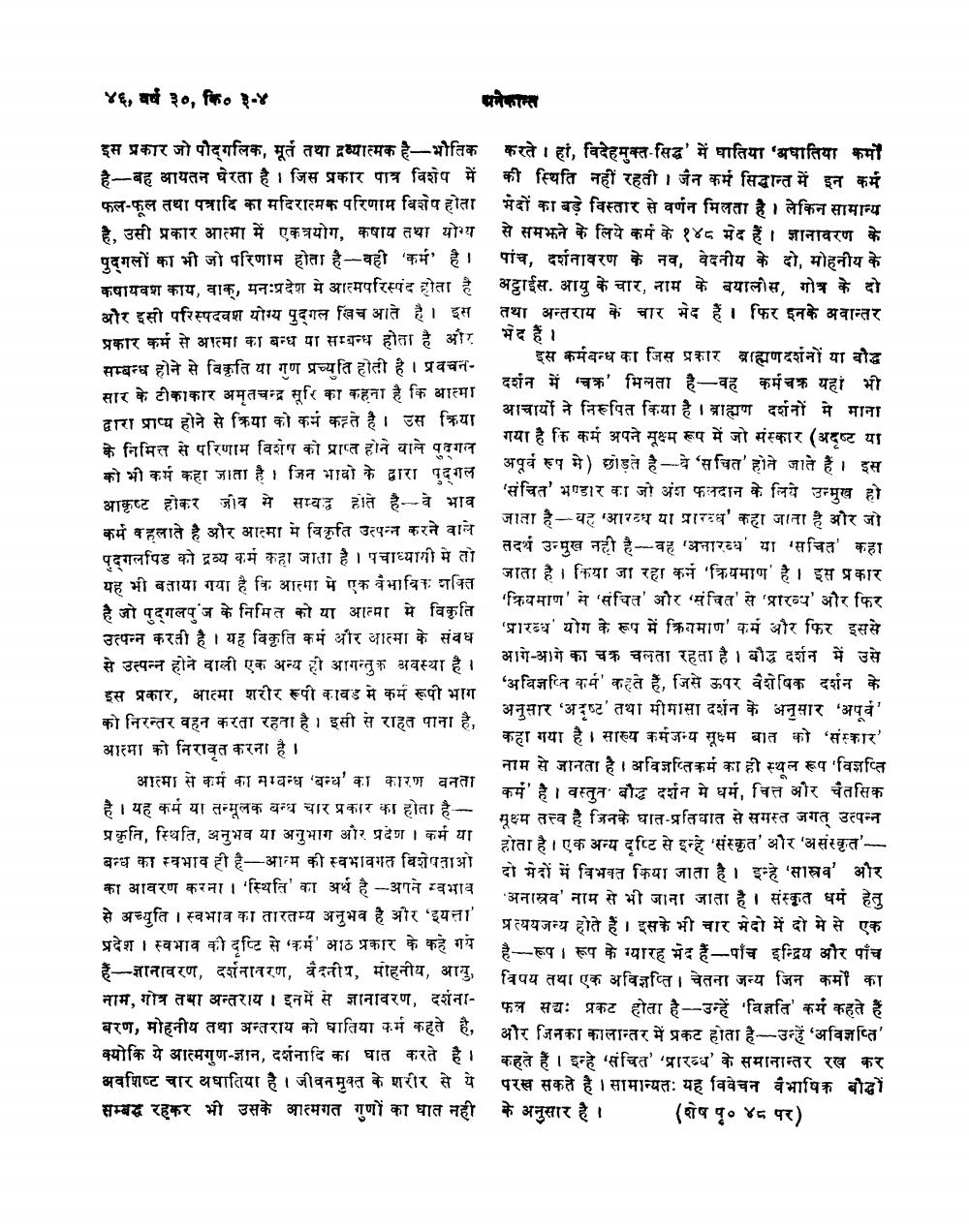________________
४६, वर्ष ३०, कि० ३-४
इस प्रकार जो पौद्गलिक, मूर्त तथा द्रव्यात्मक है-भौतिक करते । हां, विदेहमुक्त-सिद्ध' में घातिया 'अधातिया को है-बह आयतन घेरता है । जिस प्रकार पात्र विशेष में की स्थिति नहीं रहती। जैन कर्म सिद्धान्त में इन कर्म फल-फूल तथा पत्रादि का मदिरात्मक परिणाम विशेष होता भेदों का बड़े विस्तार से वर्णन मिलता है। लेकिन सामान्य है, उसी प्रकार आत्मा में एकत्रयोग, कषाय तथा योग्य से समझने के लिये कर्म के १४८ मेद हैं। ज्ञानावरण के पदगलों का भी जो परिणाम होता है-वही 'कर्म' है। पांच, दर्शनावरण के नव, वेदनीय के दो, मोहनीय के कषायवश काय, वाक्, मनःप्रदेश मे आत्मपरिस्पंद होता है अट्ठाईस. आयु के चार, नाम के बयालीस, गोत्र के दो
और इसी परिस्पदवश योग्य पुद्गल खिच आते है। इस तथा अन्तराय के चार भेद हैं। फिर इनके अवान्तर प्रकार कर्म से आत्मा का बन्ध या सम्बन्ध होता है और भेद हैं।
इस कर्मबन्ध का जिस प्रकार ब्राह्मणदर्शनों या बौद्ध सम्बन्ध होने से विकृति या गण प्रच्यति होती है । प्रवचन
दर्शन में 'चक्र' मिलता है-वह कर्मचक्र यहां भी सार के टीकाकार अमृतचन्द्र सूरि का कहना है कि आत्मा
आचार्यों ने निरूपित किया है । ब्राह्मण दर्शनों में माना द्वारा प्राप्य होने से क्रिया को कर्म कहते है। उस क्रिया
गया है कि कर्म अपने मूक्ष्म रूप में जो संस्कार (अदृष्ट या के निमित्त से परिणाम विशेष को प्राप्त होने वाले पदगल
अपूर्व रूप मे) छोड़ते है--वे 'सचित' होते जाते हैं। इस को भी कर्म कहा जाता है। जिन भादो के द्वारा पद्गल
'संचित' भण्डार का जो अंश फलदान के लिये उन्मुख हो आकृष्ट होकर जीव मे सम्बद्ध होते है-वे भाव
जाता है-वह 'आरब्ध या प्रारब्ध' कहा जाता है और जो कर्म कहलाते है और आत्मा में विकृति उत्पन्न करने वाले
तदर्थ उन्मुख नहीं है-वह 'अनारब्ध' या 'सचित' कहा पद्गलपिड को द्रव्य कर्म कहा जाता है। पचाध्यायी मे तो
जाता है। किया जा रहा कनं 'क्रियमाण' है। इस प्रकार यह भी बताया गया है कि आत्मा मे एक वैभाविक शक्ति
'क्रियमाण' से 'संचित' और 'संचित' से 'प्रारम्प' और फिर है जो पगलपुज के निमित को या आत्मा मे विकृति
'प्रारब्ध' योग के रूप में क्रियमाण' कर्म और फिर इससे उत्पन्न करती है । यह विकृति कर्म और आत्मा के संबंध से उत्पन्न होने वाली एक अन्य ही आगन्तुक अवस्था है।
आगे-आगे का चक्र चलता रहता है । बौद्ध दर्शन में उसे
'अविज्ञप्ति कर्म' कहते हैं, जिसे ऊपर वैशेषिक दर्शन के इस प्रकार, आत्मा शरीर रूपी कावड में कम रूपी भाग
अनुसार 'अदष्ट' तथा मीमासा दर्शन के अनुसार 'अपर्व' को निरन्तर वहन करता रहता है। इसी से राहत पाना है,
कहा गया है। साख्य कर्मजन्य सूक्ष्म बात को 'संस्कार' आत्मा को निरावृत करना है।
नाम से जानता है । अविज्ञप्तिकर्म का ही स्थल रूप 'विज्ञप्ति ____ आत्मा से कर्म का मम्वन्ध 'बन्ध' का कारण बनता
कर्म' है। वस्तुतः बौद्ध दर्शन मे धर्म, चित्त और चैतसिक है। यह कर्म या तन्मूलक बन्ध चार प्रकार का होता है
सूक्ष्म तत्त्व है जिनके घात-प्रतिवात से समस्त जगत् उत्पन्न प्रकृति, स्थिति, अनुभव या अनुभाग और प्रदेश । कर्म या
होता है। एक अन्य दृष्टि से इन्हे 'संस्कृत' और 'असंस्कृत'बन्ध का स्वभाव ही है-आन्म की स्वभावगत विशेषताओ
दो भेदों में विभक्त किया जाता है। इन्हे 'सासव' और का आवरण करना । 'स्थिति' का अर्थ है -अपने स्वभाव
'अनास्रव' नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत धर्म हेतु से अच्युति । स्वभाव का तारतम्य अनुभव है और 'इयत्ता'
प्रत्ययजन्य होते हैं। इसके भी चार भेदो में दो मे से एक प्रदेश । स्वभाव की दृष्टि से 'कर्म' आठ प्रकार के कहे गये
है-रूप । रूप के ग्यारह भेद हैं-पाँच इन्द्रिय और पाँच ह-शानावरण, दशनावरण, वदनाथ, माहनाय, आयु, विषय तथा एक अविज्ञप्ति । चेतना जन्य जिन कर्मों का नाम, गोत्र तथा अन्तराय । इनमें से ज्ञानावरण, दर्शना
फल सद्यः प्रकट होता है--उन्हें 'विज्ञति' कर्म कहते हैं बरण, मोहनीय तथा अन्तराय को घातिया कर्म कहते है, और जिनका
होता है जो अविति' क्योकि ये आत्मगुण-ज्ञान, दर्शनादि का घात करते है। कहते हैं। इन्हे 'संचित' 'प्रारब्ध' के समानान्तर रख कर अवशिष्ट चार बघातिया है। जीवनमुक्त के शरीर से ये परख सकते है । सामान्यतः यह विवेचन वैभाषिक बौद्धों सम्बद्ध रहकर भी उसके आत्मगत गुणों का घात नही के अनुसार है। (शेष पृ० ४८ पर)