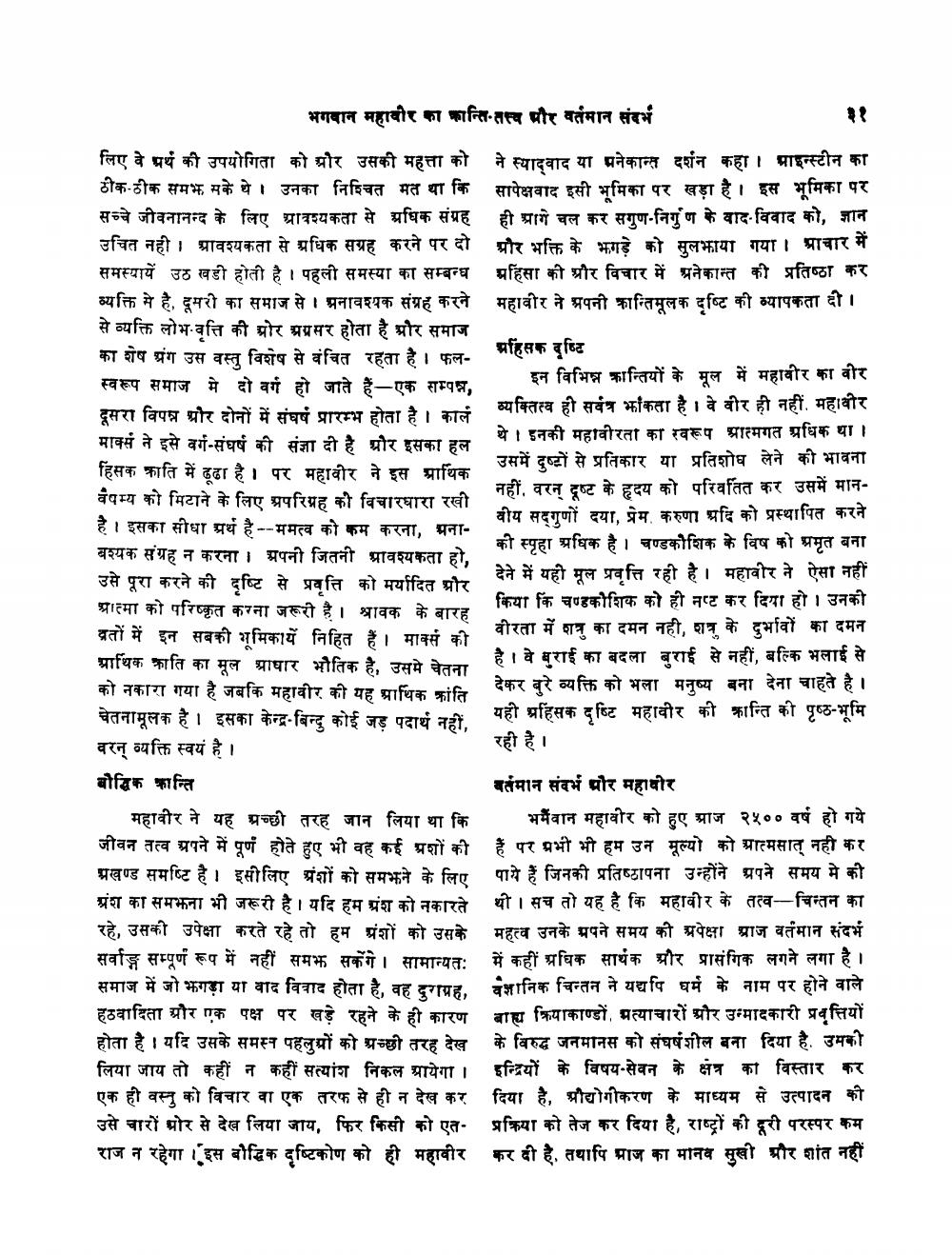________________
भगवान महावीर का कान्ति-तस्वीर वर्तमान संदर्भ
लिए वे प्रर्थ की उपयोगिता को और उसकी महत्ता को ने स्यादवाद या भनेकान्त दर्शन कहा। माइन्स्टीन का ठीक-ठीक समझ सके थे। उनका निश्चित मत था कि सापेक्षवाद इसी भूमिका पर खड़ा है। इस भूमिका पर सच्चे जीवनानन्द के लिए आवश्यकता से अधिक संग्रह ही आगे चल कर सगुण-निर्गुण के वाद-विवाद को, ज्ञान उचित नही। अावश्यकता से अधिक सग्रह करने पर दो और भक्ति के झगडे को सुलझाया गया। प्राचार में समस्यायें उठ खडी होती है। पहली समस्या का सम्बन्ध अहिंसा की और विचार में अनेकान्त की प्रतिष्ठा कर व्यक्ति मे है, दूसरी का समाज से । अनावश्यक संग्रह करने महावीर ने अपनी क्रान्तिमूलक दृष्टि की व्यापकता दी। से व्यक्ति लोभ-वृत्ति की ओर अग्रसर होता है और समाज का शेष अंग उस वस्तु विशेष से वंचित रहता है। फल
अहिंसक दृष्टि स्वरूप समाज मे दो वर्ग हो जाते हैं-एक सम्पन्न,
इन विभिन्न क्रान्तियों के मूल में महावीर का वीर दूसरा विपन्न और दोनों में संघर्ष प्रारम्भ होता है। कार्ल
व्यक्तित्व ही सर्वत्र झांकता है। वे वीर ही नहीं. महावीर मास ने इसे वर्ग-संघर्ष की संज्ञा दी है और इसका हल
थे। इनकी महावीरता का स्वरूप प्रात्मगत अधिक था। हिंसक क्राति में ढढा है। पर महावीर ने इस प्राथिक
उसमें दुष्टों से प्रतिकार या प्रतिशोध लेने की भावना वैषम्य को मिटाने के लिए अपरिग्रह की विचारधारा रखी
नहीं. वरन् दूष्ट के हृदय को परिवर्तित कर उसमें मानहै। इसका सीधा अर्थ है --ममत्व को कम करना, अना
वीय सद्गुणों दया, प्रेम करुणा अदि को प्रस्थापित करने बश्यक संग्रह न करना। अपनी जितनी प्रावश्यकता हो,
की स्पृहा अधिक है। चण्डकौशिक के विष को अमृत बना उसे पूरा करने की दृष्टि से प्रवृत्ति को मर्यादित और
देने में यही मूल प्रवृत्ति रही है। महावीर ने ऐसा नहीं प्रात्मा को परिष्कृत करना जरूरी है। श्रावक के बारह
किया कि चण्डकौशिक को ही नष्ट कर दिया हो। उनकी व्रतों में इन सबकी भूमिकायें निहित हैं। मार्क्स की
वीरता में शत्रु का दमन नही, शत्रु के दुर्भावों का दमन आर्थिक क्राति का मूल आधार भौतिक है, उसमे चेतना
है । वे बुराई का बदला बुराई से नहीं, बल्कि भलाई से को नकारा गया है जबकि महावीर की यह पार्थिक क्रांति
देकर बुरे व्यक्ति को भला मनुष्य बना देना चाहते है। चेतनामूलक है। इसका केन्द्र-बिन्दु कोई जड़ पदार्थ नहीं,
यही अहिंसक दृष्टि महावीर की क्रान्ति की पृष्ठ-भूमि वरन् व्यक्ति स्वयं है।
रही है। बौद्धिक क्रान्ति
वर्तमान संदर्भ और महावीर महावीर ने यह अच्छी तरह जान लिया था कि भमैवान महावीर को हुए आज २५०० वर्ष हो गये जीवन तत्व अपने में पूर्ण होते हुए भी वह कई प्रशों की हैं पर अभी भी हम उन मूल्यो को प्रात्मसात् नही कर प्रखण्ड समष्टि है। इसीलिए अंशों को समझने के लिए पाये हैं जिनकी प्रतिष्ठापना उन्होंने अपने समय में की अंश का समझना भी जरूरी है। यदि हम ग्रंश को नकारते थी। सच तो यह है कि महावीर के तत्व-चिन्तन का रहे, उसकी उपेक्षा करते रहे तो हम अंशों को उसके महत्व उनके अपने समय की अपेक्षा प्राज वर्तमान संदर्भ सर्वाङ्ग सम्पूर्ण रूप में नहीं समझ सकेंगे। सामान्यत: में कहीं अधिक सार्थक और प्रासंगिक लगने लगा है। समाज में जो झगड़ा या वाद विवाद होता है, वह दुराग्रह वज्ञानिक चिन्तन ने यद्यपि धर्म के नाम पर होने वाले हठवादिता और एक पक्ष पर खड़े रहने के ही कारण बाह्य क्रियाकाण्डों, अत्याचारों और उन्मादकारी प्रवृत्तियों होता है। यदि उसके समस्त पहलमों को अच्छी तरह देख के विरुद्ध जनमानस को संघर्षशील बना दिया है. उमकी लिया जाय तो कहीं न कहीं सत्यांश निकल पायेगा। इन्द्रियों के विषय-सेवन के क्षेत्र का विस्तार कर एक ही वस्तु को विचार वा एक तरफ से ही न देख कर दिया है, औद्योगीकरण के माध्यम से उत्पादन की उसे चारों ओर से देख लिया जाय, फिर किसी को एत- प्रक्रिया को तेज कर दिया है, राष्ट्रों की दूरी परस्पर कम राज न रहेगा। इस बौद्धिक दृष्टिकोण को ही महावीर कर दी है, तथापि प्राज का मानव सुखी और शांत नहीं