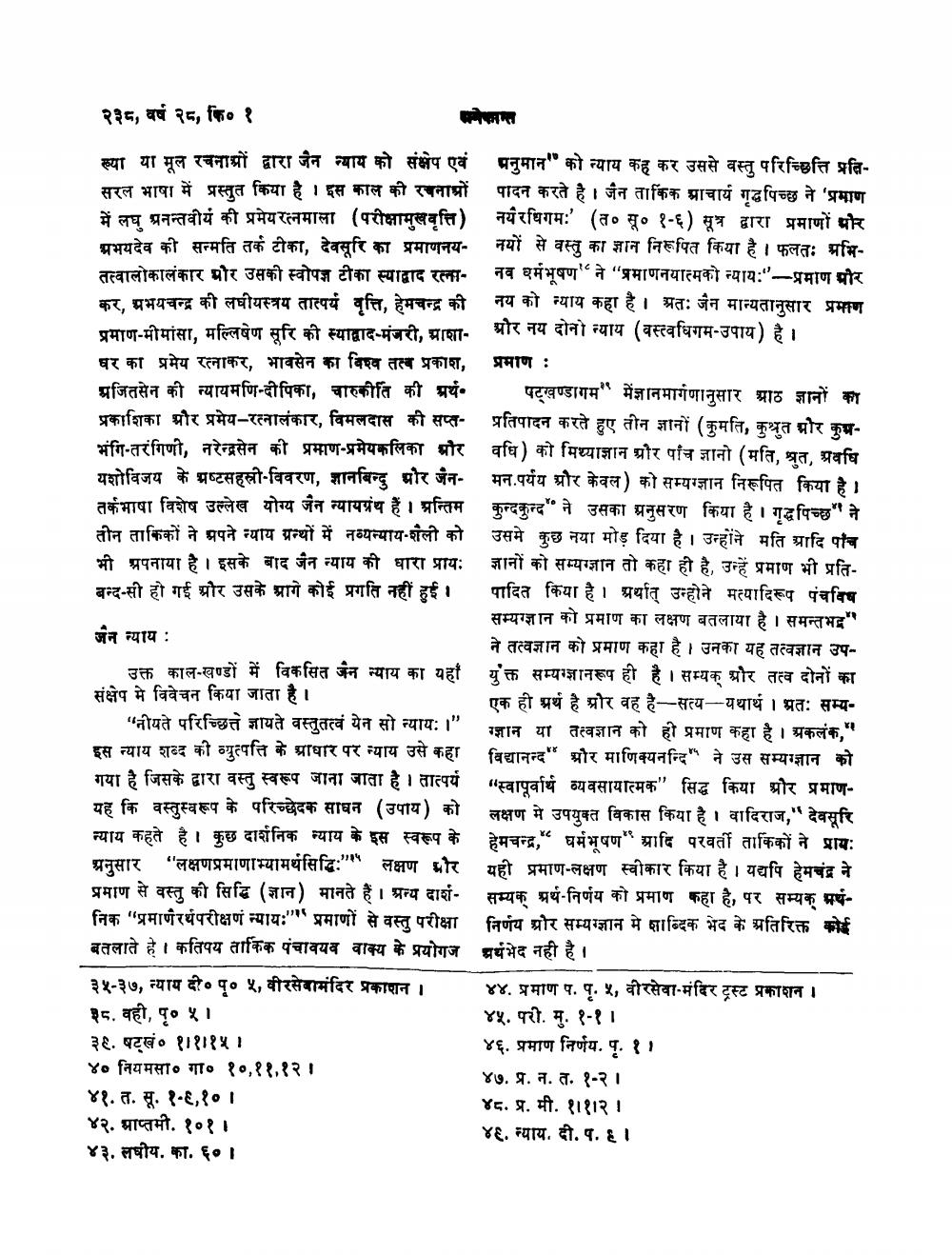________________
२३८, वर्ष २८, कि.१
ख्या या मूल रचनाओं द्वारा जैन न्याय को संक्षेप एवं अनुमान" को न्याय कह कर उससे वस्तु परिच्छित्ति प्रतिसरल भाषा में प्रस्तुत किया है । इस काल की रचनाओं पादन करते है । जैन तार्किक प्राचार्य गद्धपिच्छ ने 'प्रमाण में लय अनन्तवीर्य की प्रमेयरत्नमाला (परीक्षामुखवृत्ति) नयैरधिगमः' (त० सू० १-६) सूत्र द्वारा प्रमाणों और अभयदेव की सन्मति तर्क टीका, देवसूरि का प्रमाणनय- नयों से वस्तु का ज्ञान निरूपित किया है। फलतः अभितत्वालोकालंकार और उसकी स्वोपज्ञ टीका स्याद्वाद रत्ना- नव धर्मभूषण" ने "प्रमाणनयात्मको न्याय:"-प्रमाण पोर कर, अभयचन्द्र की लघीयस्त्रय तात्पर्य वृत्ति, हेमचन्द्र की नय को न्याय कहा है। अतः जैन मान्यतानुसार प्रमाण प्रमाण-मीमांसा, मल्लिषेण सूरि की स्याद्वाद-मंजरी, माशा- और नय दोनो न्याय (वस्त्वधिगम-उपाय) है। घर का प्रमेय रत्नाकर, भावसेन का विश्व तत्व प्रकाश, प्रमाण : प्रजितसेन की न्यायमणि-दीपिका, चारुकीति की अर्थ- पट्खण्डागम" मेंज्ञानमार्गणानुसार पाठ ज्ञानों का प्रकाशिका और प्रमेय-रत्नालंकार, विमलदास की सप्त- प्रतिपादन करते हुए तीन ज्ञानों (कूमति, कुथुत पोर कुमभंगि-तरंगिणी, नरेन्द्रसेन की प्रमाण-प्रमेयकलिका और वधि) को मिथ्याज्ञान और पांच ज्ञानो (मति, श्रत, अवधि यशोविजय के प्रष्टसहस्री-विवरण, ज्ञानबिन्दु और जैन- मन.पर्यय और केवल) को सम्यग्ज्ञान निरूपित किया है। तर्कभाषा विशेष उल्लेख योग्य जैन न्यायग्रंथ हैं । अन्तिम कुन्दकुन्द ने उसका अनुसरण किया है । गद्धपिच्छ" ने तीन ताकिकों ने अपने न्याय ग्रन्थों में नव्यन्याय-शैली को उसमे कुछ नया मोड़ दिया है। उन्होंने मति प्रादि पांच भी अपनाया है। इसके बाद जैन न्याय की धारा प्रायः ज्ञानों को सम्यग्ज्ञान तो कहा ही है, उन्हें प्रमाण भी प्रतिबन्द-सी हो गई और उसके आगे कोई प्रगति नहीं हुई। पादित किया है। अर्थात् उन्होने मत्यादिरूप पंचविध
सम्यग्ज्ञान को प्रमाण का लक्षण बतलाया है । समन्तभद्र" जैन न्याय :
ने तत्वज्ञान को प्रमाण कहा है। उनका यह तत्वज्ञान उपउक्त काल-खण्डों में विकसित जैन न्याय का यहाँ युक्त सम्यग्ज्ञानरूप ही है। सम्यक् और तत्व दोनों का संक्षेप मे विवेचन किया जाता है।
एक ही अर्थ है और वह है-सत्य-यथार्थ । अतः सम्यनीयते परिच्छित्ते ज्ञायते वस्तुतत्वं येन सो न्यायः ।" रज्ञान या तत्वज्ञान को ही प्रमाण कहा है । अकलंक," इस न्याय शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर न्याय उसे कहा विद्यानन्द" और माणिक्यनन्दि" ने उस सम्यग्ज्ञान को गया है जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप जाना जाता है । तात्पर्य "स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मक" सिद्ध किया और प्रमाणयह कि वस्तुस्वरूप के परिच्छेदक साधन (उपाय) को लक्षण मे उपयुक्त विकास किया है। वादिराज," देवसरि न्याय कहते है। कुछ दार्शनिक न्याय के इस स्वरूप के हेमचन्द्र, धर्मभूषण" प्रादि परवर्ती ताकिकों ने प्रायः अनुसार "लक्षणप्रमाणाभ्यामर्थसिद्धिः" लक्षण और यही प्रमाण-लक्षण स्वीकार किया है । यद्यपि हेमचंद्र ने प्रमाण से वस्तु की सिद्धि (ज्ञान) मानते हैं । अन्य दार्श- सम्यक् अर्थ-निर्णय को प्रमाण कहा है, पर सम्यक् अर्थनिक "प्रमाणरर्थपरीक्षणं न्यायः" प्रमाणों से वस्तु परीक्षा निर्णय और सम्यग्ज्ञान मे शाब्दिक भेद के अतिरिक्त कोई बतलाते है । कतिपय तार्किक पंचावयव वाक्य के प्रयोगज अर्थभेद नही है। ३५-३७, न्याय दी० पृ० ५, वीरसेवामंदिर प्रकाशन । ४४. प्रमाण प. पृ. ५, वीरसेवा-मंदिर ट्रस्ट प्रकाशन । ३८. वही, पृ० ५।
४५. परी. मु. १-१ । ३६. षट्खं० १४१०१५।
४६. प्रमाण निर्णय. पृ. १। ४० नियमसा० गा० १०,११,१२ ।
४७. प्र. न. त. १-२। ४१. त. सू. १.६,१०।
४८. प्र. मी. ११११२। ४२. प्राप्तमी. १०१।
४६. न्याय. दी.प.ई। ४३. लघीय. का. ६०।