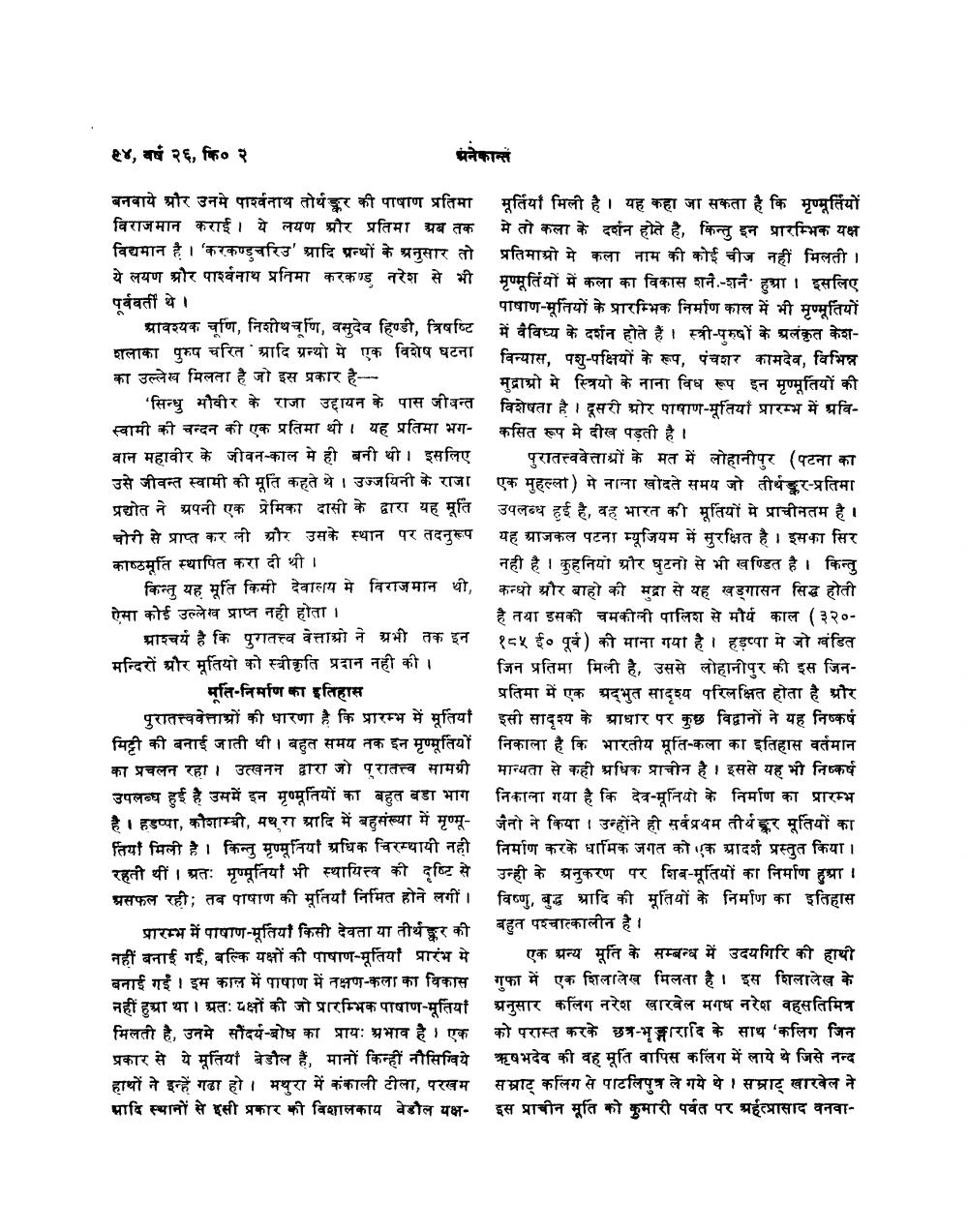________________
९४, वर्ष २६, कि०२
अनेकान्त
बनवाये और उनमे पार्श्वनाथ तोर्थङ्कर की पाषाण प्रतिमा मूर्तियां मिली है। यह कहा जा सकता है कि मृण्मूर्तियों विराजमान कराई। ये लयण और प्रतिमा अब तक मे तो कला के दर्शन होते है, किन्तु इन प्रारम्भिक यक्ष विद्यमान है । 'करकण्डुचरिउ' आदि प्रन्थों के अनुसार तो प्रतिमानो मे कला नाम की कोई चीज नहीं मिलती। ये लयण और पार्श्वनाथ प्रतिमा करकण्ड नरेश से भी मृणमूर्तियों में कला का विकास शन.-शन हुआ। इसलिए पूर्ववर्ती थे।
पाषाण-मूर्तियों के प्रारम्भिक निर्माण काल में भी मृण्मूर्तियों पावश्यक चूणि, निशीथचणि, वसुदेव हिण्डी, त्रिषष्टि में वैविध्य के दर्शन होते हैं। स्त्री-पुरुषों के अलंकृत केशशलाका पुरुष चरित 'अादि ग्रन्थो मे एक विशेष घटना विन्यास. पश-पक्षियों के रूप पंचार कामदेव विभिन्न का उल्लेख मिलता है जो इस प्रकार है
मुद्रानो मे स्त्रियो के नाना विध रूप इन मृण्मूर्तियों की 'सिन्धु मौवीर के राजा उद्दायन के पास जीवन्त विशेषता है। दूसरी ओर पाषाण-मतियाँ प्रारम्भ में प्रविस्वामी की चन्दन की एक प्रतिमा थी। यह प्रतिमा भग- कसित रूप मे दीख पड़ती है। वान महावीर के जीवन-काल मे ही बनी थी। इसलिए पुरातत्त्ववेत्तात्रों के मत में लोहानीपुर (पटना का उसे जीवन्त स्वामी की मूर्ति कहते थे । उज्जयिनी के राजा एक मुहल्ला) मे नाला खोदते समय जो तीर्थङ्कर-प्रतिमा प्रद्योत ने अपनी एक प्रेमिका दासी के द्वारा यह मूर्ति उपलब्ध हुई है, वह भारत की मूर्तियों में प्राचीनतम है । चोरी से प्राप्त कर ली और उसके स्थान पर तदनुरूप यह आजकल पटना म्यूजियम में सुरक्षित है। इसका सिर काष्ठमूर्ति स्थापित करा दी थी।
नही है । कुहनियों और घुटनो से भी खण्डित है। किन्तु किन्तु यह मूर्ति किमी देवालय में विराजमान थी,
कन्धो और बाहो की मुद्रा से यह खड्गासन सिद्ध होती ऐसा कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता।
है तथा इसकी चमकीली पालिश से मौर्य काल (३२०प्राश्चर्य है कि पूरातत्त्व वेत्तानो ने अभी तक इन १८५ ई०पूर्व) की माना गया है। हड़प्पा मे जो खंडित मन्दिरों और मूर्तियो को स्वीकृति प्रदान नहीं की।
जिन प्रतिमा मिली है, उससे लोहानीपुर की इस जिनमूति-निर्माण का इतिहास
प्रतिमा में एक अद्भुत सादृश्य परिलक्षित होता है और पुरातत्त्ववेत्ताओं की धारणा है कि प्रारम्भ में मूर्तियाँ इसी सादृश्य के आधार पर कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्ष मिट्टी की बनाई जाती थी। बहुत समय तक इन मृण्मूर्तियों निकाला है कि भारतीय मूर्ति-कला का इतिहास वर्तमान का प्रचलन रहा। उत्खनन द्वारा जो पुरातत्त्व सामग्री मान्यता से कही अधिक प्राचीन है । इससे यह भी निष्कर्ष उपलब्ध हुई है उसमें इन मृण्मूर्तियों का बहुत बडा भाग निकाला गया है कि देव-मूर्तियो के निर्माण का प्रारम्भ है। हडप्पा, कौशाम्बी, मथुरा आदि में बहुसंख्या में मृण्मू- जैनो ने किया। उन्होंने ही सर्वप्रथम तीर्थर मूर्तियों का तियां मिली है। किन्तु मृण्मूर्तियां अधिक चिरस्थायी नही निर्माण करके धार्मिक जगत को एक आदर्श प्रस्तुत किया। रहती थीं । अतः मृणमूर्तियां भी स्थायित्त्व की दृष्टि से उन्ही के अनुकरण पर शिब-मूर्तियों का निर्माण हुआ । असफल रही; तब पाषाण की मूर्तियां निर्मित होने लगीं। विष्णु, बुद्ध आदि की मूर्तियों के निर्माण का इतिहास
प्रारम्भ में पाषाण-मूर्तियां किसी देवता या तीर्थकर की बहुत पश्चात्कालीन है। नहीं बनाई गई, बल्कि यक्षों की पाषाण-मूर्तियां प्रारंभ मे एक अन्य मूर्ति के सम्बन्ध में उदयगिरि की हाथी बनाई गई। इस काल में पाषाण में तक्षण-कला का विकास गुफा में एक शिलालेख मिलता है। इस शिलालेख के नहीं हुआ था। अतः यक्षों की जो प्रारम्भिक पाषाण-मूर्तियाँ अनुसार कलिंग नरेश खारवेल मगध नरेश वहसतिमित्र मिलती है, उनमे सौंदर्य-बोध का प्रायः प्रभाव है। एक को परास्त करके छत्र-भृङ्गारादि के साथ 'कलिग जिन प्रकार से ये मूर्तियां बेडौल हैं, मानों किन्हीं नौसिग्विये ऋषभदेव की वह मूर्ति वापिस कलिंग में लाये थे जिसे नन्द हाथों ने इन्हें गढा हो। मथुरा में कंकाली टीला, परखम सम्राट् कलिंग से पाटलिपुत्र ले गये थे । सम्राट् खारवेल ने मादि स्थानों से इसी प्रकार की विशालकाय बेडौल यक्ष- इस प्राचीन मूर्ति को कुमारी पर्वत पर महत्प्रासाद वनवा
तहास