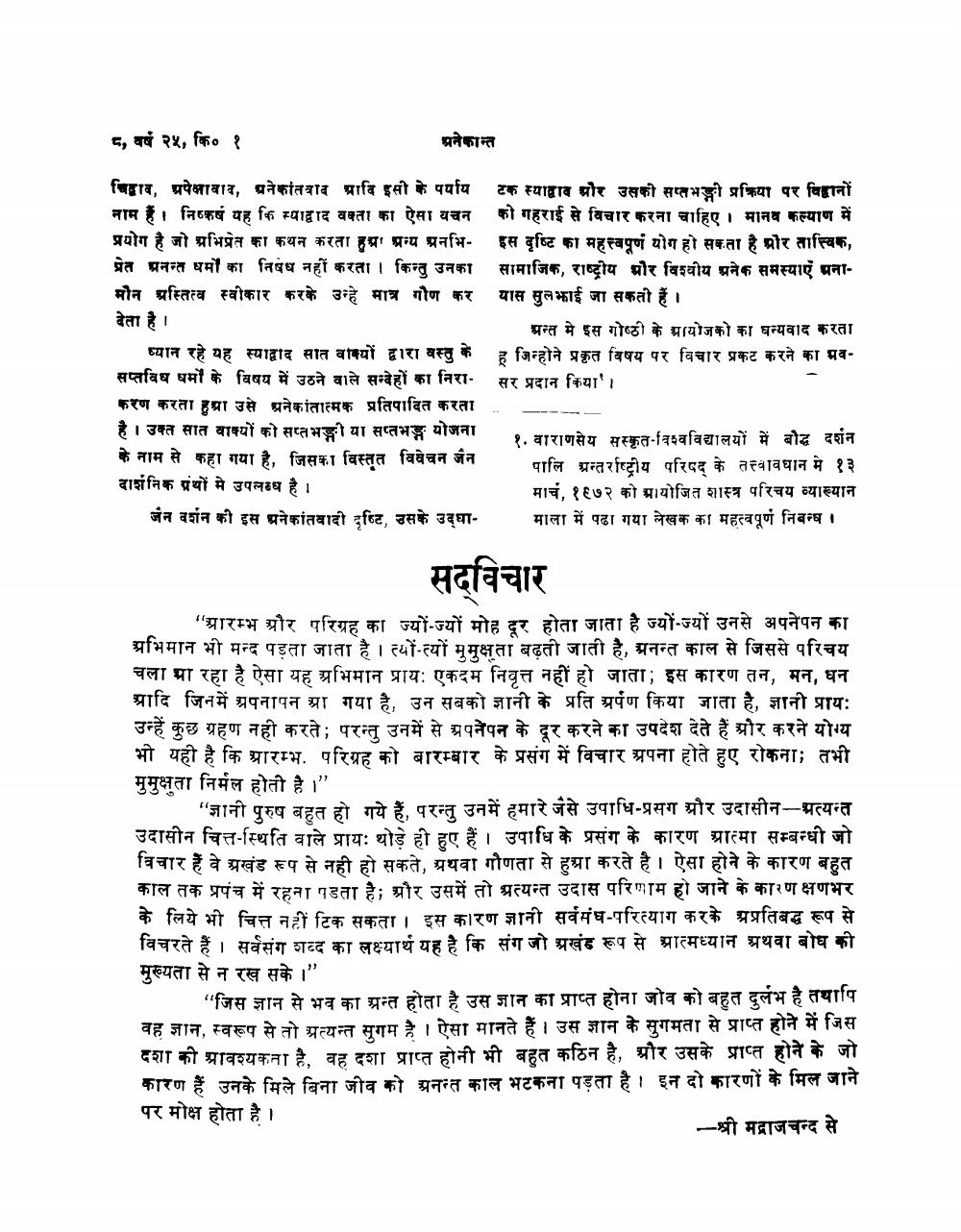________________
८ वर्ष २५, कि०१
अनेकान्त
चिहाव, अपेक्षावाद, अनेकांतवाद प्रादि इसी के पर्याय टक स्यावाव और उसको सप्तभती प्रक्रिया पर विद्वानों नाम हैं। निष्कर्ष यह कि स्याद्वाद वक्ता का ऐसा वचन को गहराई से विचार करना चाहिए। मानव कल्याण में प्रयोग है जो अभिप्रेत का कथन करता हुमा अन्य अनभि- इस दृष्टि का महत्वपूर्ण योग हो सकता है और तात्त्विक, प्रेत अनन्त धर्मों का निषध नहीं करता। किन्तु उनका सामाजिक, राष्ट्रीय और विश्वीय अनेक समस्याएँ प्रनामौन अस्तित्व स्वीकार करके उन्हे मात्र गौण कर यास सुलझाई जा सकती हैं। देता है।
अन्त मे इस गोष्ठी के आयोजको का धन्यवाद करता ध्यान रहे यह स्याद्वाद सात वाक्यों द्वारा वस्तु के ह जिन्होने प्रकृत विषय पर विचार प्रकट करने का प्रव. सप्तविध धर्मों के विषय में उठने वाले सन्वेहों का निरा- सर प्रदान किया। करण करता हुमा उसे अनेकांतात्मक प्रतिपादित करता ... है । उक्त सात वाक्यों को सप्तभङ्गी या सप्तभङ्ग योजना
१. वाराणसेय सस्कृत-विश्वविद्यालयों में बौद्ध दर्शन के नाम से कहा गया है, जिसका विस्तृत विवेचन जैन
पालि अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् के तत्वावधान मे १३ दार्शनिक ग्रंथों मे उपलब्ध है।
मार्च, १९७२ को प्रायोजित शास्त्र परिचय व्याख्यान जैन वर्शन की इस अनेकांतवादी दृष्टि, उसके उद्घा- माला में पढ़ा गया लेखक का महत्वपूर्ण निबन्ध ।
सदविचार "प्रारम्भ और परिग्रह का ज्यों-ज्यों मोह दूर होता जाता है ज्यों-ज्यों उनसे अपनेपन का अभिमान भी मन्द पड़ता जाता है । त्यों-त्यों मुमुक्षता बढ़ती जाती है, अनन्त काल से जिससे परिचय चला मा रहा है ऐसा यह अभिमान प्राय: एकदम निवृत्त नहीं हो जाता; इस कारण तन, मन, धन प्रादि जिनमें अपनापन आ गया है, उन सबको ज्ञानी के प्रति अर्पण किया जाता है, ज्ञानी प्रायः उन्हें कुछ ग्रहण नही करते; परन्तु उनमें से अपनेपन के दूर करने का उपदेश देते हैं और करने योग्य भी यही है कि प्रारम्भ. परिग्रह को बारम्बार के प्रसंग में विचार अपना होते हुए रोकना; तभी मुमुक्षुता निर्मल होती है।"
_ "ज्ञानी पुरुष बहुत हो गये हैं, परन्तु उनमें हमारे जैसे उपाधि-प्रसग और उदासीन-अत्यन्त उदासीन चित्त-स्थिति वाले प्रायः थोडे ही हए हैं। उपाधि के प्रसंग के कारण प्रात्मा सम्बन्धी जो विचार हैं वे अखंड रूप से नही हो सकते, अथवा गौणता से हुआ करते है। ऐसा होने के कारण बहुत काल तक प्रपंच में रहना पड़ता है। और उसमें तो अत्यन्त उदास परिणाम हो जाने के कारण क्षणभर के लिये भी चित्त नहीं टिक सकता। इस कारण ज्ञानी सर्वसंध-परित्याग करके अप्रतिबद्ध रूप से विचरते हैं। सर्वसंग शब्द का लक्ष्यार्थ यह है कि संग जो अखंड रूप से प्रात्मध्यान अथवा बोध की मुख्यता से न रख सके।"
"जिस ज्ञान से भव का अन्त होता है उस ज्ञान का प्राप्त होना जोव को बहुत दुर्लभ है तथापि वह ज्ञान, स्वरूप से तो अत्यन्त संगम है । ऐसा मानते हैं। उस ज्ञान के सुगमता से प्राप्त होने में जिस दशा को प्रावश्यकता है. वह दशा प्राप्त होनी भी बहत कठिन है, और उसके प्राप्त होने के जो कारण हैं उनके मिले बिना जीव को अनन्त काल भटकना पड़ता है। इन दो कारणों के मिल जाने पर मोक्ष होता है।
-श्री मद्राजचन्द से