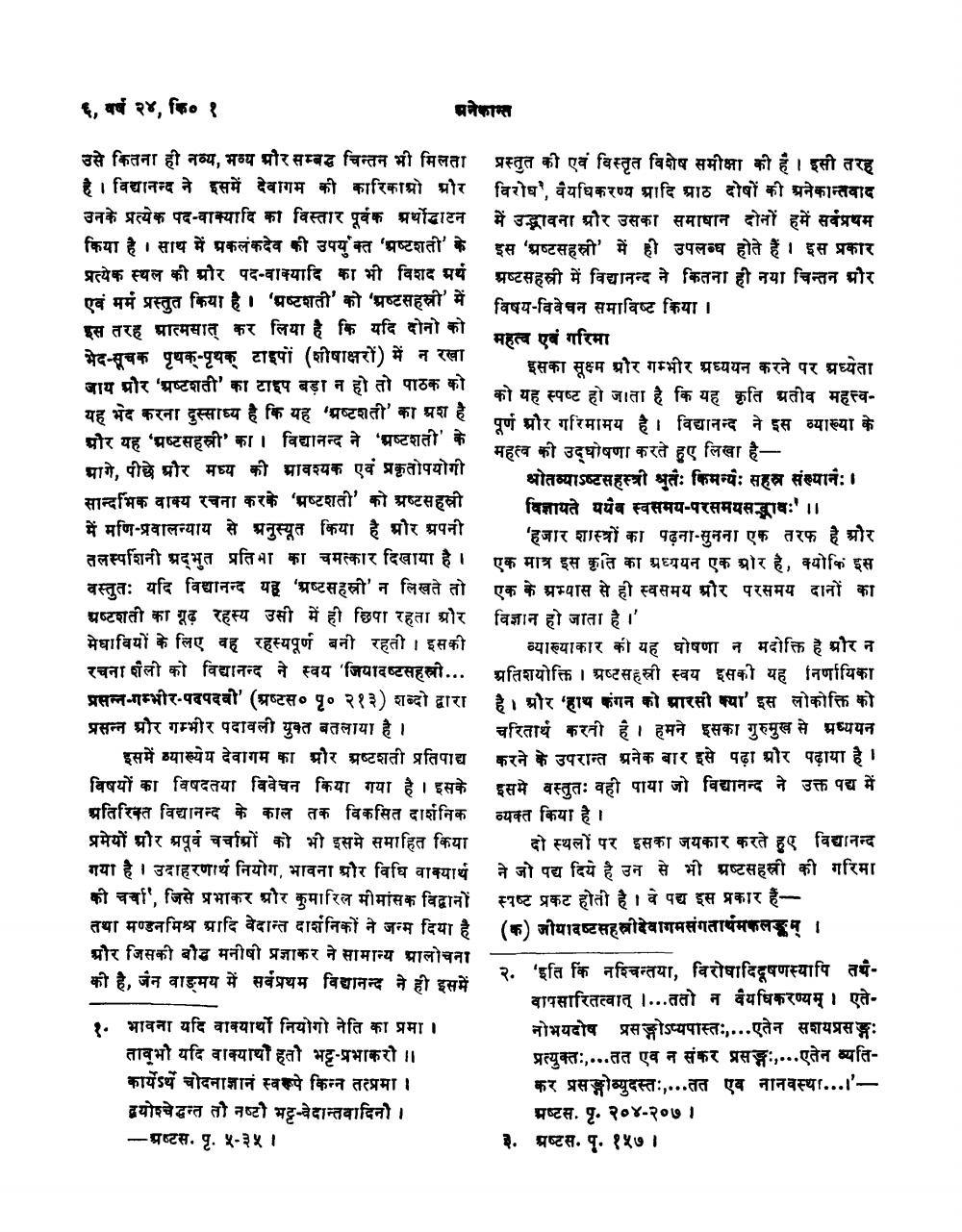________________
६, वर्ष २४, कि० १
अनेकान्त
उसे कितना ही नव्य, भव्य पोर सम्बद्ध चिन्तन भी मिलता प्रस्तुत की एवं विस्तृत विशेष समीक्षा की है। इसी तरह है। विद्यानन्द ने इसमें देवागम की कारिकामो पोर विरोध', वैयधिकरण्य प्रादि पाठ दोषों की अनेकान्तवाद उनके प्रत्येक पद-वाक्यादि का विस्तार पूर्वक अर्थोदाटन में उद्भावना और उसका समाधान दोनों हमें सर्वप्रथम किया है। साथ में प्रकलंकदेव की उपयुक्त 'अष्टशती' के इस 'प्रष्टसहस्री' में ही उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक स्थल की मोर पद-वाक्यादि का भी विशद मर्य प्रष्टसहस्री में विद्यानन्द ने कितना ही नया चिन्तन और एवं मम प्रस्तुत किया है। 'प्रष्टशती' को 'प्रष्टसहस्री' में
विषय-विवेचन समाविष्ट किया ।
विषय-नि ममानित इस तरह पात्मसात् कर लिया है कि यदि दोनो को
महत्व एवं गरिमा भेद-सूचक पृथक्-पृथक् टाइपों (शीषाक्षरों) में न रखा।
इसका सूक्ष्म और गम्भीर अध्ययन करने पर प्रध्येता जाय पोर 'प्रष्टशती' का टाइप बड़ा न हो तो पाठक को
को यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कृति प्रतीव महत्त्वयह भेद करना दुस्साध्य है कि यह 'प्रष्टशती' का प्रश है
पूर्ण और गरिमामय है। विद्यानन्द ने इस व्याख्या के पौर यह 'प्रष्टसहस्री' का। विद्यानन्द ने 'प्रष्टशती' के
महत्व की उद्घोषणा करते हुए लिखा हैमागे, पीछे और मध्य की मावश्यक एवं प्रकृतोपयोगी
श्रोतव्याऽष्टसहस्त्री श्रुतः किमन्यः सहस्र संख्यानः । सान्दभिक वाक्य रचना करके 'मष्टशती' को प्रष्टसहस्री
विज्ञायते ययैव स्वसमय-परसमयसद्भावः ।। में मणि-प्रवालन्याय से अनुस्यूत किया है और अपनी
'हजार शास्त्रों का पढ़ना-सुनना एक तरफ है और तलस्पशिनी अद्भुत प्रतिभा का चमत्कार दिखाया है। एक मात्र इस कृति का अध्ययन एक पोर है, क्योकि इस वस्तुतः यदि विद्यानन्द यह 'प्रष्टसहस्री' न लिखते तो एक के अभ्यास से ही स्वसमय और परसमय दानों का अष्टशती का गूढ़ रहस्य उसी में ही छिपा रहता और विज्ञान हो जाता है।' मेधावियों के लिए वह रहस्यपूर्ण बनी रहती। इसकी व्याख्याकार की यह घोषणा न मदोक्ति है और न रचना शैली को विद्यानन्द ने स्वय 'जियावष्टसहस्री... अतिशयोक्ति । प्रष्टसहस्री स्वय इसकी यह निर्णायिका प्रसन्न-गम्भीर-पदपदवी' (प्रष्टस० पृ० २१३) शब्दो द्वारा है। और हाथ कंगन को प्रारसी क्या' इस लोकोक्ति को प्रसन्न और गम्भीर पदावली युक्त बतलाया है। चरितार्थ करती है। हमने इसका गुरुमुख से अध्ययन ___ इसमें व्याख्येय देवागम का मोर अष्टशती प्रतिपाद्य करने के उपरान्त अनेक बार इसे पढ़ा और पढ़ाया है । विषयों का विषदतया विवेचन किया गया है। इसके इसमे वस्तुतः वही पाया जो विद्यानन्द ने उक्त पद्य में अतिरिक्त विद्यानन्द के काल तक विकसित दार्शनिक व्यक्त किया है। प्रमेयों और अपूर्व चर्चानों को भी इसमे समाहित किया दो स्थलों पर इसका जयकार करते हुए विद्यानन्द गया है। उदाहरणार्थ नियोग, भावना और विधि वाक्यार्थ ने जो पद्य दिये है उन से भी प्रष्टसहस्री की गरिमा की चर्चा', जिसे प्रभाकर और कुमारिल मीमांसक विद्वानों स्पष्ट प्रकट होती है। वे पद्य इस प्रकार हैंतथा मण्डनमिश्र प्रादि वेदान्त दार्शनिकों ने जन्म दिया है (क) जीयावष्टसहस्रीदेवागमसंगतार्थमकलङ्कम् । और जिसकी बौद्ध मनीषी प्रज्ञाकर ने सामान्य पालोचना की है, जैन वाङ्मय में सर्वप्रथम विद्यानन्द ने ही इसमें
२. 'इति कि नश्चिन्तया, विरोषादिषणस्यापि तथ
वापसारितत्वात् ।...ततो न वैयधिकरण्यम् । एते. १. भावना यदि वाक्यार्थी नियोगो नेति का प्रमा। नोभयदोष प्रसङ्गोऽप्यपास्तः,...एतेन सशयप्रसङ्गः तावुभौ यदि वाक्याथो हतो भट्ट-प्रभाकरी ॥
प्रत्युक्तः,...तत एव न संकर प्रसङ्गः,...एतेन व्यतिकार्येऽर्थे चोदनाशानं स्वरूपे किन्न तत्प्रमा।
कर प्रसङ्गोव्युदस्तः,...तत एव नानवस्था....'द्वयोश्चे द्धन्त तो नष्टौ भद्र-वेदान्तवादिनी।
मष्टस. पृ. २०४-२०७। -प्रष्टस. पृ. ५-३५।
३. प्रष्टस. पृ. १५७ ।