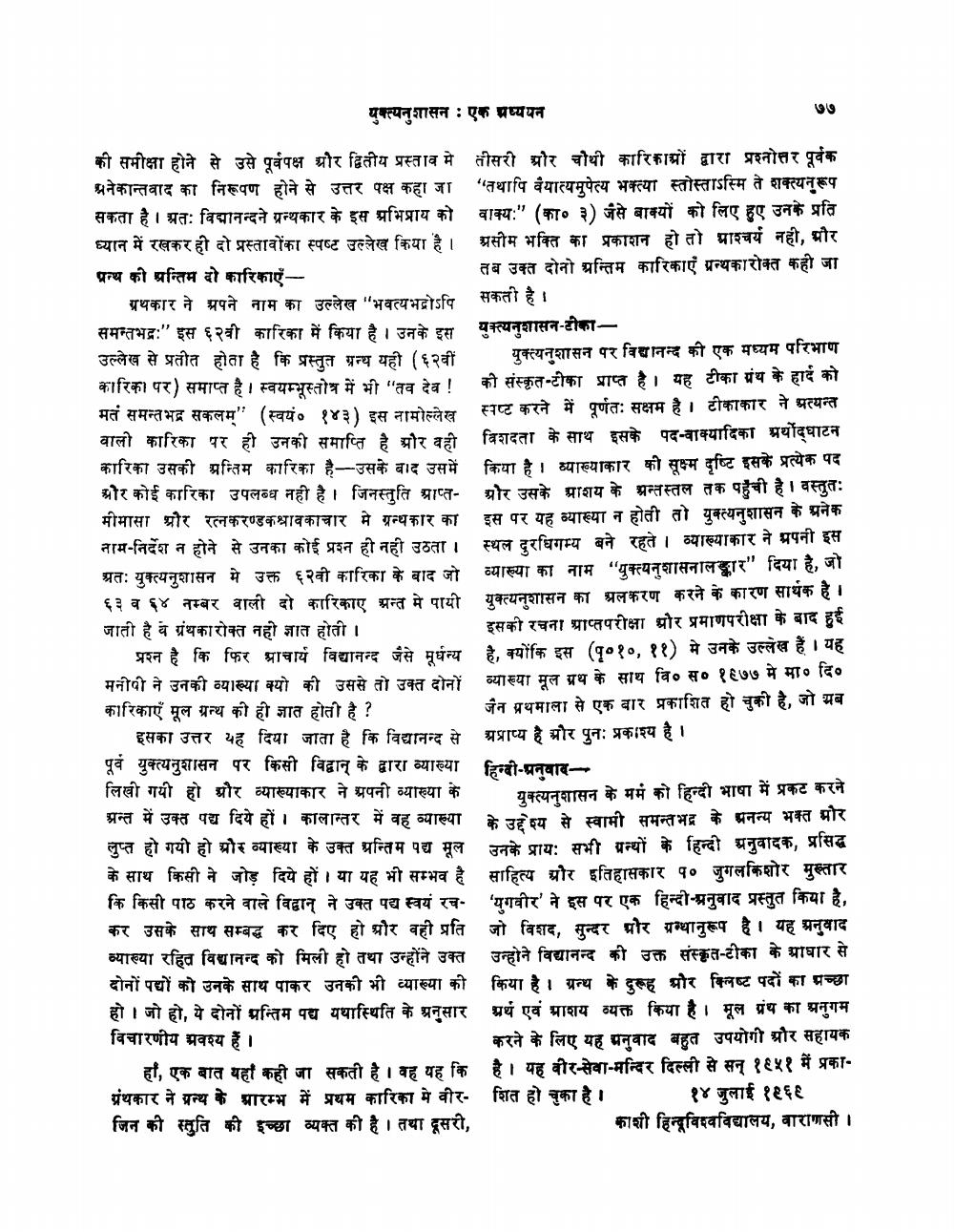________________
युक्त्यनुशासन : एक अध्ययन
की समीक्षा होने से उसे पूर्वपक्ष और द्वितीय प्रस्ताव में तीसरी और चौथी कारिकामों द्वारा प्रश्नोत्तर पूर्वक अनेकान्तवाद का निरूपण होने से उत्तर पक्ष कहा जा "तथापि वैयात्यमुपेत्य भक्त्या स्तोस्ताऽस्मि ते शक्त्यनुरूप सकता है । अतः विद्यानन्दने ग्रन्थकार के इस अभिप्राय को वाक्य:" (का० ३) जैसे बाक्यों को लिए हुए उनके प्रति ध्यान में रखकर ही दो प्रस्तावोंका स्पष्ट उल्लेख किया है। असीम भक्ति का प्रकाशन हो तो माश्चर्य नही, और प्रन्थ की अन्तिम दो कारिकाएँ
तब उक्त दोनो अन्तिम कारिकाएं ग्रन्थकारोक्त कही जा प्रथकार ने अपने नाम का उल्लेख "भवत्यभद्रोऽपि सकती है। समन्तभद्रः" इस ६२वी कारिका में किया है। उनके इस युक्त्यनुशासन-टीकाउल्लेख से प्रतीत होता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ यही (६२वीं युक्त्यनुशासन पर विद्यानन्द की एक मध्यम परिभाण कारिका पर) समाप्त है। स्वयम्भूस्तोत्र में भी "तव देव! की संस्कृत-टीका प्राप्त है। यह टीका ग्रंय के हार्द को मतं समन्तभद्र सकलम्" (स्वयं० १४३) इस नामोल्लेख सप्ट करने में पूर्णतः सक्षम है। टीकाकार ने अत्यन्त वाली कारिका पर ही उनकी समाप्ति है और वही विशदता के साथ इसके पद-वाक्यादिका अर्थोद्घाटन कारिका उसकी अन्तिम कारिका है-उसके बाद उसमें किया है। व्याख्याकार की सूक्ष्म दृष्टि इसके प्रत्येक पद और कोई कारिका उपलब्ध नही है। जिनस्तुति प्राप्त- और उसके प्राशय के अन्तस्तल तक पहुंची है। वस्तुतः मीमासा और रत्नकरण्डकश्रावकाचार मे ग्रन्धकार का इस पर यह व्याख्या न होती तो युक्त्यनुशासन के अनेक नाम-निर्देश न होने से उनका कोई प्रश्न ही नही उठता। स्थल दूरधिगम्य बने रहते । व्याख्याकार ने अपनी इस अतः युक्त्यनुशासन मे उक्त ६२वी कारिका के बाद जो व्याख्या का नाम "युक्त्यनुशासनालङ्कार" दिया है, जो ६३ व ६४ नम्बर वाली दो कारिकाए अन्त मे पायी युक्त्यनुशासन का अलकरण करने के कारण सार्थक है । जाती है वे ग्रंथकारोक्त नही ज्ञात होती।
इसकी रचना प्राप्तपरीक्षा और प्रमाणपरीक्षा के बाद हुई प्रश्न है कि फिर प्राचार्य विद्यानन्द जैसे मूर्धन्य है, क्योंकि इस (१०१०, ११) मे उनके उल्लेख हैं । यह मनीषी ने उनकी व्याख्या क्यो की उससे तो उक्त दोनों व्याख्या मूल प्रथ के साथ वि० स० १९७७ में मा० दि. कारिकाएँ मूल ग्रन्थ की ही ज्ञात होती है ?
जैन प्रथमाला से एक बार प्रकाशित हो चुकी है, जो अब ___ इसका उत्तर यह दिया जाता है कि विद्यानन्द से अप्राप्य है और पुनः प्रकाश्य है । पूर्व युक्त्यनुशासन पर किसी विद्वान् के द्वारा व्याख्या हिन्दी-अनुवादलिखी गयी हो और व्याख्याकार ने अपनी व्याख्या के यक्त्यनशासन के मर्म को हिन्दी भाषा में प्रकट करने अन्त में उक्त पद्य दिये हों। कालान्तर में वह व्याख्या के उद्देश्य से स्वामी समन्तभद्र के अनन्य भक्त भोर लुप्त हो गयी हो और व्याख्या के उक्त अन्तिम पद्य मूल उनके प्रायः सभी ग्रन्थों के हिन्दी अनुवादक, प्रसिद्ध के साथ किसी ने जोड़ दिये हों। या यह भी सम्भव है साहित्य और इतिहासकार १० जुगलकिशोर मुख्तार कि किसी पाठ करने वाले विद्वान् ने उक्त पद्य स्वयं रच- 'युगवीर' ने इस पर एक हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया है, कर उसके साथ सम्बद्ध कर दिए हो और वही प्रति जो विशद, सुन्दर पोर ग्रन्थानुरूप है। यह अनुवाद व्याख्या रहित विद्यानन्द को मिली हो तथा उन्होंने उक्त उन्होने विद्यानन्द की उक्त संस्कृत-टीका के आधार से दोनों पद्यों को उनके साथ पाकर उनकी भी व्याख्या की किया है। ग्रन्थ के दुरूह और क्लिष्ट पदों का अच्छा हो । जो हो, ये दोनों अन्तिम पद्य यथास्थिति के अनुसार अर्थ एवं प्राशय व्यक्त किया है। मूल ग्रंथ का अनुगम विचारणीय अवश्य हैं।
करने के लिए यह मनुवाद बहत उपयोगी और सहायक हाँ, एक बात यहाँ कही जा सकती है। वह यह कि है। यह वीर-सेवा-मन्दिर दिल्ली से सन् १९५१ में प्रकाग्रंथकार ने ग्रन्थ के प्रारम्भ में प्रथम कारिका मे वीर- शित हो चुका है। १४ जुलाई १९६६ जिन की स्तुति की इच्छा व्यक्त की है । तथा दूसरी,
काशी हिन्दूविश्वविद्यालय, वाराणसी।