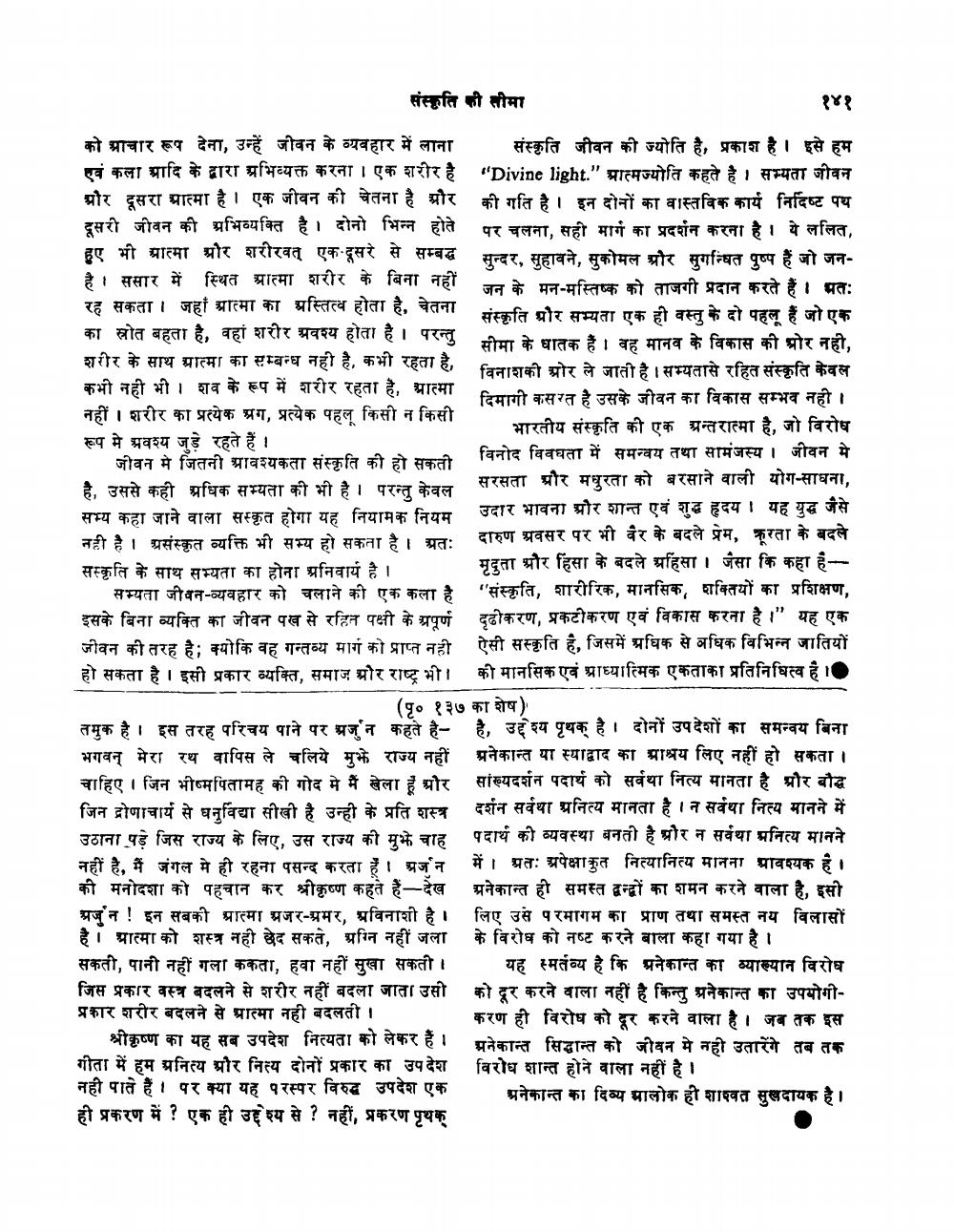________________
संस्कृति की सीमा
१४१
को आचार रूप देना, उन्हें जीवन के व्यवहार में लाना संस्कृति जीवन की ज्योति है, प्रकाश है। इसे हम एवं कला आदि के द्वारा अभिव्यक्त करना । एक शरीर है "Divine light." प्रात्मज्योति कहते है। सभ्यता जीवन और दूसरा प्रात्मा है । एक जीवन की चेतना है और की गति है। इन दोनों का वास्तविक कार्य निर्दिष्ट पथ दूसरी जीवन की अभिव्यक्ति है। दोनो भिन्न होते पर चलना, सही मार्ग का प्रदर्शन करना है। ये ललित, हुए भी प्रात्मा और शरीरवत् एक दूसरे से सम्बद्ध
वत् एक-दूसर स सम्बद्ध सुन्दर, सुहावने, सुकोमल और सुगन्धित पुष्प हैं जो जनहै। ससार में स्थित प्रात्मा शरीर के बिना नहीं
नहा जन के मन-मस्तिष्क को ताजगी प्रदान करते हैं। अत: रह सकता। जहाँ आत्मा का अस्तित्व होता है, चेतना
संस्कृति और सभ्यता एक ही वस्तु के दो पहलू हैं जो एक का स्रोत बहता है, वहां शरीर अवश्य होता है। परन्तु ।
सीमा के धातक हैं। वह मानव के विकास की पोर नही, शरीर के साथ प्रात्मा का सम्बन्ध नहीं है, कभी रहता है,
विनाशकी ओर ले जाती है । सभ्यतासे रहित संस्कृति केवल कभी नही भी। शव के रूप में शरीर रहता है, आत्मा
दिमागी कसरत है उसके जीवन का विकास सम्भव नही । नहीं । शरीर का प्रत्येक प्रग, प्रत्येक पहल किसी न किसी
भारतीय संस्कृति की एक अन्तरात्मा है, जो विरोध रूप में अवश्य जुड़े रहते हैं। जीवन मे जितनी आवश्यकता संस्कृति की हो सकती
विनोद विवधता में समन्वय तथा सामंजस्य । जीवन मे है, उससे कही अधिक सभ्यता की भी है। परन्तु केवल
सरसता और मधुरता को बरसाने वाली योग-साधना, सभ्य कहा जाने वाला सस्कृत होगा यह नियामक नियम
उदार भावना और शान्त एवं शुद्ध हृदय । यह युद्ध जैसे नहीं है। असंस्कृत व्यक्ति भी सभ्य हो सकता है। अतः
दारुण अवसर पर भी वैर के बदले प्रेम, क्रूरता के बदले सस्कृति के साथ सभ्यता का होना अनिवार्य है।
मृदुता और हिंसा के बदले अहिंसा। जैसा कि कहा है___सभ्यता जीवन-व्यवहार को चलाने की एक कला है "संस्कृति, शारीरिक, मानसिक, शक्तियों का प्रशिक्षण, इसके बिना व्यक्ति का जीवन पख से रहित पक्षी के अपूर्ण दृढीकरण, प्रकटीकरण एवं विकास करना है।" यह एक जीवन की तरह है; क्योकि वह गन्तव्य मार्ग को प्राप्त नही ऐसी सस्कृति है, जिसमें अधिक से अधिक विभिन्न जातियों हो सकता है । इसी प्रकार व्यक्ति, समाज और राष्ट्र भी। की मानसिक एवं प्राध्यात्मिक एकताका प्रतिनिधित्व है।
(पृ० १३७ का शेष) तमुक है। इस तरह परिचय पाने पर अर्जुन कहते है- है, उद्देश्य पृथक् है। दोनों उपदेशों का समन्वय बिना भगवन् मेरा रथ वापिस ले चलिये मुझे राज्य नहीं अनेकान्त या स्याद्वाद का पाश्रय लिए नहीं हो सकता। चाहिए । जिन भीष्मपितामह की गोद मे मैं खेला है और सांख्यदर्शन पदार्थ को सर्वथा नित्य मानता है और बौद्ध जिन द्रोणाचार्य से धनविद्या सीखी है उन्ही के प्रति शस्त्र दर्शन सर्वथा अनित्य मानता है । न सर्वथा नित्य मानने में उठाना पड़े जिस राज्य के लिए, उस राज्य की मुझे चाह पदार्थ की व्यवस्था बनती है और न सर्वथा प्रनित्य मानने नहीं है, मैं जंगल मे ही रहना पसन्द करता है। अर्जन में। प्रतः अपेक्षाकृत नित्यानित्य मानना प्रावश्यक है। की मनोदशा को पहचान कर श्रीकृष्ण कहते हैं-देख अनेकान्त ही समस्त द्वन्द्वों का शमन करने वाला है, इसी अर्जुन ! इन सबकी प्रात्मा अजर-अमर, अविनाशी है। लिए उसे परमागम का प्राण तथा समस्त नय विलासों है। प्रात्मा को शस्त्र नही छेद सकते, अग्नि नहीं जला के विरोध को नष्ट करने बाला कहा गया है। सकती, पानी नहीं गला ककता, हवा नहीं सुखा सकती। यह स्मर्तव्य है कि अनेकान्त का व्याख्यान विरोध जिस प्रकार वस्त्र बदलने से शरीर नहीं बदला जाता उसी को दूर करने वाला नहीं है किन्तु अनेकान्त का उपयोगीप्रकार शरीर बदलने से प्रात्मा नही बदलती।
करण ही विरोध को दूर करने वाला है। जब तक इस श्रीकृष्ण का यह सब उपदेश नित्यता को लेकर है। अनेकान्त सिद्धान्त को जीवन मे नही उतारेंगे तब तक गीता में हम अनित्य और नित्य दोनों प्रकार का उपदेश विरोध शान्त होने वाला नहीं है। नही पाते हैं। पर क्या यह परस्पर विरुद्ध उपदेश एक
अनेकान्त का दिव्य मालोक ही शाश्वत सुखदायक है। ही प्रकरण में ? एक ही उद्देश्य से ? नहीं, प्रकरण पृथक्