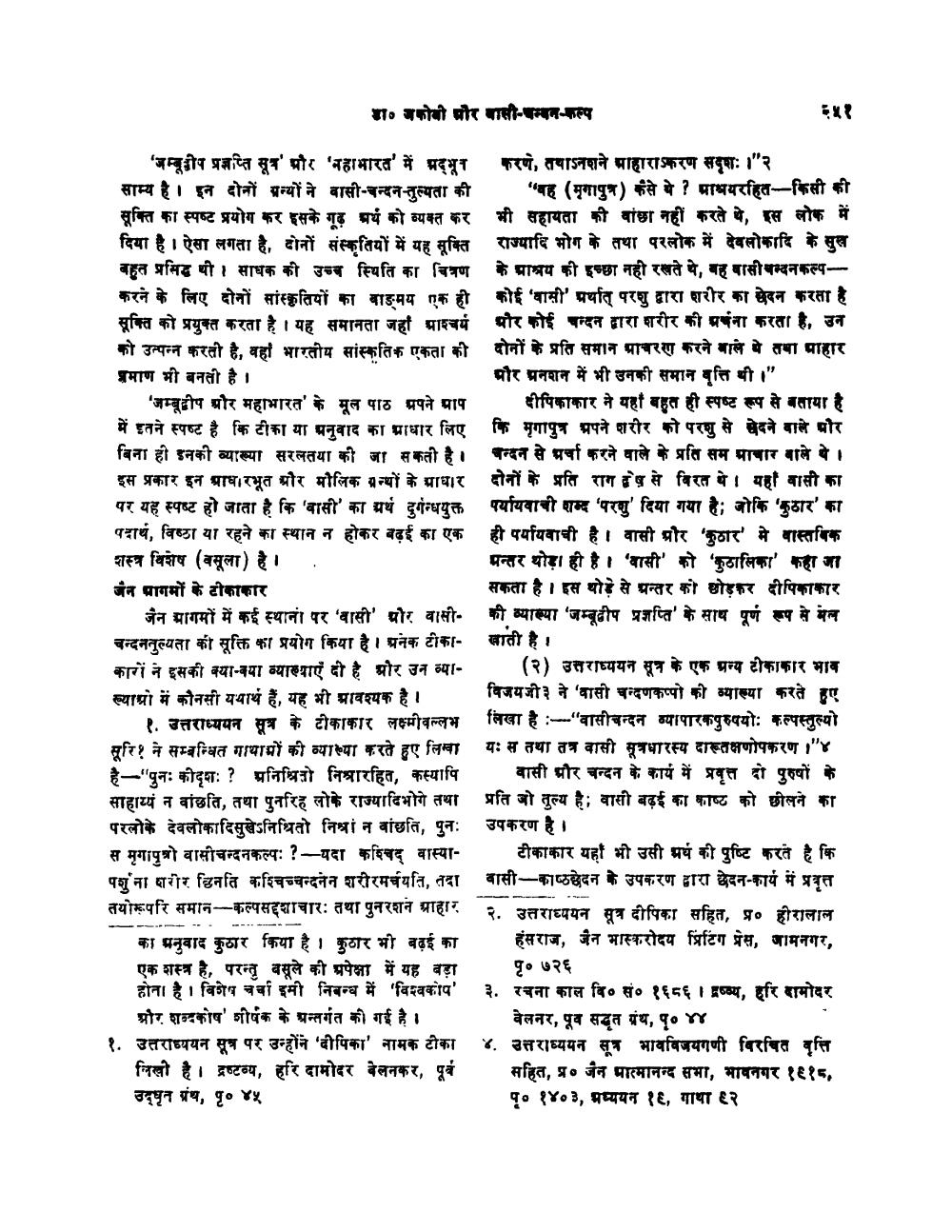________________
म.कोबी और बासी-धन्वन-कल्प
'जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र' और 'महाभारत' में अद्भूत करणे, तवाऽनशने माहाराकरण सदृशः।"२ साम्य है। इन दोनों अन्यों ने बासी-चन्दन-तुल्यता की "वह (मृगापुत्र) कैसे थे? पाश्रयरहित-किसी की सूक्ति का स्पष्ट प्रयोग कर इसके गूढ़ अर्थ को व्यक्त कर भी सहायता की वांछा नहीं करते थे, इस लोक में दिया है। ऐसा लगता है, दोनों संस्कृतियों में यह सूक्ति राज्यादि भोग के तथा परलोक में देवलोकादि के सुख बहुत प्रसिद्ध थी। साधक की उच्च स्थिति का चित्रण के प्राश्रय की इच्छा नही रखते थे, वह बासीचन्दनकल्पकरने के लिए दोनों सांस्कृतियों का वाङ्मय एक ही कोई 'वासी' अर्थात् परशु द्वारा शरीर का छेदन करता है सूक्ति को प्रयुक्त करता है। यह समानता जहां पाश्चर्य और कोई चन्दन द्वारा शरीर की पर्चना करता है, उन को उत्पन्न करती है, वहां भारतीय सांस्कृतिक एकता की दोनों के प्रति समान पाचरण करने वाले थे तथा माहार प्रमाण भी बनती है।
पौर प्रनशन में भी उनकी समान वृत्ति थी।" 'जम्बूद्वीप और महाभारत' के मूल पाठ अपने पाप दीपिकाकार ने यहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है में इतने स्पष्ट है कि टीका या अनुवाद का प्राधार लिए कि मृगापुत्र अपने शरीर को परशु से वेदने वाले और बिना ही इनकी व्याख्या सरलतया की जा सकती है। चन्दन से अर्चा करने वाले के प्रति सम माचार वाले थे। इस प्रकार इन आधारभूत और मौलिक ग्रन्थों के माधार दोनों के प्रति राग द्वेष से विरत थे। यहाँ वासी का पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 'बासी' का अर्थ दुर्गन्धयुक्त पर्यायवाची शब्द 'परशु' दिया गया है। जोकि 'कुठार' का पदार्थ, विष्ठा या रहने का स्थान न होकर बढ़ई का एक ही पर्यायवाची है। वासी और 'कुठार' में वास्तविक शस्त्र विशेष (वसूला) है। .
मन्तर थोड़ा ही है। 'वासी' को 'कुठालिका' कहा जा जन पागमों के टीकाकार
सकता है । इस थोड़े से अन्तर को छोड़कर दीपिकाकार जैन मागमों में कई स्थानों पर 'वासी' पोर वासी. की व्याख्या 'जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के साथ पूर्ण रूप से मेल चन्दनतुल्यता की सूक्ति का प्रयोग किया है। अनेक टीका- खाती है। कारों ने इसकी क्या-क्या व्याख्याएं दी है और उन व्या- (२) उत्तराध्ययन सूत्र के एक अन्य टीकाकार भाव ख्यानो में कौनसी यथार्थ हैं, यह भी प्रावश्यक है। विजयजी३ ने 'वासी चन्दणकप्पो की व्याख्या करते हुए
१. उत्तराध्ययन सूत्र के टीकाकार लक्ष्मीवल्लभ लिखा है :-"वासीचन्दन व्यापारकपुरुपयोः कल्पस्तुल्यो सूरि? ने सम्बन्धित गाथामों की व्याख्या करते हुए लिखा यः स तथा तत्र वासी सूत्रधारस्य दारूतक्षणोपकरण।"४ है-"पुनः कीदृशः ? अनिश्रितो निश्रारहित, कस्यापि वासी और चन्दन के कार्य में प्रवृत्त दो पुरुषों के साहाय्यं न वांछति, तथा पुनरिह लोके राज्यादिभोगे तथा प्रति जो तुल्य है। वासी बढ़ई का काष्ट को छीलने का परलोके देवलोकादिसुखेऽनिधितो निश्रां न वांछति, पुनः उपकरण है। स मृगापुत्रो वासीचन्दनकल्पः ?-यदा कश्चिद् वास्या- टीकाकार यहाँ भी उसी अर्थ की पुष्टि करते है कि पर्श ना बारीर छिनति कश्चिच्चन्दनेन शरीरमर्चयति, तदा वासी-काष्ठछेदन के उपकरण द्वारा छेदन-कार्य में प्रवृत्त तयोरुपरि समान-कल्पसदशाचारः तथा पुनरशन पाहार २. उत्तराध्ययन सूत्र दीपिका सहित, प्र. हीरालाल
का अनुवाद कुठार किया है । कुठार भी बढ़ई का हंसराज, जैन भास्करोदय प्रिंटिंग प्रेस, जामनगर, एक शस्त्र है, परन्तु बसूले की अपेक्षा में यह बड़ा पृ० ७२६ । होता है। विशेष चर्चा इमी निबन्ध में 'विश्वकोप' ३. रचना काल वि० सं० १६८६ । द्रव्य, हरि दामोदर और शब्दकोष' शीर्षक के अन्तर्गत की गई है।
वेलनर, पूर्व सद्धृत ग्रंथ, पृ०४ १. उत्तराध्ययन सूत्र पर उन्होंने 'दीपिका' नामक टीका ४. उत्तराध्ययन सूत्र भावविजयगणी विरचित वृत्ति
लिखी है। द्रष्टव्य, हरि दामोदर बेलनकर, पूर्व महित, प्र. जैन मात्मानन्द सभा, भावनगर १९१८, उद्धृत ग्रंथ, पृ. ४५
पृ० १४०३, अभ्ययन १६, गाथा १२