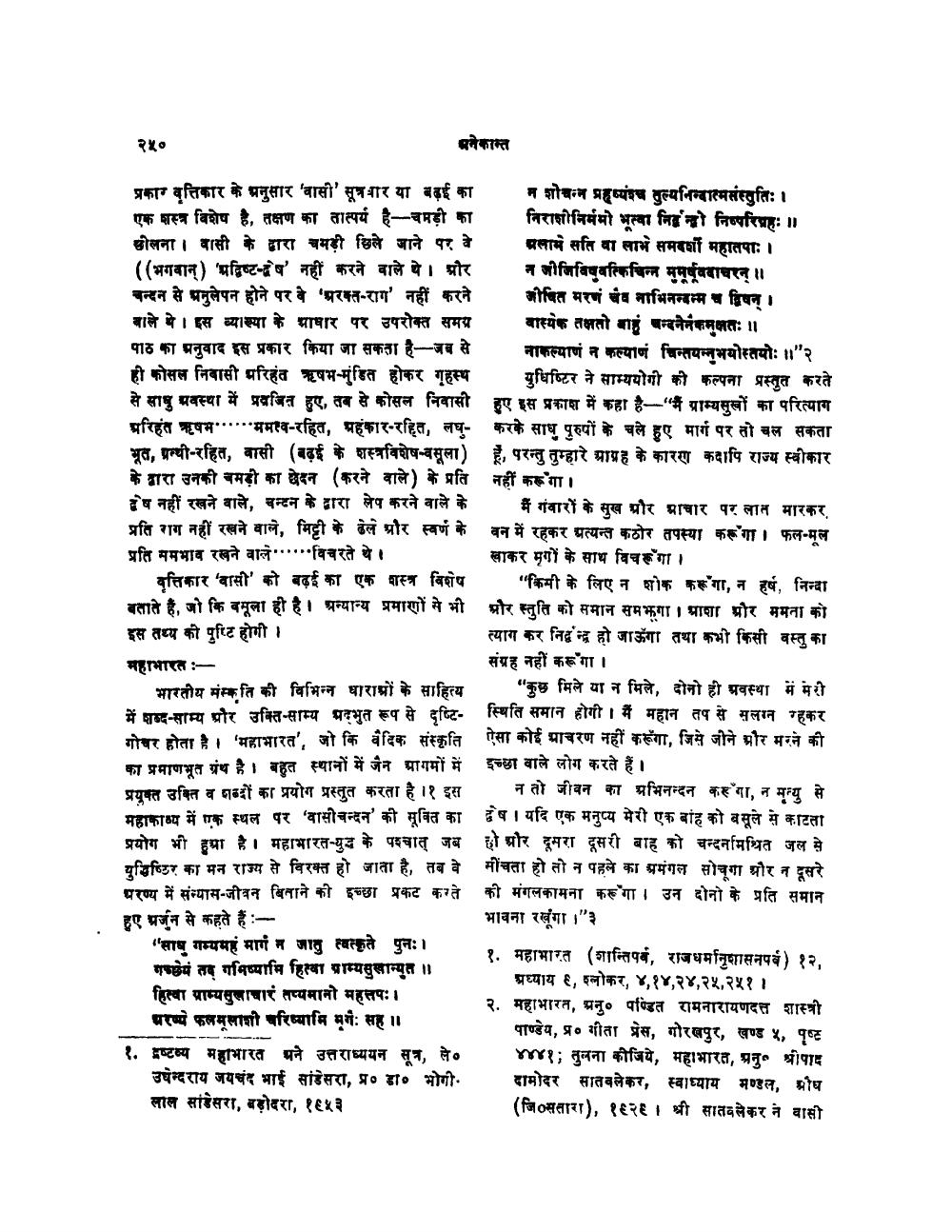________________
२५०
अनेकान्त
प्रकार वृत्तिकार के अनुसार 'वासी' सूत्रधार या बढ़ई का म शोचन्न प्रहृष्यंच तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः । एक शस्त्र विशेष है, तक्षण का तात्पर्य है-चमड़ी का निराशीनिर्ममो भूत्वा निईन्द्रो निष्परिग्रहः॥ छोलना। वासी के द्वारा चमड़ी छिले जाने पर वे मलामे सति वा लाभे समवशी महातपाः। ((भगवान्) 'पद्विष्ट-देष' नहीं करने वाले थे। और नजीनिविषुवकिचिन्न मुमधुवाचरन् । चन्दन से अनुलेपन होने पर वे 'परक्त-राग' नहीं करने जोषित मरणं चैव नाभिनन्दन्म व द्विषन् । वाले थे। इस व्याख्या के आधार पर उपरोक्त समय वास्येक तक्षतो बाहुं चन्दनेमकमुक्षतः॥ पाठ का अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है-जब से
नाकल्याणं न कल्याणं चिन्तयन्नुभयोस्तयोः॥"२ ही कोसल निवासी परिहंत ऋषभ-मुंडित होकर गृहस्थ युधिष्टिर ने साम्ययोगी की कल्पना प्रस्तुत करते से साधु अवस्था में प्रवजित हुए, तब से कोसल निवासी हुए इस प्रकाश में कहा है-"मैं ग्राम्यसुखों का परित्याग परिहंत ऋषम....."ममत्व-रहित, अहंकार-रहित, लघु- करके साधु पुरुषों के चले हुए मार्ग पर तो चल सकता भूत, प्रन्थी-रहित, वासी (बढ़ई के शस्त्रविशेष-वसूला) है, परन्तु तुम्हारे प्राग्रह के कारण कदापि राज्य स्वीकार के द्वारा उनकी चमड़ी का छेदन (करने वाले) के प्रति नहीं करूंगा। देष नहीं रखने वाले, चन्दन के द्वारा लेप करने वाले के मैं गंवारों के सुख और प्राचार पर लात मारकर प्रति राग नहीं रखने वाले, मिट्टी के ढेले और स्वर्ण के वन में रहकर अत्यन्त कठोर तपस्या करूंगा। फल-मूल प्रति ममभाव रखने वाले....."विचरते थे।
खाकर मृगों के साथ विचरूंगा। बत्तिकार 'वासी' को बढ़ई का एक वास्त्र विशेष "किमी के लिए न शोक करूंगा, न हर्ष, निन्दा बताते हैं, जो कि बमूला ही है। अन्यान्य प्रमाणों से भी और स्तुति को समान समझगा। पाशा और ममता को इस तथ्य को पुष्टि होगी।
त्याग कर निर्द्वन्द्र हो जाऊँगा तथा कभी किसी वस्तु का महाभारत:
संग्रह नहीं करूंगा। भारतीय मंकति की विभिन्न धारामों के साहित्य "कुछ मिले या न मिले, दोनो ही अवस्था में मेरी में शब्द-साम्य और उक्ति-साम्य अदभुत रूप से दृष्टि- स्थिति समान होगी। मैं महान तप से सलग्न रहकर गोचर होता है। 'महाभारत', जो कि वैदिक संस्कृति ऐसा कोई पाचरण नहीं करूँगा, जिसे जीने और मरने की का प्रमाणभूत ग्रंथ है। बहुत स्थानों में जैन भागमों में इच्छा वाले लोग करते हैं। प्रयुक्त उक्ति व शब्दों का प्रयोग प्रस्तुत करता है । इस न तो जीवन का अभिनन्दन करूंगा, न मन्यू से महाकाव्य में एक स्थल पर 'वासीचन्दन' की सूक्ति का हष । यदि एक मनुप्य मेरी एक बांह को बसले से काटता प्रयोग भी हमा है। महाभारत-युद्ध के पश्चात् जब हो और दूसरा दूसरी बाह को चन्दनमिथित जल से युधिष्ठिर का मन राज्य से विरक्त हो जाता है, तब वे मींचता हो तो न पहले का अमंगल सोचगा और न दूसरे परण्य में संन्यास-जीवन बिताने की इच्छा प्रकट करते की मंगलकामना करूंगा। उन दोनो के प्रति समान हुए अर्जुन से कहते हैं :
भावना रखंगा।"३ "साधु गम्यमहं मागं न जातु त्वत्कृते पुनः।
१. महाभारत (शान्तिपर्व, राजधर्मानुशासनपर्व) १२, गच्छेयं तद गमिष्यामि हित्वा प्राम्यसुखान्युत ॥
अध्याय ६, श्लोकर, ४,१४,२४,२५,२५१ । हित्वा ग्राम्यसुलाचारं तप्यमानो महत्तपः।
२. महाभारत, अनु० पण्डित रामनारायणदत्त शास्त्री भरष्ये फलमूलाशी चरिष्यामि मर्गः सह ॥
पाण्डेय, प्र. गीता प्रेस, गोरखपुर, खण्ड ५, पृष्ट १. द्रष्टव्य महाभारत भने उत्तराध्ययन सूत्र, ले. ४१; तुलना कीजिये, महाभारत, अनु. श्रीपाद
उपेन्दराय जयचंद भाई सांडेसरा, प्र. डा. भोगी. दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पौष साल सांडेसरा, बड़ोदरा, १९५३
(जिससाग), १९२९ । श्री सातवलेकर ने वासी