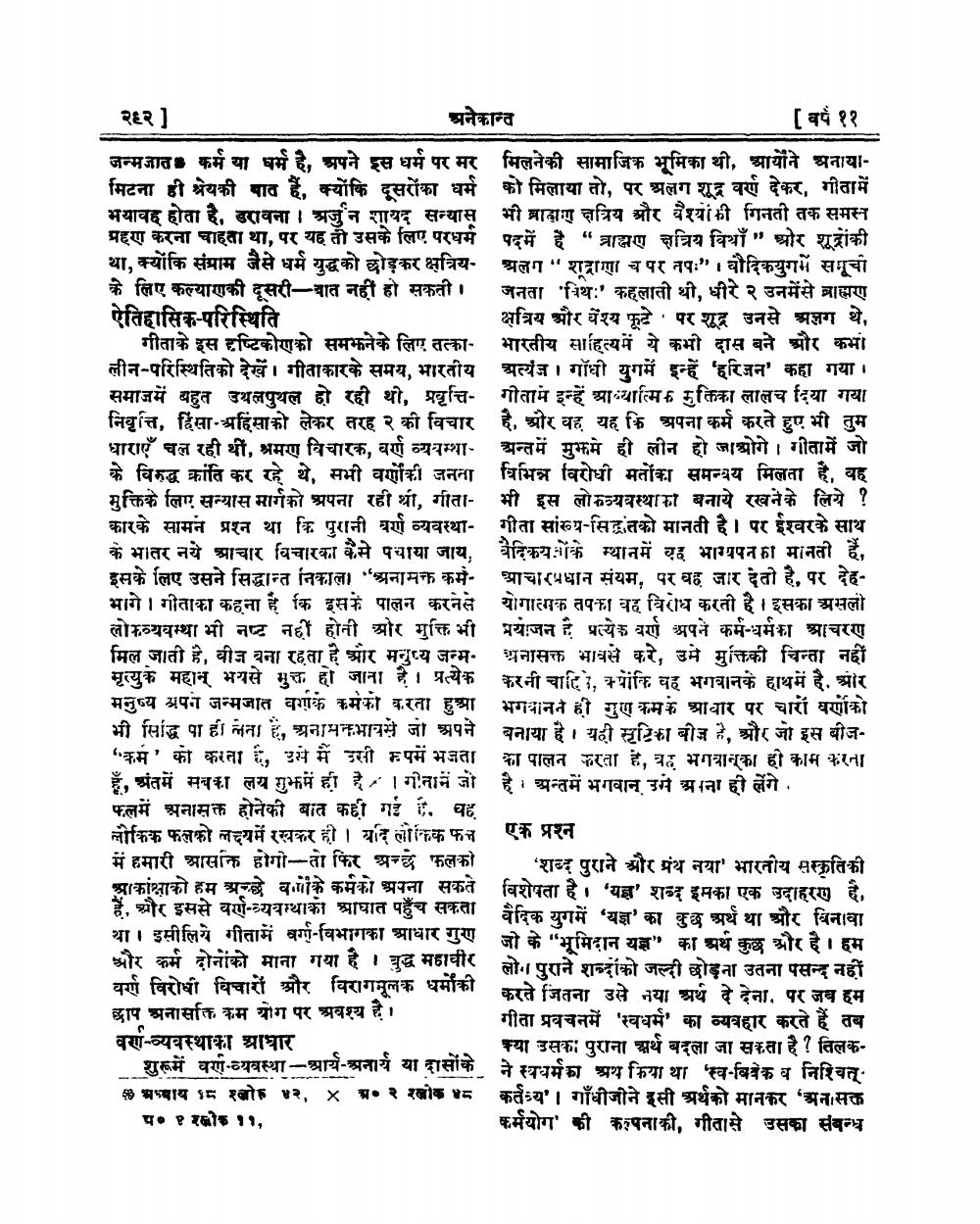________________
२६२]
अनेकान्त
[वर्ष १२
जन्मजात: कर्म या धर्म है, अपने इस धर्म पर मर मिलनेकी सामाजिक भूमिका थी, आर्योंने अनायामिटना ही श्रेयकी बात हैं, क्योंकि दूसरोंका धर्म को मिलाया तो, पर अलग शूद्र वर्ण देकर, गीतामें भयावह होता है, डरावना । अर्जुन शायद सन्यास भी ब्राह्माण क्षत्रिय और वैश्यों की गिनती तक समस प्रहण करना चाहता था, पर यह तो उसके लिए परधर्म पदमें है "ब्राह्मण क्षत्रिय वियाँ " ओर शूद्रोंकी था, क्योंकि संग्राम जैसे धर्म युद्धको छोड़कर क्षत्रिय
सग्राम जैस धर्म युद्धको छोड़कर क्षत्रिय- अलग"शदाणा च पर नपः" । वौदिकयुगमें समूची के लिए कल्याणकी दूसरी बात नहीं हो सकती। जनता "पिथः' कहलाती थी, धीरे २ उनमेंसे ब्राह्मण ऐतिहासिक-परिस्थिति
क्षत्रिय और पेंश्य फूटे । पर शूद्र उनसे अलग थे, __गीताके इस दृष्टिकोणको समझने के लिए तत्का. भारतीय साहित्यमें ये कभी दास बने और कभी लीन-परिस्थितिको देखें। गीताकारके समय, भारतीय अत्यंज । गाँधी युगमें इन्हें 'हरिजन' कहा गया। समाजमें बहुत उथलपुथल हो रही थी, प्रवृत्ति- गीताम इन्हें आध्यात्मिक मुक्तिका लालच दिया गया निवृत्ति, हिंसा-अहिंसाको लेकर तरह २ की विचार है, और वह यह कि अपना कर्म करते हुए भी तुम धाराएँ चल रही थीं, श्रमण विचारक, वर्ण व्यवस्था- अन्तमें मुझमे ही लीन हो जाओगे। गीतामें जो के विरुद्ध क्रांति कर रहे थे, सभी वर्गों की जनता विभिन्न विरोधी मतोंका समन्वय मिलता है, वह मुक्तिके लिए सन्यास मार्गको अपना रही थी, गीता- भी इस लोकव्यवस्थाका बनाये रखने के लिये ? कारके सामने प्रश्न था कि पुरानी वर्ण व्यवस्था- गीता सांख्य-सिद्वांतको मानती है। पर ईश्वरके साथ के भातर नये आचार विचारका कैसे पचाया जाय, वैदिकयोंके स्थानमें यह भाग्यपनका मानती हैं, इसके लिए उसने सिद्धान्त निकाला "अनामत कर्म- आचारप्रधान संयम, पर वह जार देतो है, पर देहभागे । गीताका कहना है कि इसके पालन करनेसे योगात्मक तपका वह विरोध करती है । इसका असली लोकव्यवस्था भी नष्ट नहीं होनी ओर मुक्ति भी प्रयोजन है. प्रत्येक वर्ण अपने कर्म-धर्मका आचरण मिल जाती है, बीज बना रहता है और मनुष्य जन्म. अनासक्त भावसे करे, उमे मुक्तिकी चिन्ता नहीं मृत्युके महान् भयसे मुक्त हो जाना है। प्रत्येक करनी चादि, क्योंकि यह भगवानके हाथ में है. और मनुष्य अपने जन्मजात वाके कमको करता हुआ भगवानने ही गुण कम आधार पर चारों वर्णको भी सिद्धि पाही लेना है, अनामनभावसे जो अपने बनाया है। यही मृटिका बीज है, और जो इस बीज"कर्म' को करता है, उसे में उसी कपमें भजता का पालन करता है, वह भगवानका ही काम करता हूँ. अंतमें सबका लय गुझमें ही है । गीनामें जो है। अन्तमें भगवान उसे अपना ही लेंगे । फलमें अनासक्त होनेकी बात कही गई है. यह लौकिक फलको लक्ष्यमें रखकर ही। यदि लौकिक फन एक प्रश्न में हमारी आसकि होगी-तो फिर अच्छे फलको शब्द पुराने और ग्रंथ नया' भारतीय सस्क्रतिकी आकांक्षाको हम अच्छे वीके कर्मको अपना सकते विशेषता है। 'यज्ञ' शब्द इमका एक उदाहरण है, हैं, और इससे वर्ण-व्यवस्थाका आघात पहुँच सकता वैदिक युगमें 'यज्ञ' का कुछ अर्थ था और विनावा
इसीलिय गीताम वा-विभागका आधार गुण जो के "भूमिदान यज्ञ" का अर्थ कुछ और है। हम और कर्म दोनोंको माना गया है । बुद्ध महावीर
लोग पुराने शब्दोंको जल्दी छोड़ना उतना पसन्द नहीं वर्ण विरोधी विचारों और विरागमूलक धर्मोंकी
करते जितना उसे नया अर्थ दे देना, पर जब हम छाप अनासक्ति कम योग पर अवश्य है।
गीता प्रवचनमें 'स्वधर्म' का व्यवहार करते हैं तब वर्ण-व्यवस्थाका प्राधार
क्या उसका पुराना अर्थ बदला जा सकता है ? तिलकशुरूमें वर्ण-व्यवस्था-आर्य-अनार्य या दासोंके ने स्वधर्मका अथ किया था 'स्व-विवेक व निश्वित्१ अश्याय 11 श्लोक ४२, ४ . २ रखोक ४८ कर्तव्य'। गाँधीजीने इसी अर्थको मानकर 'अनासक्त प. लोक,
कर्मयोग' की कपनाकी, गीतासे उसका संबन्ध