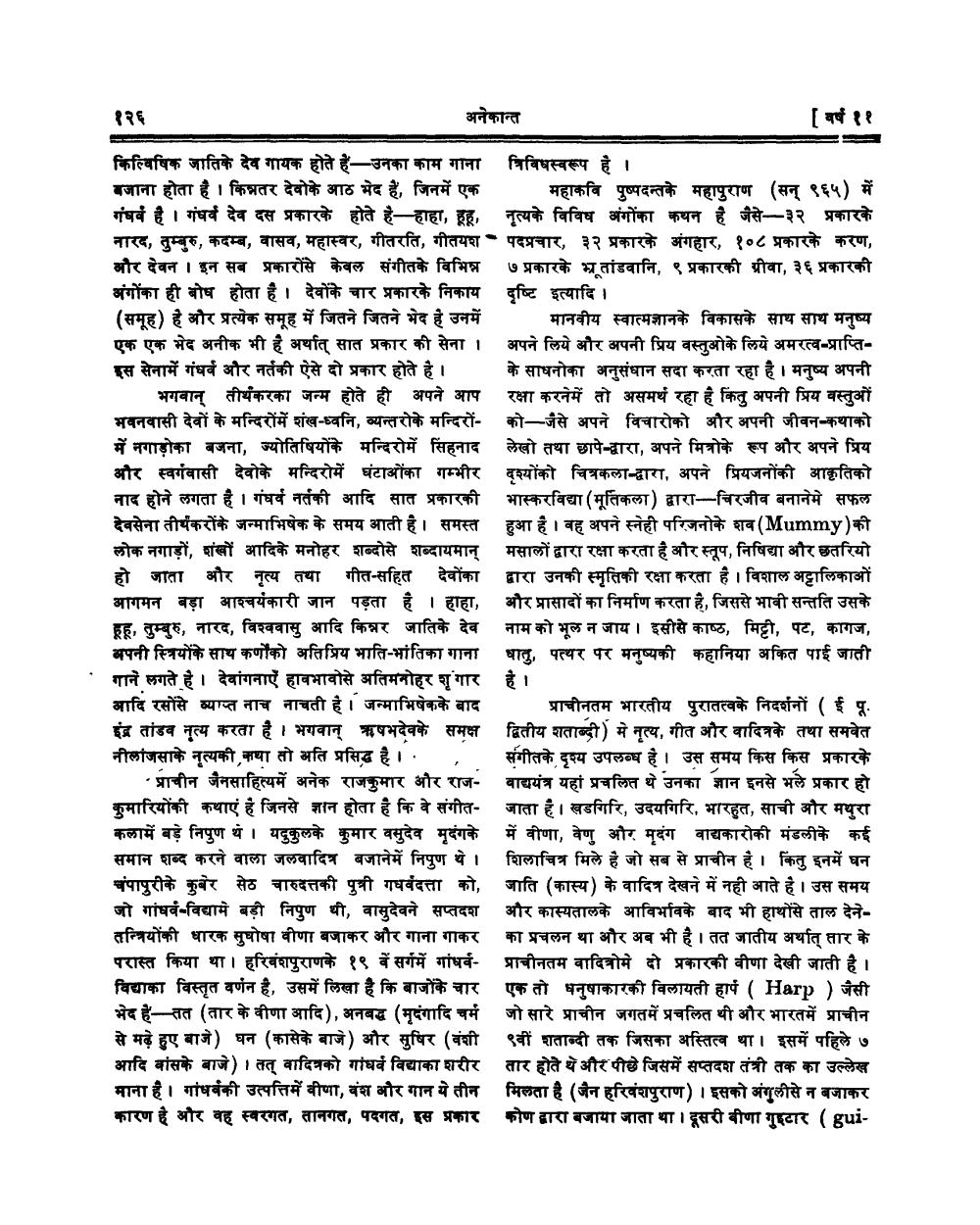________________
अनेकान्त
१२६
किल्विषक जातिके देव गायक होते हैं—उनका काम गाना बजाना होता है । किनतर देवोके आठ भेद हैं, जिनमें एक गंधर्व है। गंधर्व देव दस प्रकारके होते है- हाहा, इहू, नारद, तुम्बुरु, कदम्ब, वासव, महास्वर, गीतरति गीतयश और देवन । इन सब प्रकारोंसे केवल संगीतके विभिन्न अंगोंका ही बोध होता है । देवोंके चार प्रकारके निकाय (समूह) है और प्रत्येक समूह में जितने जितने भेद है उनमें एक एक भेद अनीक भी है अर्थात् सात प्रकार की सेना । इस सेनामें गंधर्व और नर्तकी ऐसे दो प्रकार होते है ।
भगवान् तीर्थंकरका जन्म होते ही अपने आप भवनवासी देवों के मन्दिरोंमें शंख-ध्वनि, व्यन्तरोके मन्दिरों में नगाड़ोका बजना, ज्योतिषियोंके मन्दिरोमें सिंहनाद और स्वर्गवासी देवोके मन्दिरोंमें घंटाजका गम्भीर नाद होने लगता है । गंधर्व नर्तकी आदि सात प्रकारकी देवसेना तीर्थंकरोंके जन्माभिषेक के समय आती है । समस्त लोक नगाड़ों, शंखों आदिके मनोहर शब्दोसे शब्दायमान् हो जाता और नृत्य तथा गीत - सहित देवोंका आगमन बड़ा आश्चर्यकारी जान पड़ता है । हाहा, इहू. तुम्बुरु, नारद, विश्ववासु आदि किन्नर जातिके देव अपनी स्त्रियोंके साथ कर्णोको अतिप्रिय भाति-भांतिका गाना गाने लगते है। देवांगनाएं हावभावोसे अतिमनोहर शृंगार आदि रसोंसे व्याप्त नाच नाचती है । जन्माभिषेकके बाद इंद्र तांडव नृत्य करता है । भगवान् ऋषभदेवके समक्ष नीलांजसा नृत्यकी, कथा तो अति प्रसिद्ध है।
प्राचीन जैनसाहित्यमें अनेक राजकुमार और राजकुमारियोंकी कथाएं है जिनसे ज्ञान होता है कि वे संगीतकलामें बड़े निपुण थे । यदुकुलके कुमार वसुदेव मृदंगके समान शब्द करने वाला जलवादित्र बजानेमें निपुण थे । चंपापुरीके कुबेर सेठ चारुदत्तकी पुत्री गधवंदता को जो गांधर्व विद्यामे बड़ी निपुण थी, वासुदेवने सप्तदश तन्त्रियोंकी धारक सुघोषा वीणा बजाकर और गाना गाकर परास्त किया था। हरिवंशपुराणके १९ में सर्गमें गांधर्वविद्याका विस्तृत वर्णन है, उसमें लिखा है कि बाजोंके चार भेद हैं—तत (तार के वीणा आदि), अनबद्ध ( मृदंगादि चर्म से मढ़े हुए बाजे) घन (कासेके बाजे) और सुषिर (वंशी आदि बांसके बाजे) । तत् वादित्रको गांधर्व विद्याका शरीर माना है। गांधर्वकी उत्पत्तिमें बीणा, वंश और गान वे तीन कारण है और वह स्वरगत, तानगत, पदगत, इस प्रकार
[ वर्ष ११
त्रिविधस्वरूप है ।
महाकवि पुष्पदन्तके महापुराण ( सन् ९६५ ) में नृत्यके विविध अंगोंका कथन है जैसे—३२ प्रकारके पदप्रचार, ३२ प्रकारके अंगहार, १०८ प्रकारके करण, ७ प्रकारके भ्रूतांडवानि, ९ प्रकारकी ग्रीवा, ३६ प्रकारकी दृष्टि इत्यादि ।
1
मानवीय स्वात्मज्ञानके विकासके साथ साथ मनुष्य अपने लिये और अपनी प्रिय वस्तुओके लिये अमरत्व-प्राप्तिके साधनोका अनुसंधान सदा करता रहा है। मनुष्य अपनी रक्षा करनेमें तो असमर्थ रहा है किंतु अपनी प्रिय वस्तुओं को — जैसे अपने विचारोको और अपनी जीवन - कथाको लेखो तथा छापे-द्वारा अपने मित्रोके रूप और अपने प्रिय बृश्योंको चित्रकला द्वारा अपने प्रियजनोंकी आकृतिको भास्करविद्या ( मूर्तिकला ) द्वारा -- चिरजीव बनानेमे सफल हुआ है। वह अपने स्नेही परिजनोके शव ( Mummy) की मसालों द्वारा रक्षा करता है और स्तूप, निषिद्या और छतरियो द्वारा उनकी स्मृतिको रक्षा करता है। विशाल अट्टालिकाओं और प्रासादों का निर्माण करता है, जिससे भावी सन्तति उसके नाम को भूल न जाय । इसीसे काष्ठ, मिट्टी, पट, कागज, धातु, पत्थर पर मनुष्यकी कहानिया अकित पाई जाती
है।
प्राचीनतम भारतीय पुरातत्वके निदर्शनों ( ई पू. द्वितीय शताब्दी) में नृत्य, गीत और वादिनके तथा समवेत संगीतके दृश्य उपलब्ध है । उस समय किस किस प्रकारके वाद्ययंत्र यहां प्रचलित थे उनका ज्ञान इनसे भले प्रकार हो जाता है खर्डागिरि, । खगिरि, उदयगिरि, भारहूत साची और मथुरा में वीणा, वेणु और मृदंग वाद्यकारोकी मंडलीके कई शिलाचित्र मिले है जो सब से प्राचीन है। किंतु इनमें धन जाति (कास्य) के वादित्र देखने में नही आते है। उस समय और कास्यतालके आविर्भावके बाद भी हाथोंसे ताल देनेका प्रचलन था और अब भी है । तत जातीय अर्थात् तार के प्राचीनतम वादिनोमे दो प्रकारकी वीणा देखी जाती है। एक तो धनुषाकारकी विलायती हार्प ( Harp ) जैसी जो सारे प्राचीन जगत में प्रचलित थी और भारतमें प्राचीन ९वीं शताब्दी तक जिसका अस्तित्व था। इसमें पहिले ७ तार होते थे और पीछे जिसमें सप्तदश तंत्री तक का उल्लेख मिलता है (जैन हरिबंशपुराण) । इसको अंगुली से न बजाकर कोण द्वारा बजाया जाता था। दूसरी बीणा गुरुवार (gui