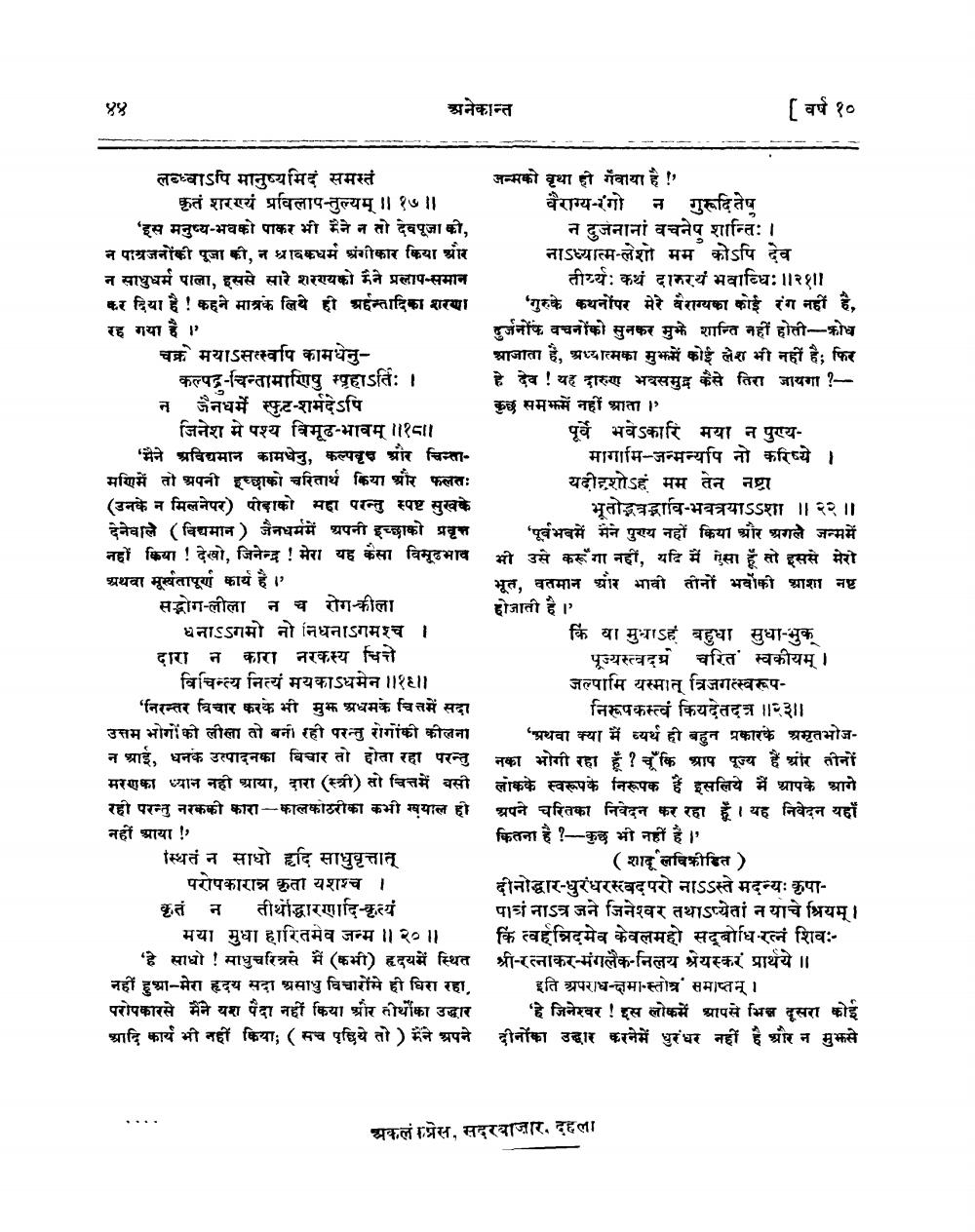________________
अनेकान्त
[वर्ष १०
%3
लब्ध्वाऽपि मानुष्यमिदं समस्तं
जन्मको वृथा हो गवाया है, कृतं शरण्यं प्रविलाप-तुल्यम् ॥ १७ ॥
वैराग्य-रंगो न गुरूदितेष 'इस मनुष्य-भवको पाकर भी मैंने न तो देवपूजा की,
न दुजनानां वचनेप शान्तिः । न पायजनोंकी पूजा की, न श्रावकधर्म अंगीकार किया और नाऽध्यात्म-लेशो मम कोऽपि देव न साधुधर्म पाला, इससे सारे शरण्यको मैंने प्रलाप-समान
तीर्यः कथं दामरयं भवाब्धिः॥२॥ कर दिया है ! कहने मात्रके लिये ही अर्हन्तादिका शरणा 'गुरुके कथनोंपर मेरे वैराग्यका कोई रंग नहीं है, रह गया है।"
दुर्जनोंक वचनोंको सुनकर मुझे शान्ति नहीं होती-क्रोध चक्र मयाऽसत्स्वपि कामधेनु
श्राजाता है, अध्यात्मका मुझमें कोई लेश भी नहीं है। फिर कल्पद्रु-चिन्तामाणिषु स्पृहाऽतिः । हे देव ! यह दारुण भवसमुद्र कैसे तिरा जायगा ?न जैनधर्मे स्फुट-शर्मदेऽपि
कुछ समझमें नहीं पाता।। जिनेश मे पश्य विमूढ-भावम् ॥१८॥
पूर्वे भवेऽकारि मया न पुण्य'मैने अविद्यमान कामधेनु, कल्पवृक्ष और चिन्ता
मागामि-जन्मन्यपि नो करिष्ये । मणिमें तो अपनी इच्छाको चरितार्थ किया और फलतः यदीदशोऽहं मम तेन नष्टा (उनके न मिलनेपर) पोद्दाको महा परन्तु स्पष्ट सुखके
भूतोद्भवद्भावि-भवत्रयाऽऽशा ।।२२।। देनेवाले (विद्यमान) जैनधर्म में अपनी इच्छाको प्रवृत्त 'पूर्वभवमें मैने पुण्य नहीं किया और अगले जन्ममें नहीं किया ! देखो, जिनेन्द्र ! मेरा यह कैसा विमूढभाव भी उसे करूँगा नहीं, यदि में ऐसा हूँ तो इससे मेरो अथवा मूर्खतापूर्ण कार्य है।
भूत, वतमान और भावी तीनों भवोंकी पाशा नष्ट सद्भोग-लीला न च रोग-कीला
होजाती है। धनाऽऽगमो नो निधनागमश्च ।
किं या मुधाऽहं बहुधा सुधा-भुक् दारा न कारा नरकस्य चित्रे
पूज्यस्त्वदग्रं चरित स्वकीयम् । विचिन्त्य नित्यं मयकाऽधमेन ॥१॥
जल्पामि यस्मात् त्रिजगत्स्वरूप'निरन्तर विचार करके भी मुझ अधमके चित्तमें सदा
निरूपकस्त्वं कियदेतदत्र ॥२३॥ उत्तम भोगों को लीला तो बनी रही परन्तु रोगोंकी कीलना प्रथवा क्या मैं व्यर्थ ही बहुन प्रकारके अमृतभोजन प्राई, धनक उत्पादनका विचार तो होता रहा परन्तु नका भोगी रहा हैं? कि श्राप पूज्य हैं और तीनों मरणका ध्यान नही पाया, दारा (स्त्री) तो चित्तमें बसी लोकके स्वरूपके निरूपक हैं इसलिये मैं आपके आगे रही परन्तु नरककी कारा-कालकोठरीका कभी खयाल ही अपने चरितका निवेदन कर रहा है। यह निवेदन यहाँ नहीं आया।
कितना है ?-कुछ भी नहीं है।' स्थितं न साधो हदि साधुवृत्तात्
(शार्दूलविक्रीडित) परोपकारान्न कृता यशश्च ।
दीनोद्धार-धुरंधरस्वदपरो नाऽऽस्ते मदन्यः कृपाकृतं न तीर्थोद्धारणादि-कृत्यं
पात्र नाऽत्र जने जिनेश्वर तथाऽप्येतां न याचे श्रियम्। मया मुधा हारितमेव जन्म || २०॥ कि वहन्निदमेव केवलमहो सदबोधि-रत्नं शिव:'हे साधो ! माधुचरित्रसे में (कभी) हृदयमें स्थित श्री-रत्नाकर-मंगलैक-निलय श्रेयस्कर प्रार्थये ।। नहीं हुश्रा-मेरा हृदय सदा असाधु विचारोंसे ही घिरा रहा, इति अपराध-क्षमा-स्तोत्र समाप्तन् । परोपकारसे मैंने यश पैदा नहीं किया और तीर्थीका उद्धार 'हे जिनेश्वर ! इस लोकमें आपसे भिन्न दूसरा कोई श्रादि कार्य भी नहीं किया; (सच पूछिये तो) मैंने अपने दीनोंका उद्धार करने में धुरंधर नहीं है और न मुझसे
घरा रहा,
अकलंसप्रेस, सदरबाजार, दद्दला