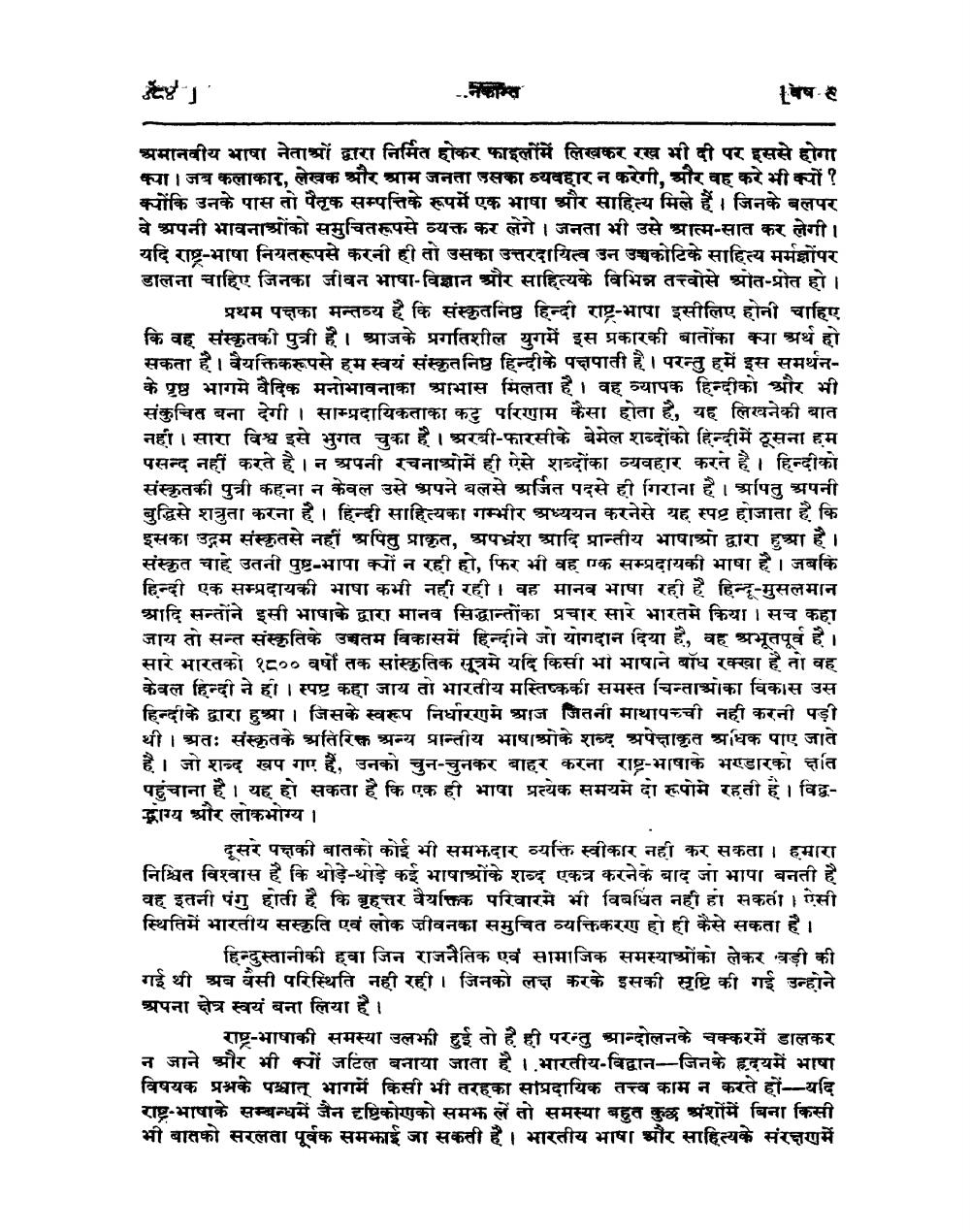________________
अमानवीय भाषा नेताओं द्वारा निर्मित होकर फाइलोंमें लिखकर रख भी दी पर इससे होगा क्या। जब कलाकार, लेखक और आम जनता उसका व्यवहार न करेगी, और वह करे भी क्यों ? क्योंकि उनके पास तो पैतृक सम्पत्तिके रूपमें एक भाषा और साहित्य मिले हैं। जिनके बलपर वे अपनी भावनाओंको समुचितरूपसे व्यक्त कर लेगे। जनता भी उसे आत्म-सात कर लेगी। यदि राष्ट्र-भाषा नियतरूपसे करनी ही तो उसका उत्तरदायित्व उन उच्चकोटिके साहित्य मर्मज्ञोपर डालना चाहिए जिनका जीवन भाषा-विज्ञान और साहित्यके विभिन्न तत्त्वोसे ओत-प्रोत हो।
प्रथम पक्षका मन्तव्य है कि संस्कृतनिष्ठ हिन्दी राष्ट्र-भाषा इसीलिए होनी चाहिए कि वह संस्कृतकी पुत्री है। श्राजके प्रगतिशील युगमें इस प्रकारकी बातोंका क्या अर्थ हो सकता है। वैयक्तिकरूपसे हम स्वयं संस्कृतनिष्ठ हिन्दीके पक्षपाती है। परन्तु हमें इस समर्थनके पृष्ठ भागमे वैदिक मनोभावनाका आभास मिलता है। वह व्यापक हिन्दीको और भी संकुचित बना देगी। साम्प्रदायिकताका कद परिणाम कैसा होता है, यह लिखनेकी बात नही । सारा विश्व इसे भुगत चुका है। अरबी-फारसीके बेमेल शब्दोंको हिन्दीमें ठूसना हम पसन्द नहीं करते है। न अपनी रचनाओमें ही ऐसे शब्दोंका व्यवहार करते है। हिन्दीको संस्कृतकी पुत्री कहना न केवल उसे अपने बलसे अर्जित पदसे ही गिराना है। अपितु अपनी बुद्धिसे शत्रुता करना है। हिन्दी साहित्यका गम्भीर अध्ययन करनेसे यह स्पष्ट होजाता है कि इसका उद्गम संस्कृतसे नहीं अपितु प्राकृत, अपभ्रंश आदि प्रान्तीय भाषाओं द्वारा हुआ है। संस्कृत चाहे उतनी पुष्ट-भापा क्यों न रही हो, फिर भी वह एक सम्प्रदायकी भाषा है। जबकि हिन्दी एक सम्प्रदायकी भाषा कभी नहीं रही। वह मानव भाषा रही है हिन्दू-मुसलमान
आदि सन्तोंने इसी भाषाके द्वारा मानव सिद्धान्तोंका प्रचार सारे भारतमे किया। सच कहा जाय तो सन्त संस्कृतिके उच्चतम विकासमें हिन्दीने जो योगदान दिया है, वह अभूतपूर्व है। सारे भारतको १८०० वर्षों तक सांस्कृतिक सूत्रमे यदि किसी भी भाषाने बाँध रक्खा है तो वह केवल हिन्दी ने ही । स्पष्ट कहा जाय तो भारतीय मस्तिष्ककी समस्त चिन्ताओका विकास उस हिन्दीके द्वारा हुश्रा। जिसके स्वरूप निर्धारणमे आज जितनी माथापच्ची नहीं करनी पड़ी थी। अतः संस्कृतके अतिरिक्त अन्य प्रान्तीय भाषाओके शब्द अपेक्षाकृत अधिक पाए जाते है। जो शब्द खप गए हैं, उनको चुन-चुनकर बाहर करना राष्ट्र-भाषाके भण्डारको क्षति पहुंचाना है। यह हो सकता है कि एक ही भाषा प्रत्येक समयमे दो रूपोमे रहती है। विद्वद्भाग्य और लोकभोग्य।
दूसरे पक्षकी बातको कोई भी समझदार व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। हमारा निश्चित विश्वास है कि थोड़े-थोड़े कई भाषाओंके शब्द एकत्र करने के बाद जो भापा बनती है वह इतनी पंगु होती है कि बृहत्तर वैयक्तिक परिवारमे भी विबधित नही हो सकती। ऐसी स्थितिमें भारतीय सस्कृति एवं लोक जीवनका समुचित व्यक्तिकरण हो ही कैसे सकता है।
हिन्दुस्तानीकी हवा जिन राजनैतिक एवं सामाजिक समस्याओंको लेकर बड़ी की गई थी अब वैसी परिस्थिति नही रही। जिनको लक्ष करके इसकी सृष्टि की गई उन्होने अपना क्षेत्र स्वयं बना लिया है।
राष्ट्र-भाषाकी समस्या उलझी हुई तो है ही परन्तु आन्दोलनके चक्करमें डालकर न जाने और भी क्यों जटिल बनाया जाता है। भारतीय विद्वान-जिनके हृदयमें भाषा विषयक प्रश्नके पश्चात् भागमें किसी भी तरहका सांप्रदायिक तत्त्व काम न करते हों-यदि राष्ट्र-भाषाके सम्बन्धमें जैन दृष्टिकोणको समझ लें तो समस्या बहुत कुछ अंशोंमें बिना किसी भी बासको सरलता पूर्वक समझाई जा सकती है। भारतीय भाषा और साहित्यके संरक्षणमें