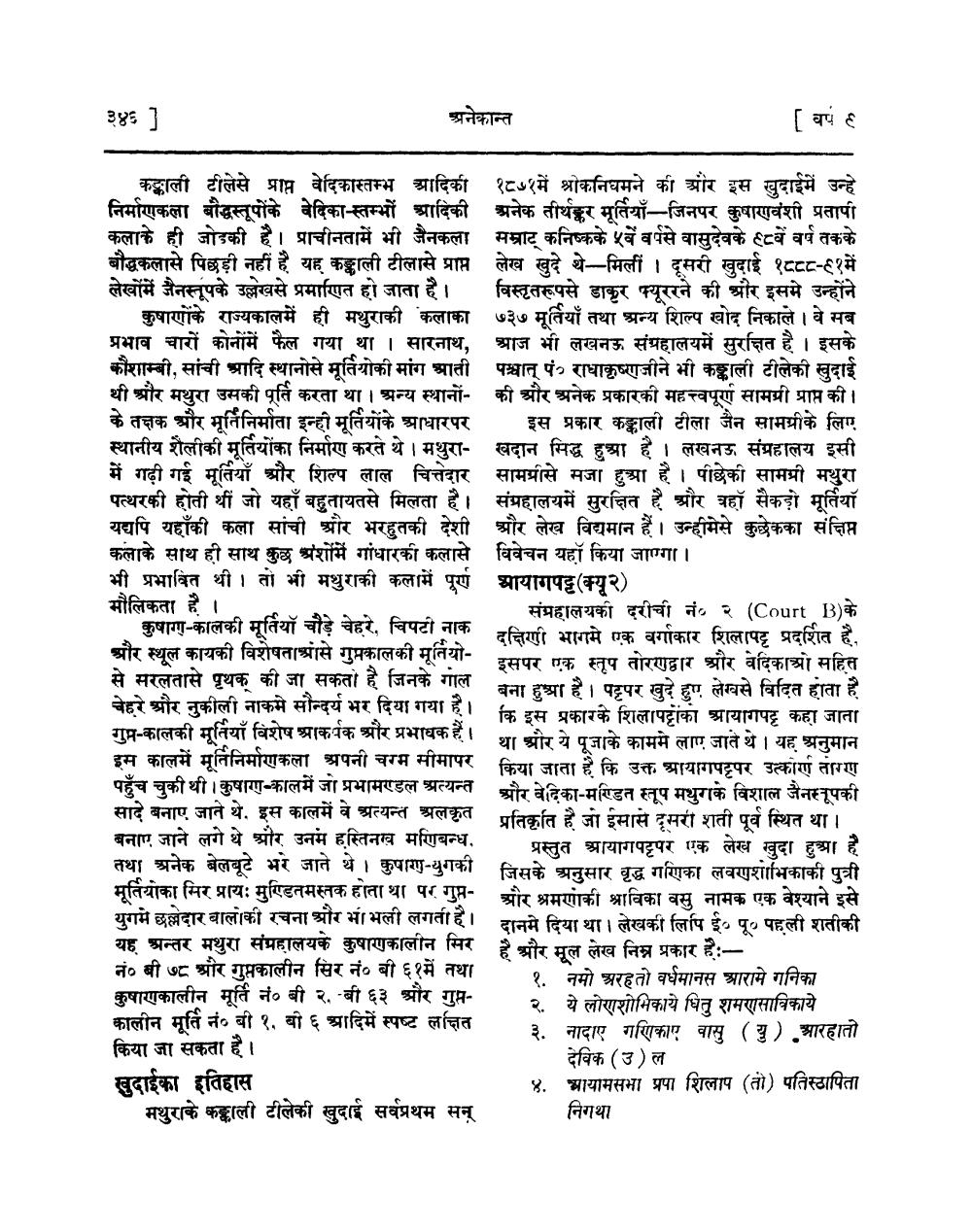________________
अनेकान्त
३४६ ]
कङ्काली टीलेसे प्राप्त वेदिकास्तम्भ आदिका निर्माणकला बौद्धस्तूपोंके वेदिका स्तम्भों आदिकी कला ही जोडकी है। प्राचीनतामें भी जैनकला बौद्धकलासे पिछड़ी नहीं है, यह कङ्काली टीलासे प्राप्त लेखोंमें जैनस्तूपके उल्लेख से प्रमाणित हो जाता है ।
कुषाणोंके राज्यकालमें ही मथुराकी कलाका प्रभाव चारों कोनोंमें फैल गया था । सारनाथ, कौशाम्बी, सांची आदि स्थानोसे मूर्तियोकी मांग आती थी और मथुरा उसकी पूर्ति करता था । अन्य स्थानों के तक्षक और मूर्तिनिर्माता इन्ही मूर्तियोंके आधारपर स्थानीय शैलीकी मूर्तियोंका निर्माण करते थे। मथुरामें गढ़ी गई मूर्तियाँ और शिल्प लाल चित्तेदार पत्थर की होती थीं यहाँ बहुतायतसे मिलता है । यद्यपि यहाँकी कला सांची और भरहुतकी देशी कला के साथ ही साथ कुछ अंशोंमें गांधारकी कलासे भी प्रभावित थी । तो भी मधुराकी कला में पूर्ण मौलिकता है ।
कुषाण-कालकी मूर्तियॉ चौड़े चेहरे, चिपटी नाक और स्थूल कायकी विशेषताओं से गुप्तकाल की मूर्तियो - से सरलता से पृथक की जा सकती है जिनके गाल चेहरे और नुकीली नाकमे सौन्दर्य भर दिया गया है। गुम-कालकी मूर्तियाँ विशेष आकर्षक और प्रभावक हैं । इस कालमें मूर्तिनिर्माणकला अपनी चरम सीमापर पहुँच चुकी थी। कुषाण कालमें जो प्रभामण्डल अत्यन्त सादे बनाए जाते थे. इस कालमें वे अत्यन्त अलकृत बनाए जाने लगे थे और उनमें हस्तिनख मणिबन्ध, तथा अनेक बेलबूटे भरे जाते थे । कुषाण युगकी मूर्तियोका मिर प्रायः मुण्डितमस्तक होता था पर गुप्तयुगमे छल्लेदार बालो की रचना और भां भली लगती है । यह अन्तर मथुरा संग्रहालयके कुषाणकालीन सिर नं० बी ७८ और गुप्तकालीन सिर नं० बी ६१में तथा कुषाणकालीन मूर्ति नं० बी २, बी ६३ और गुप्तकालीन मूर्ति नं० बी १, बी ६ आदिमें स्पष्ट लक्षित किया जा सकता है।
खुदाईका इतिहास
मथुरा कङ्काली टीकी खुदाई सर्वप्रथम सन्
[ वर्ष ह
१८७१ में लोकनिघमने की और इस खुदाई में उन्हे अनेक तीर्थङ्कर मूर्तियाँ - जिनपर कुषाणवंशी प्रतापी सम्राट कनिष्कके ५ वें वर्पसे वासुदेवके ह८वें वर्ष तक के लेख खुदे थे- मिलीं । दूसरी खुदाई १८८८-९१ में विस्तृतरूपसे डाकुर फ्यूररने की और इसमे उन्होंने ७३७ मूर्तियाँ तथा अन्य शिल्प खोद निकाले । वे सब आज भी लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है । इसके पश्चात् पं० राधाकृष्णजीने भी कङ्काली टीलेकी खुदाई की और अनेक प्रकारकी महत्त्वपूर्ण सामग्री प्राप्त की।
इस प्रकार कङ्काली टीला जैन सामग्री के लिए खदान सिद्ध हुआ है । लखनऊ संग्रहालय इसी सामग्री से सजा हुआ है । पीछेकी सामग्री मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है और वहाँ सैकड़ो मूर्तियाँ और लेख विद्यमान हैं। उन्हीमेसे कुछेकका संक्षिप्त विवेचन यहाँ किया जाएगा । श्रायागपट्ट (क्यू२)
संग्रहालयकी दरीची नं० २ ( Court B) के दक्षिणी भागमे एक वर्गाकार शिलापट्ट प्रदर्शित है, इसपर एक स्तूप तोरणद्वार और वेदिकाओ सहित कि इस प्रकार के शिलापट्टाका आया कहा बना हुआ है। पट्टपर खुदे हुए लेखसे विदित होता है था और ये पूजाके काममे लाए जाते थे । यह अनुमान किया जाता है कि उक्त श्रायागपट्टपर उत्कीर्ण ताग्या और वेदिका - मण्डित स्तूप मथुरा के विशाल जैनस्नूपकी प्रतिकृति है जो ईसासे दूसरी शती पूर्व स्थित था ।
प्रस्तुत आयागपट्ट पर एक लेख खुदा हुआ है जिसके अनुसार वृद्ध गरिणका लवणशोभिकाकी पुत्री और श्रमणांकी श्राविका वसु नामक एक वेश्याने इसे दानमे दिया था। लेखकी लिपि ई० पू० पहली शतीकी हैं और मूल लेख निम्न प्रकार है:
२.
१. नमो अरहतो वर्धमानस श्रारामे गनिका ये लोणशोभिकाये धितु शमणसाविकाये नादाए गणिकाए वासु (यु) आरहातो देविक (3 ) ल
३.
४. प्रायामसभा प्रपा शिलाप (तो) पतिस्ठापिता
निगथा