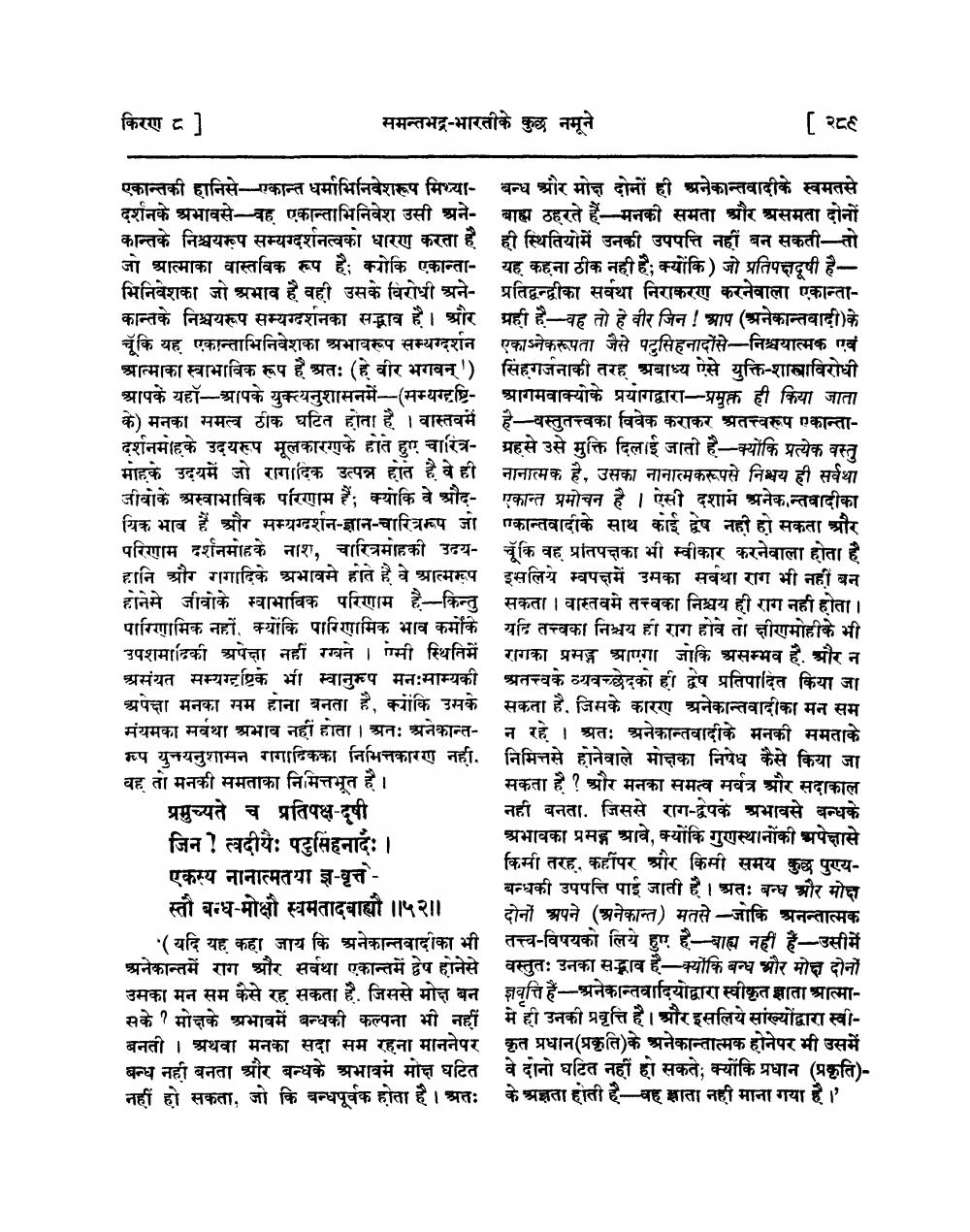________________
समन्तभद्र - भारती के कुछ नमूने
किरण ८ ]
एकान्तकी हानिसे - एकान्त धर्माभिनिवेशरूप मिथ्यादर्शनके प्रभावसे वह एकान्ताभिनिवेश उसी अनेकान्तके निश्चयरूप सम्यग्दर्शनत्वको धारण करता है जो श्रात्माका वास्तविक रूप क्योकि एकान्ताभिनिवेशका जो अभाव है वही उसके विरोधी अने कान्तके निश्चयरूप सम्यग्दर्शनका सद्भाव है। और चूँकि यह एकान्ताभिनिवेशका अभावरूप सम्यग्दर्शन श्रमका स्वाभाविक रूप है अतः (हे वीर भगवन् ) आपके यहाँ आपके युक्त्यनुशासनमें - ( सम्यग्दृष्टिके) मनका समत्व ठीक घटित होता है । वास्तवमें दर्शनमोहके उदयरूप मूलकारणके होते हुए चारित्रमोहके उदयमें जो रागादिक उत्पन्न होते है वे ही जीवीके अस्वाभाविक परिणाम हैं; क्योकि वे औदfra भाव हैं और सम्यग्दर्शन- ज्ञान - चारित्ररूप जो परिणाम दर्शनमोहके नाश, चारित्रमोहकी उदय हानि और गगादिके अभाव से होते है वे आत्मरूप होनेमे जीवोके स्वाभाविक परिणाम है- किन्तु पारिणामिक नहीं, क्योंकि पारिणामिक भाव कर्मोके उपशमादिकी अपेक्षा नहीं रखते। ऐसी स्थिति में असंयत सम्यग्दृष्टिके भी स्वानुरूप मनः साम्यकी अपेक्षा मनका सम होना बनता है, क्योंकि उसके संयमका सर्वथा अभाव नहीं होता । अतः अनेकान्तरूप युभ्यनुशासन गंगादिकका निमित्तकारण नहीं. वह तो मनकी समताका निमित्तभूत है ।
प्रमुच्यते च प्रतिपक्ष-दुषी जिन ! त्वदीयैः पटुसिंहनादैः । एकस्य नानात्मतया ज्ञ- वृत्त े -
बन्ध-मोक्ष स्वमतादबाह्यौ ॥ ५२ ॥
( यदि यह कहा जाय कि अनेकान्तवादीका भी अनेकान्त राग और सर्वथा एकान्तमें द्वेष होनेसे उसका मन सम कैसे रह सकता है. जिससे मोक्ष बन सके ? मोक्षके अभाव में बन्धकी कल्पना भी नहीं बनती | अथवा मनका सदा सम रहना माननेपर बन्ध नही बनता और बन्धके अभावमं मोक्ष घटित नहीं हो सकता, जो कि बन्धपूर्वक होता है । अतः
[ २८६
बन्ध और मोक्ष दोनों ही अनेकान्तवादीके स्वमतसे बाह्य ठहरते हैं—मनकी समता और असमता दोनों ही स्थितियो में उनकी उपपत्ति नहीं बन सकती - तो यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि ) जो प्रतिपक्षदूषी हैप्रतिद्वन्द्वीका सर्वथा निराकरण करनेवाला एकान्तायही है - वह तो हे वीर जिन ! आप (अनेकान्तवादी) के एकानेकरूपता जैसे पटुसिहनादोंसे - निश्चयात्मक एवं सिंहगर्जनाकी तरह अबाध्य ऐसे युक्ति - शास्त्राविरोधी आगमवाक्योके प्रयोगद्वारा - प्रमुक्त ही किया जाता है— वस्तुतत्त्वका विवेक कराकर तत्त्वरूप एकान्ताग्रहसे उसे मुक्ति दिलाई जाती है- क्योंकि प्रत्येक वस्तु नानात्मक है, उसका नानात्मकरूपसे निश्चय ही सर्वथा एकान्त प्रमोचन है । ऐसी दशाम अनेक, न्तवादीका एकान्तवादीके साथ कोई द्वेष नही हो सकता और चूँकि वह प्रतिपक्षका भी स्वीकार करनेवाला होता है। इसलिये स्वपक्षमें उसका सर्वथा राग भी नहीं बन सकता । वास्तवमे तत्त्वका निश्चय ही राग नहीं होता । यदि तत्त्वका निश्चय ही राग होवे तो क्षीणमोहीके भी
का प्रसङ्ग आएगा जोकि असम्भव है. और न तत्त्वके व्यवच्छेदको ही द्वेष प्रतिपादित किया जा सकता है, जिसके कारण अनेकान्तवादीका मन सम न रहे । अतः अनेकान्तवादीके मनकी ममता के निमित्तसे होनेवाले मोक्षका निषेध कैसे किया जा सकता है ? और मनका समत्व सर्वत्र और सदाकाल नही बनता. जिससे राग-द्वेपके प्रभावसे बन्धके अभावका प्रसङ्ग श्रावे, क्योंकि गुणस्थानोंकी अपेक्षासे किसी तरह, कहीं और किसी समय कुछ पुण्यबन्धकी उपपत्ति पाई जाती है। अतः बन्ध और मोक्ष दोनों अपने ( अनेकान्त) मतसे - जोकि अनन्तात्मक तत्त्व विषयको लिये हुए है - बाह्य नहीं हैं— उसीमें वस्तुतः उनका सद्भाव है- क्योंकि बन्ध और मोक्ष दोनों ज्ञवृत्ति हैं — अनेकान्तवादियोद्वारा स्वीकृत ज्ञाता श्रात्मामें ही उनकी प्रवृत्ति है । और इसलिये सांख्योंद्वारा स्वीकृत प्रधान (प्रकृति) के अनेकान्तात्मक होनेपर भी उसमें वे दोनो घटित नहीं हो सकते; क्योंकि प्रधान (प्रकृति) - के अता होती है वह ज्ञाता नही माना गया है।'