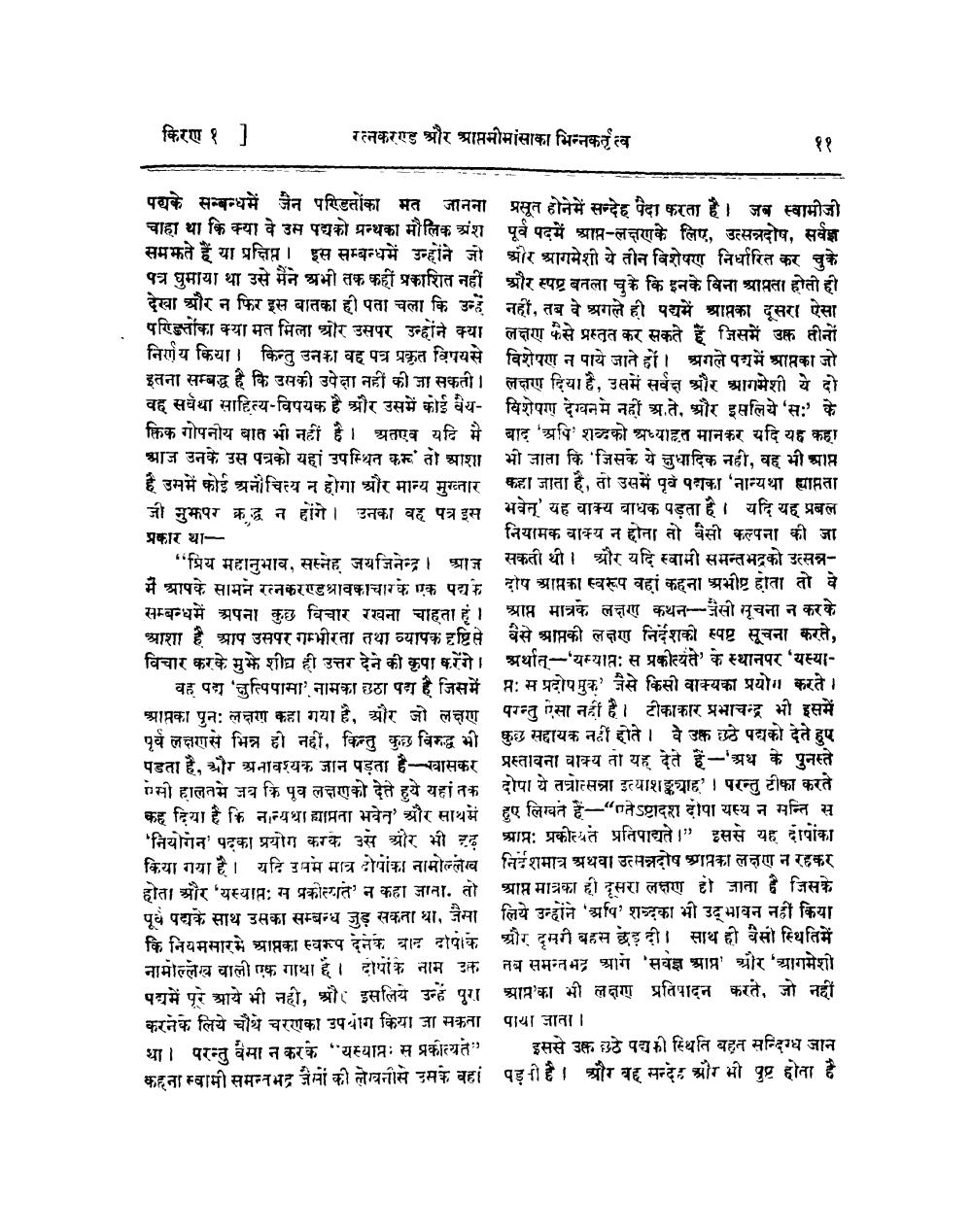________________
किरण १ ]
पथके सम्बन्ध में जेन पण्डितोंका मत जानना चाहा था कि क्या वे उस पथको प्रन्थका मौलिक अंश समझते हैं या प्रक्षिप्त इस सम्बन्धमें उन्होंने जो
रत्नकरण्ड और प्तमीमांसाका भिन्नकर्तृत्व
पत्र घुमाया था उसे मैंने अभी तक कहीं प्रकाशित नहीं देखा और न फिर इस बातका ही पता चला कि उन्हें परितका क्या मत मिला और उसपर उन्होंने क्या निर्णय किया। किन्तु उनका वह पत्र प्रकृत विषय से इतना सम्बद्ध है कि उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वद्द वह सर्वथा साहित्य विषयक है और उसमें कोई वेवफिफ गोपनीय बात भी नहीं है। अतएव यदि मे आज उनके उस पत्रको यहां उपस्थित कम तो आशा हैं उसमें कोई अनौचित्य न होगा और मान्य मुख्तार जी मुझपर क्रुद्ध न होंगे। उनका वह पत्र इस
प्रकार था-
"प्रिय महानुभाव, सस्नेह जयजिनेन्द्र | आज मैं आपके सामने रत्नकरण्ड श्रावकाचार के एक सम्बन्ध में अपना कुछ विचार रखना चाहता हूँ । आशा है आप उसपर गम्भीरता तथा व्यापक दृष्टि से विचार करके मुझे शीघ्र ही उत्तर देने की कृपा करेंगे
वह पद्य 'चुत्पिपासा' नामका छठा पद्म है जिसमें आप्तका पुन: लक्षण कहा गया है, और जो लक्षण पूर्व लक्षण से भिन्न हो नहीं, किन्तु कुछ विरुद्ध भी पडता है, और अनावश्यक जान पड़ता है-खासकर ऐसी हालत में जय कि पूर्व लक्षणको देते हुये यहां तक कह दिया है कि नया द्यामता भवेत' और साथ में 'नियोगेन पदका प्रयोग करके उसे और भी एड किया गया है। यदि उसमें मात्र दोपों का नामोल्लेख होता और 'यस्याप्तः स प्रकोत्यते' न कहा जाता. तो पूर्व पथके साथ उसका सम्बन्ध जुड़ सकता था. जैसा कि नियमसारमे आप्तका स्वरूप देनेके बाद दीपक नामोल्लेख वाली एक गाथा है। दोपांक नाम उक्त पद्य में पूरे आये भी नहीं, और इसलिये उन्हें पूरा करनेके लिये चौथे चरण का उपयोग किया जा सकता था। परन्तु वैसा न करके "यस्यातः स प्रकीत्यते" कहना स्वामी समन्तभद्र जैसों की लेखनीसे उसके वहां
११
प्रसूत होनेमें सन्देह पैदा करता है। जब स्वामीजी पूर्व पदमें आम लक्षण के लिए, उसनदोष, सर्वज्ञ और आगमेशी वे तीन विशेषण निर्धारित कर चुके और स्पष्ट बतला चुके कि इनके विना श्रातता होती ही नहीं, तब वे अगले ही पयमें चातका दूसरा ऐसा लक्षण कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें उक्त तीनों विशेषण न पाये जाते हों। अगले पद्य में श्राप्तका जो लक्षण दिया है, उसमें सर्वज्ञ और आगमेशी ये दो विशेषण देखन में नहीं अते. और इसलिये 'सः' के बाद 'अपि शब्दको अभ्याहत मानकर यदि यह कहा भी जाता कि जिसके ये शुभादिक नही, यह भी बत कहा जाता है, तो उसमें पूर्व पद्यका 'नान्यथा ह्याप्तता भवेत्' यह वाक्य बाधक पड़ता है । यदि यह प्र नियामक वाक्य न होना तो वैसी कल्पना की जा सकती थी । और यदि स्वामी समन्तभद्रको उत्सन्नदो स्वरूप वहां कहना अभीए होता तो वे आप्त मात्रके लक्षण कथन-जैसी सूचना न कर के वैसे आपकी लक्षण निर्देशकी स्पष्ट सूचना करते, अर्थात् 'यम्यानः स प्रकोश्यते' के स्थानपर 'यस्थाप्रः स प्रदोष मुक' जैसे किसी वाक्यका प्रयोग करते । परन्तु ऐसा नहीं है। टीकाकार प्रभाचन्द्र भी इसमें कुछ सहायक नहीं होते। वे उक्त छठे पद्यको देते हुए प्रस्तावना वाक्य तो यह देते हैं- 'अथ के पुनस्ते दोषा ये तत्रोत्सना इत्याशङ्कया परन्तु टीका करते हुए लिखते हैं- “तेादश दोपा यस्य न सन्ति स प्राप्तः प्रकीत्यंत प्रतिपाद्यते ।" इससे यह दोपका निर्देशमात्र अथवा उत्सन्नदोष प्राप्तका लक्षण न रहकर श्राप्त मात्रका ही दूसरा लक्षण हो जाता है जिसके लिये उन्होंने 'अधि' शब्दका भी उद्भावन नहीं किया और दूसरी बहस छेड़ दी। साथ ही वैसी स्थिति में तब समन्तभद्र आगे 'सर्वज्ञ आप्त' और 'आगमेशी आत का भी लक्षण प्रतिपादन करते, जो नहीं
पाया जाता।
इससे उस छठे पची स्थिति बहुत सन्दिग्ध जान पड़ती है । और वह सन्देह और भी पुष्ट होता है