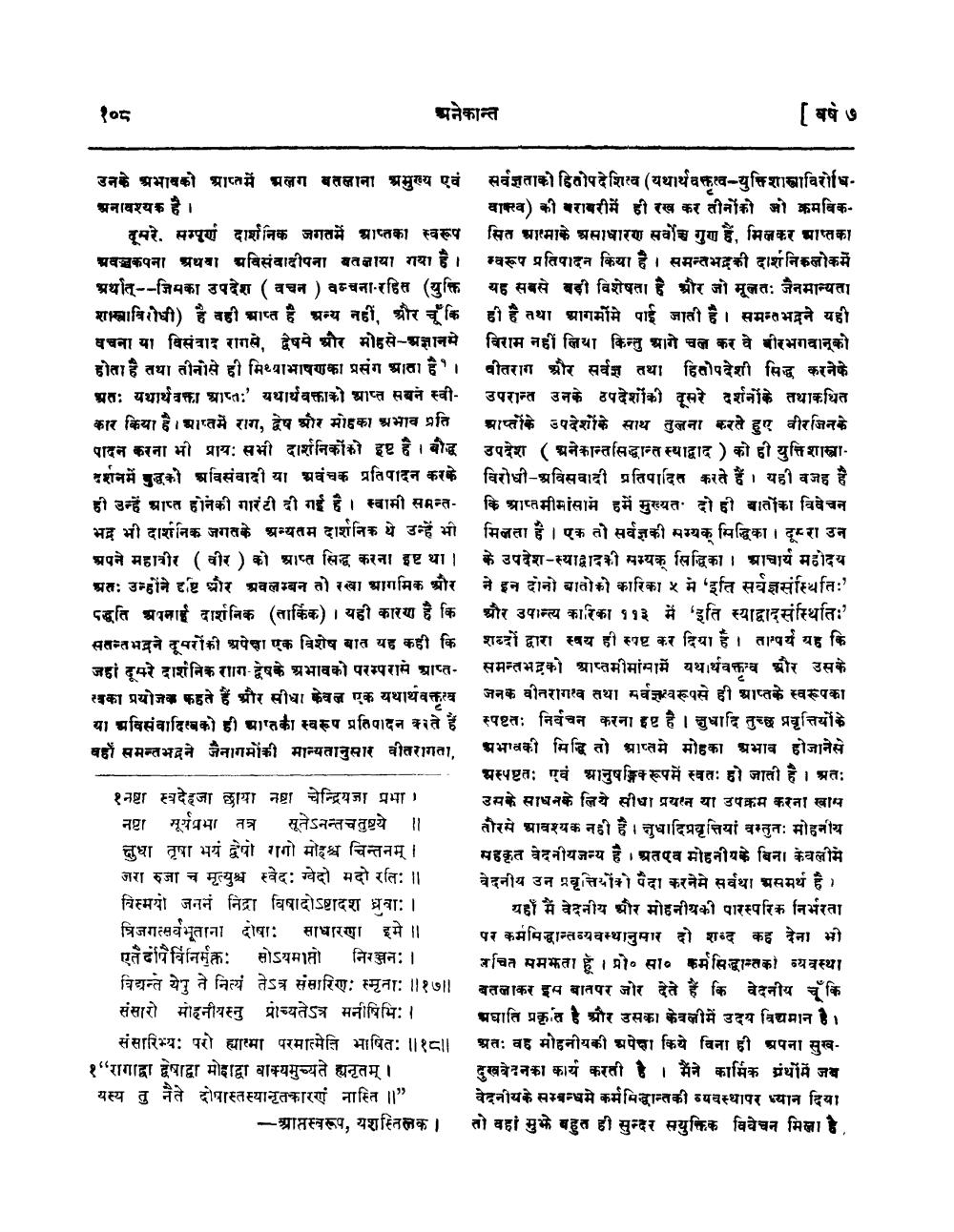________________
१०८
अनेकान्त
[वर्ष ७
उनके प्रभावको प्राप्त में अलग बतलाना अमुख्य एवं सर्वज्ञताको हितोपदेशित्व (यथार्थवक्तृत्व-युक्तिशास्त्राविरोधि. अनावश्यक है।
____वाक्रव) की बराबरीमें ही रख कर तीनोंको जो क्रमविकदूमरे. सम्पूर्ण दार्शनिक जगतमें प्राप्तका स्वरूप सित प्रारमाके असाधारण सर्वोच्च गुण हैं, मिलकर प्राप्तका अवञ्चकपना अथवा अविसंवादीपना बताया गया है। म्वरूप प्रतिपादन किया है। समन्तभद्रकी दार्शनिकलोकमें अर्थात्--जिमका उपदेश (वचन ) वचना-रहिस (युक्ति यह सबसे बड़ी विशेषता है और जो मूलत: जैनमान्यता शास्त्राविरोधी) है वही प्राप्त है अन्य नहीं, और चूँ कि ही है तथा प्रागोमे पाई जाती है। समन्तभदने यही बचना या विसंवाद राग, द्वेषसे और मोहसे-अज्ञानमे विराम नहीं लिया किन्तु भागे चल कर वे बीरभगवान्को होता है तथा तीनोसे ही मिथ्याभाषणका प्रसंग पाता है। वीतराग और सर्वज्ञ तथा हितोपदेशी सिद्ध करनेके अतः यथार्थवक्ता प्राप्त:' यथार्थवक्ताको प्राप्त सबने स्वी- उपरान्त उनके उपदेशोंकी दूसरे दर्शनोंके तथाकथित कार किया है। प्राप्तमें राग, द्वेष और मोहका प्रभाव प्रति प्राप्तोंके उपदेशोंके साथ तुलना करते हुए वीरजिनके पादन करना भी प्राय: सभी दार्शनिकोंको इष्ट है । बौद्ध उपदेश (अनेकान्तसिद्धान्त स्याद्वाद ) को ही युति शास्त्रादर्शनमें बुद्धको अविसंवादी या अवंचक प्रतिपादन करके विरोधी-अविसवादी प्रतिपादित करते हैं। यही वजह है ही उन्हें प्राप्त होनेकी गारंटी दी गई है। स्वामी समन्त- कि श्राप्तमीमांसामे हमें मुख्यतः दो ही बातोंका विवेचन भद्र भी दार्शनिक जगतके अन्यतम दार्शनिक थे उन्हें भी मिलता है । एक तो सर्वज्ञकी मम्यक् मिद्धिका । दूसरा उन अपने महावीर ( वीर ) को प्राप्त सिद्ध करना इष्ट था। के उपदेश-स्यावादकी सम्यक् सिद्धिका । प्राचार्य महोदय अत: उन्होंने दृष्टि और अवलम्बन तो रखा श्रागमिक और ने इन दोनो बातोको कारिका ५ मे 'इति सर्वज्ञसंस्थितिः' पद्धति अपनाई दार्शनिक (तार्किक)। यही कारण है कि और उपान्त्य कारिका ११३ में 'इति स्याद्वादसंस्थितिः' सतन्तभद्रने दूसरों की अपेक्षा एक विशेष बात यह कही कि शब्दों द्वारा स्वय ही स्पष्ट कर दिया है। तापर्य यह कि जहां दूपरे दार्शनिक राग-द्वेषके प्रभावको परम्परासे प्राप्त- समन्तभद्रको प्राप्तमीमांसामें यथार्थवक्तव और उसके स्वका प्रयोजक कहते हैं और सीधा केवल एक यथार्थवक्तत्व जनक वीतरागव तथा सर्वज्ञस्वरूपसे ही प्राप्तके स्वरूपका या अविसंवादिषको ही भारतका स्वरूप प्रतिपादन करते हैं स्पष्टतः निर्वचन करना इष्ट है । सुधादि तुच्छ प्रवृत्तियों के वहाँ समन्तभद्रने जैनागमोंकी मान्यतानुसार वीतरागता, प्रभावकी सिद्धि तो प्राप्तमे मोहका प्रभाव होजानेसे
अस्पष्टतः एवं भानुषङ्गिक रूपमें स्वतः हो जाती है। अत: १नष्टा स्वदेहजा छाया नष्टा चेन्द्रियजा प्रभा। उसके साधनके लिये सीधा प्रयत्न या उपक्रम करना खाप नष्टा मूर्यप्रभा तत्र सूतेऽनन्त चतुष्टये ॥ तौरसे आवश्यक नहीं है। नुधादिप्रवृत्तियां वस्तुतः मोहनीय क्षुधा तृषा भयं द्वषो गगो मोहश्च चिन्तनम् । सहकृत वेदनीयजन्य है । अतएव मोहनीयके बिना केवलीमें जरा रुजा च मृत्युश्च स्वेद: ग्वेदो मदो रतिः ।।
वेदनीय उन प्रवृत्तियों को पैदा करनेमे सर्वथा असमर्थ है। विस्मयो जननं निद्रा विषादोऽष्टादश ध्रवाः ।
यहाँ मैं वेदनीय और मोहनीयकी पारस्परिक निर्भरता त्रिजगत्सर्वभूताना दोषा: साधारणा इमे ।।
पर कममिद्धान्तव्यवस्थानुमार दो शब्द कह देना भी एतदोपैविनिर्मक्तः सोऽयमातो निरञ्जनः।
अचित समझता है। प्रो. सा. कर्मसिद्धान्तको व्यवस्था विद्यन्तं ये ते नित्यं तेऽत्र संसारिणः स्मृताः ॥१७॥ बतलाकर इस बातपर जोर देते हैं कि वेदनीय चकि संसारो मोहनीयस्नु प्रोच्यतेऽत्र मनीषिभिः ।
प्रघाति प्रकृति है और उसका केवलीमें उदय विद्यमान है। संसारिभ्य: परो ह्यारमा परमात्मेति भाषितः ॥१८॥ अत: वह मोहनीयकी अपेक्षा किये बिना ही अपना सुख१"रागाद्वा द्वेषाद्वा मोहाद्वा वाक्यमुच्यते ह्यनृतम् । दुखवेदनका कार्य करती है। मैंने कार्मिक ग्रंथों में जब यस्य तु नैते दोषास्तस्यानृतकारणं नास्ति ॥" वेदनीयके सम्बन्धमे कर्ममिद्धान्तकी व्यवस्थापर ध्यान दिया
-श्राप्तस्वरूप, यशस्तिलक। तो वहां मुझे बहुत ही सुन्दर सयुक्तिक विवेचन मिला है,