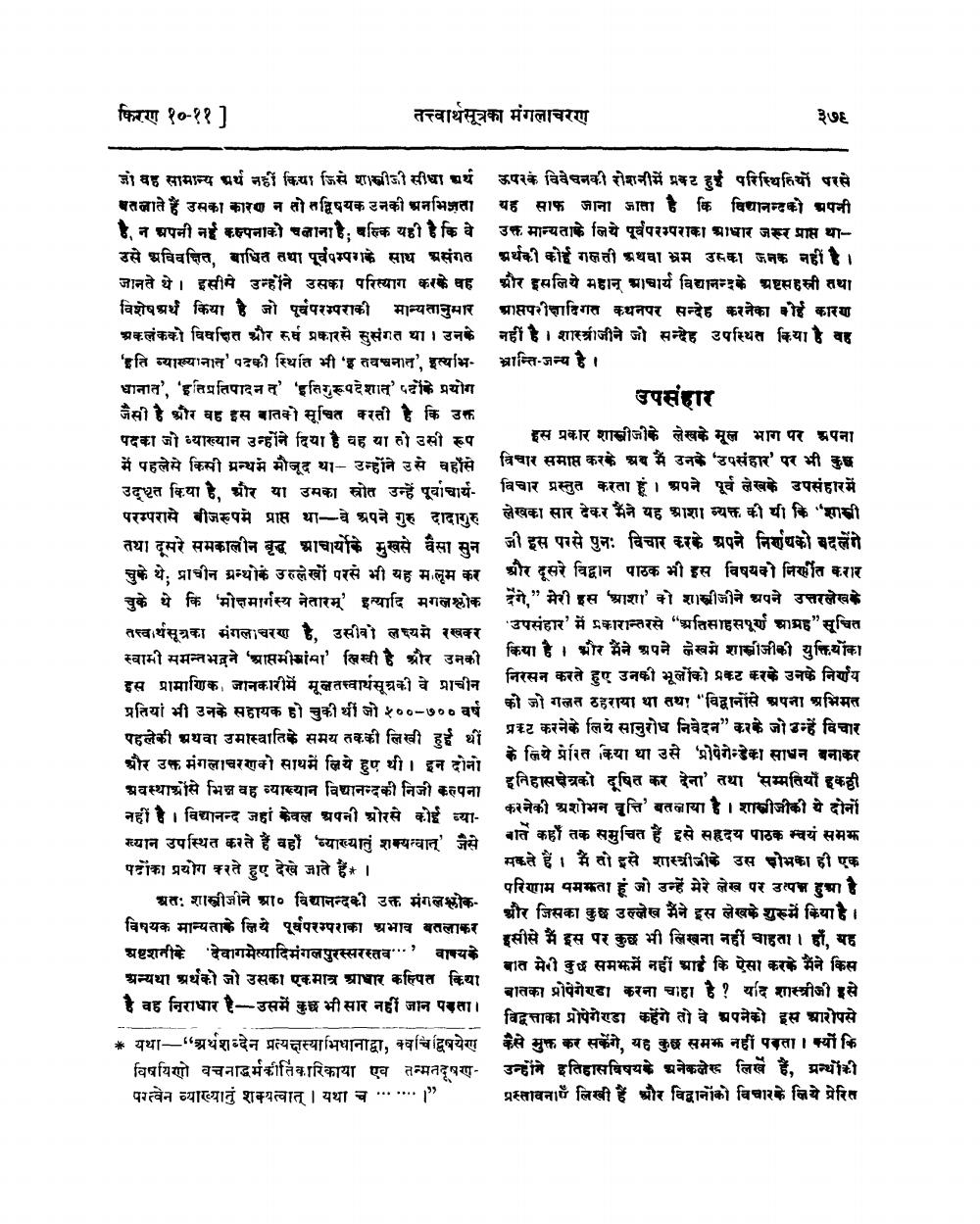________________
फिरण १०-११]
तत्त्वार्थसूत्रका मंगलाचरण
३७६
जो वह सामान्य अर्थ नहीं किया जिसे शास्त्रीजी सीधा अर्थ उपरक विवेचनकी रोशनी में प्रकट हुई परिस्थितियों परसे बतलाते हैं उसका कारण न तो तद्विषयक उनकी अनभिजता यह साफ जाना जाता है कि विद्यानन्दको अपनी है, न अपनी नई कल्पनाको चलाना है, बल्कि यही है कि वे उक्त मान्यताके लिये पूर्वपरम्पराका श्राधार जरूर प्राप्त थाउसे अविवक्षित, बाधित तथा पूर्वपम्पके साथ असंगत अर्थकी कोई गलती अथवा भ्रम उसका जनक नहीं है। जानते थे। इसीमे उन्होंने उसका परित्याग करके वह और इसलिये महान् प्राचार्य विद्यानन्दके अष्टसहस्री तथा विशेष अर्थ किया है जो पूर्वपरम्पराकी मान्यतानुमार प्राप्तपरीक्षादिगत कथनपर सन्देह करनेका कोई कारण अकलंकको विवक्षित और रूर्व प्रकारसे सुसंगत था। उनके नहीं है। शास्त्रीजीने जो सन्देह उपस्थित किया है वह 'इति व्याख्यानात' पदकी स्थिति भी 'इ तवचनात', इत्यभि- भ्रान्ति-जन्य है। धानात', 'इतिप्रतिपादन त्' 'इतिगुरूपदेशात्' पदोंके प्रयोग
उपसंहार जैसी है और वह इस बातको सूचित करती है कि उक्त पदका जो व्याख्यान उन्होंने दिया है वह या तो उसी रूप
इस प्रकार शास्त्रीजीके लेखके मूल भाग पर अपना में पहलेसे किसी अन्य मौजूद था- उन्होंने उसे वहाँसे विचार समाप्त करके अब मैं उनके 'उपसंहार' पर भी कुछ उदृत किया है, और या उसका स्रोत उन्हें पूर्वाचार्य- विचार प्रस्तुत करता हूं। अपने पूर्व लेखके उपसंहार में परम्परासे बीजरूपमै प्राप्त था-वे अपने गुरु दादागुरु लेखका सार देकर मैंने यह प्राशा व्यक्त की थी कि "शास्त्री तथा दूसरे समकालीन बृद्ध प्राचार्योके मुखसे वैसा सन जी इस परसे पुनः विचार करके अपने निर्णयको बदलेंगे चुके थे प्राचीन ग्रन्थोके उल्लेखों परसे भी यह मालूम कर और दूसरे विद्वान पाठक भी इस विषयको निति करार चुके थे कि 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्' इत्यादि मगलश्लोक देंगे," मेरी इस 'आशा' को शास्त्रीजीने अपने उत्तरलेखक तत्वार्थसूत्रका मंगलाचरण है, उसीवो लक्ष्य में रखकर
'उपसंहार' में प्रकारान्तरसे "अतिसाहसपूर्ण भाग्रह" सूचित स्वामी समन्तभनने 'प्राप्तमीमांसा' विस्वी है और उनकी
किया है। और मैंने अपने लेखमे शास्त्रीजीकी युक्तियोंका इस प्रामाणिक जानकारीमें मूलतत्त्वार्थसूत्रकी वे प्राचीन
निरसन करते हुए उनकी भूलोको प्रकट करके उनके निर्णय प्रतियां भी उनके सहायक हो चुकी थीं जो ५००-७०० वर्ष
को जो गलत ठहराया था तथा "विद्वानोंसे अपना अभिमत पहलेकी अथवा उमास्वातिके समय तककी लिखी हुई थीं
प्रकट करनेके लिये सानुरोध निवेदन" करके जो उन्हें विचार और उक्त मंगलाचरणको साथमें लिये हुए थी। इन दोनो
के लिये प्रेरित किया था उसे 'प्रोपेगेन्डेका साधन बनाकर अवस्थाओंसे भिन्न वह व्याख्यान विद्यानन्दकी निजी कल्पना
इतिहासक्षेत्रको दूषित कर देना' तथा 'सम्मतियों इकठ्ठी नहीं है। विद्यानन्द जहां केवल अपनी पोरसे कोई व्या
करनेकी अशोभन वृत्ति' बतलाया है। शास्त्रीजीकी ये दोनों ख्यान उपस्थित करते हैं वहीं 'व्याख्यातुं शक्यन्वात्' जैसे
बात कहाँ तक समुचित हैं इसे सहृदय पाठक स्वयं समझ पदोंका प्रयोग करते हुए देखे जाते हैं ।
सकते हैं। मैं तो इसे शास्त्रीजीके उस चोभका ही एक
परिणाम पममता हूं जो उन्हें मेरे लेख पर उत्पन्न हुआ है अत: शास्त्रीजीने प्रा. विद्यानन्दकी उक्त मंगलश्लोक
और जिसका कुछ उल्लेख मैंने इस लेखके शुरूमें किया है। विषयक मान्यताके लिये पूर्वपरम्पराका प्रभाव बतलाकर
इसीसे मैं इस पर कुछ भी लिखना नहीं चाहता। हाँ. यह अष्टशनीके 'देवागमेत्यादिमंगलपुरस्सरस्तव' वाक्यके
बात मेरी कुछ समझमें नहीं आई कि ऐसा करके मैंने किस अन्यथा अर्थको जो उसका एकमात्र अाधार कल्पित किया
बातका प्रोपेगेण्डा करना चाहा है? यदि शास्त्रीजी से है वह निराधार है-उसमें कुछ भी सार नहीं जान पड़ता।
विद्वत्ताका प्रोपेगेण्डा कहेंगे तो वे अपनेको इस प्रारोपसे * यथा-"अर्थशब्देन प्रत्यक्षस्याभिधानाद्वा, क्वचिद्विषयेण कैसे मुक्त कर सकेंगे, यह कुछ समझ नहीं पड़ता। क्यों कि विर्षायणो वचनाद्धर्मकीतिकारिकाया एव तन्मतदूषण- उन्होंने इतिहासविषयके भनेकलेस लिखे हैं, ग्रन्थोंकी परत्वेन व्याख्यातुं शक्यत्वात् । यथा च .......।" प्रस्तावना लिखी हैं और विद्वानोंको विचार के लिये प्रेरित