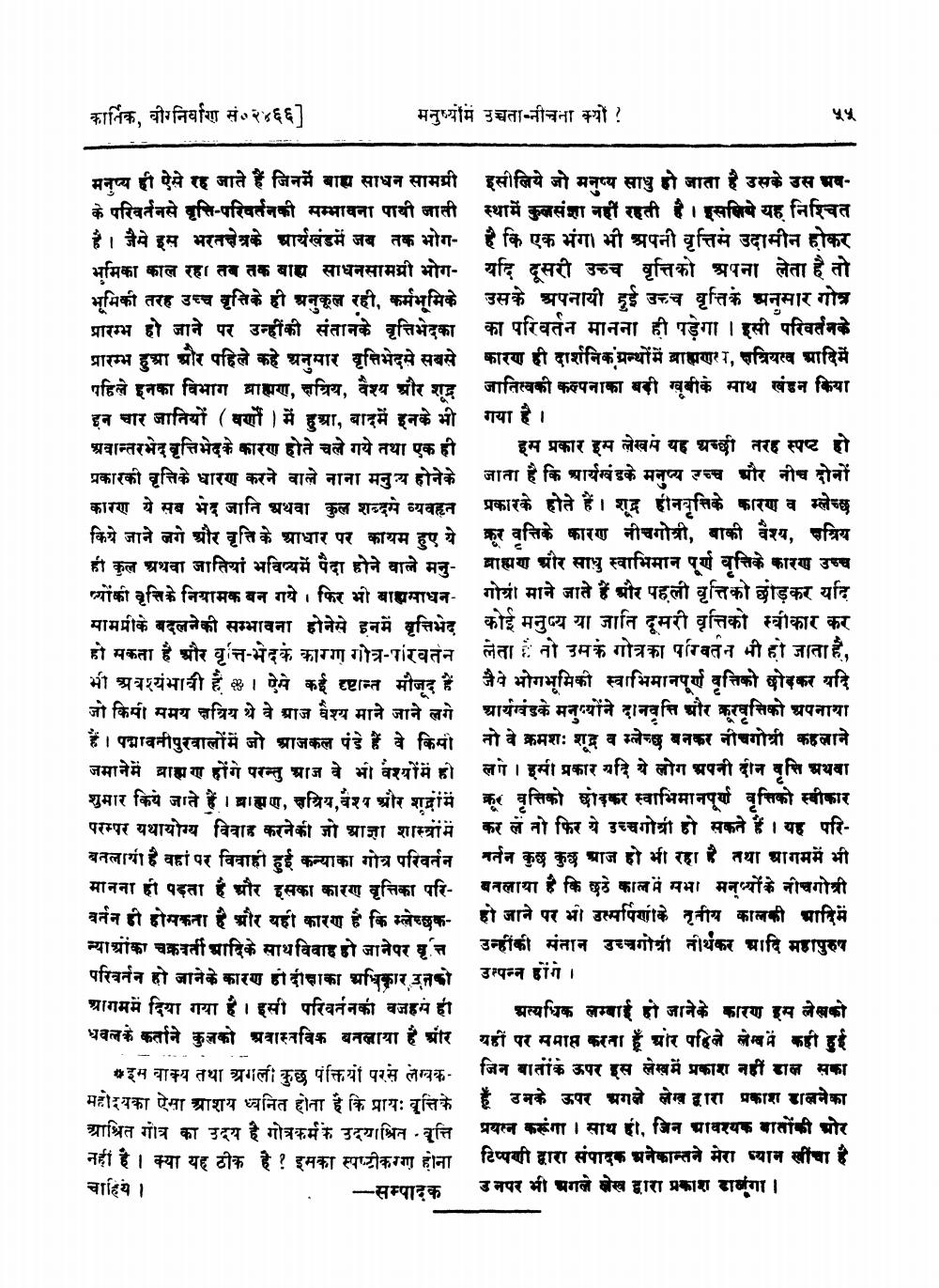________________
कार्तिक, वीरनिर्वाण सं०२४६६ ]
'
मनुष्य ही ऐसे रह जाते हैं जिनमें बाह्य साधन सामग्री के परिवर्तन से वृत्ति-परिवर्तनकी सम्भावना पायी जाती हैं। जैसे इस भरतक्षेत्र के चार्यखंडमें जब तक भोग भूमिका काल रहा तब तक बाह्य साधनसामग्री भोगभूमिकी तरह उच्च वृत्तिके ही अनुकूल रही, कर्मभूमिके प्रारम्भ हो जाने पर उन्हींकी संतानके वृत्तिभेदका प्रारम्भ हुआ और पहिले कहे अनुसार वृत्तिभेदसे सबसे पहिले इनका विभाग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार जातियों (वर्णों में हुआ, बादमें इनके भी श्रवान्तरभेद वृत्तिभेद के कारण होते चले गये तथा एक ही प्रकारकी वृत्तिके धारण करने वाले नाना मनुष्य होनेके कारण ये सब भेद जाति अथवा कुल शब्दमे व्यवहृत किये जाने लगे और वृत्ति के आधार पर कायम हुए ये ही कुल अथवा जातियां भविष्य में पैदा होने वाले मनुयोंकी वृसिके नियामक बन गये। फिर भी बाह्यमाधनमामी के बदलने की सम्भावना होनेसे इनमें वृत्तिभेद हो सकता है और वृत्ति-भेदकं कारण गोत्र-परिवर्तन भी अवश्यंभावी हैं । ऐसे कई दृष्टान्त मौजूद हैं जो किसी समय क्षत्रिय थे वे श्राज वैश्य माने जाने लगे हैं। पद्मावतीपुरवालों में जो श्राजकल पंडे हैं वे किसी जमाने में ब्राह्मण होंगे परन्तु आज वे भी वैश्यों में हो शुमार किये जाते हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंमें परस्पर यथायोग्य विवाह करनेकी जो आज्ञा शास्त्रों में बतलायी है वहां पर विवाही हुई कन्याका गोत्र परिवर्तन मानना ही पड़ता है और इसका कारण वृत्तिका परिवर्तन ही होसकता है और यही कारण है कि म्लेच्छकन्यायका चक्रवर्ती भादिके साथ विवाह हो जानेपर वृति परिवर्तन हो जाने के कारण ही दीक्षाका अधिकार, उनको श्रागम में दिया गया है। इसी परिवर्तनकी वजहसे ही धवल कर्ताने कुलको अवास्तविक बनलाया है और
मनुष्यों उच्चता-नीचता क्यों ?
*इस वाक्य तथा अगली कुछ पंक्तियों परसे लेखकमहोदयका ऐसा आशय ध्वनित होता है कि प्रायः वृत्तिके श्राश्रित गोत्र का उदय है गोत्रकर्मके उदद्याश्रित वृत्ति नहीं है। क्या यह ठीक है ? इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये ।
-सम्पादक
५५
इसीलिये जो मनुष्य साधु हो जाता है उसके उस अवस्थामें कुलसंज्ञा नहीं रहती है। इसलिये यह निश्चित है कि एक भंगा भी अपनी वृत्तिमं उदासीन होकर यदि दूसरी उच्च वृत्तिको अपना लेता है तो उसके अपनायी हुई उच्च वृत्तिकं अनुसार गोत्र का परिवर्तन मानना ही पड़ेगा । इसी परिवर्तनके कारण ही दार्शनिक ग्रन्थों में ब्राह्मण, क्षत्रियत्व आदिमें जातिवकी कल्पनाका बड़ी खूबी के साथ खंडन किया
गया 1
इस प्रकार इस लेख में यह धच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है कि श्रार्यखंडके मनुष्य उच्च और नीच दोनों प्रकारके होते हैं। शूद्र हीनवृत्तिके कारण व म्लेच्छ क्रूर वृत्तिके कारण नीचगोत्री, बाकी वैश्य, क्षत्रिय ब्राह्मण और साधु स्वाभिमान पूर्ण वृत्तिके कारण उच्च गोत्री माने जाते हैं और पहली वृत्तिको छोड़कर यदि कोई मनुष्य या जाति दूसरी वृत्तिको स्वीकार कर लेता है तो उसके गोत्रका परिवर्तन भी हो जाता है, जैसे भोग भूमिकी स्वाभिमानपूर्ण वृत्तिको छोड़कर यदि श्रार्यखंडके मनुष्योंने दानवृत्ति और क्रूरवृत्तिको अपनाया तो वे क्रमशः शुद्र व म्लेच्छ बनकर नीचगोत्री कहलाने लगे । इसी प्रकार यदि ये लोग अपनी दीन वृत्ति अथवा क्रूर वृत्तिको छोड़कर स्वाभिमानपूर्ण वृत्तिको स्वीकार कर ले तो फिर ये उच्चगोत्री हो सकते हैं। यह परिनर्तन कुछ कुछ श्राज हो भी रहा है तथा श्रागममें भी बतलाया है कि छठे काल में सभा मनुष्यों के नीचगोत्री हो जाने पर भी उस्मर्पिण के तृतीय कालकी धादि उन्हींकी संतान उच्चगोत्री तीर्थंकर आदि महापुरुष उत्पन्न होंगे।
अत्यधिक लम्बाई हो जानेके कारण इस लेखको यहीं पर समाप्त करता हूँ चार पहिले लेख में कही हुई जिन बातोंके ऊपर इस लेख में प्रकाश नहीं डाल सका हैं उनके ऊपर अगले लेख द्वारा प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा । साथ ही, जिन आवश्यक बातोंकी ओर टिप्पणी द्वारा संपादक अनेकान्तने मेरा ध्यान खींचा है उनपर भी अगले लेख द्वारा प्रकाश डालूंगा ।