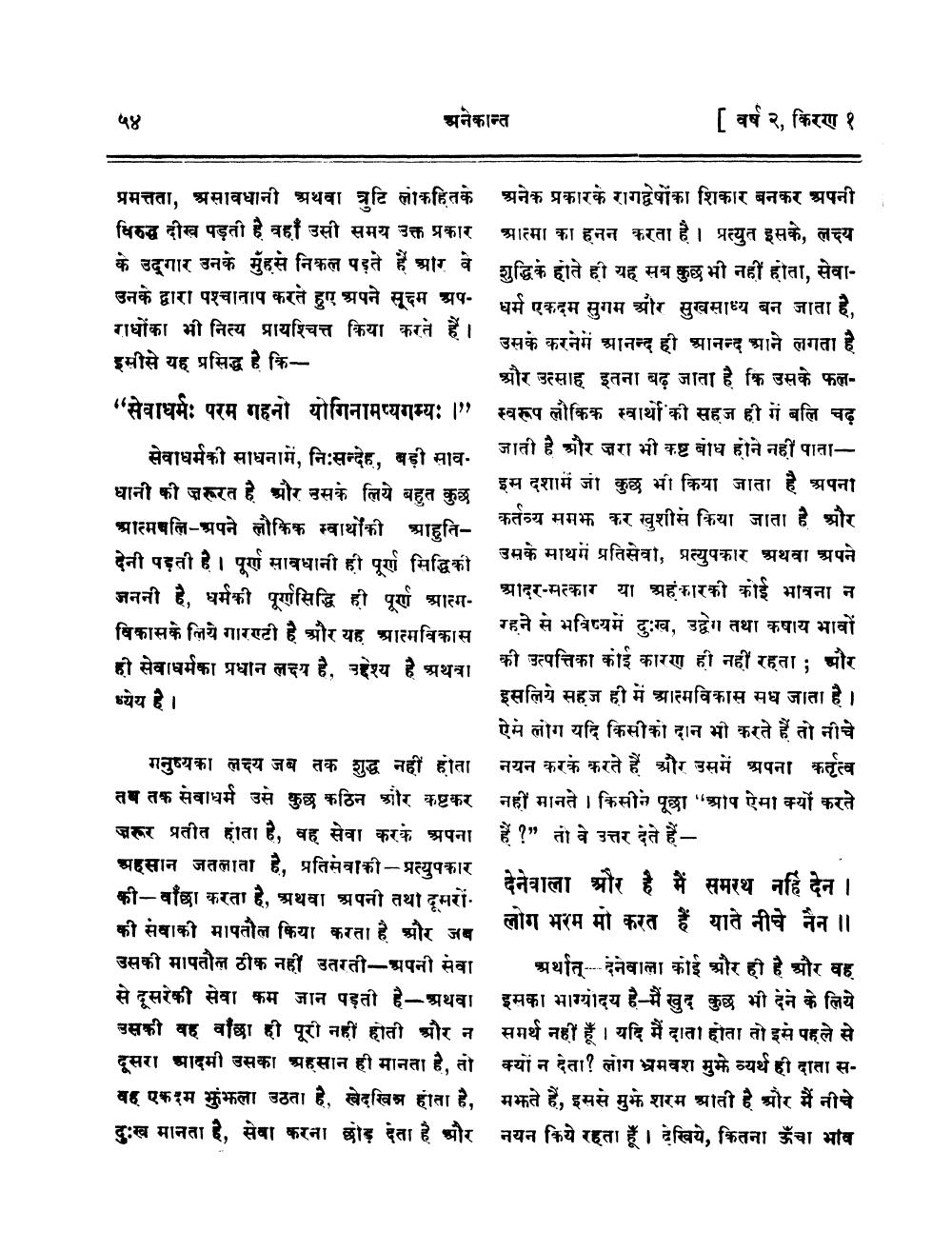________________
अनेकान्त
[ वर्ष २, किरण १
प्रमत्तता, असावधानी अथवा त्रुटि लोकहितके अनेक प्रकारके रागद्वेषोंका शिकार बनकर अपनी विरुद्ध दीख पड़ती है वहाँ उसी समय उक्त प्रकार आत्मा का हनन करता है। प्रत्युत इसके, लक्ष्य के उद्गार उनके मुंहसे निकल पड़ते हैं और वे शुद्धिकं होते ही यह सब कुछ भी नहीं होता, सेवाउनके द्वारा पश्चाताप करते हुए अपने सूक्ष्म अप- धर्म एकदम सगम और सुखसाध्य बन जाता है, गधोंका भी नित्य प्रायश्चित्त किया करते हैं।
उसके करनेमें आनन्द ही आनन्द आने लगता है इसीसे यह प्रसिद्ध है कि
और उत्साह इतना बढ़ जाता है कि उसके फल"सेवाधर्मः परम गहनो योगिनामप्यगम्यः ।" स्वरूप लौकिक स्वार्थो की सहज ही में बलि चढ़
सेवाधर्मकी साधनामें, निःसन्देह. बडी साव. जाती है और जरा भी कष्ट बोध होने नहीं पाताधानी की जरूरत है और उसके लिये बहुत कुछ
इम दशामें जो कुछ भी किया जाता है अपना आत्मबलि-अपने लौकिक स्वार्थोकी प्राइति- कर्तव्य ममझ कर खुशीस किया जाता है और देनी पड़ती है। पूर्ण सावधानी ही पूर्ण मिद्धिकी उसके माथमं प्रतिसेवा, प्रत्युपकार अथवा अपने जननी है, धर्मकी पूर्णसिद्धि ही पर्ण आत्म- श्रादर-मत्कार या अहंकारकी कोई भावना न विकासके लिये गारण्टी है और यह प्रामाविका रहने से भविष्यम दुःख, उद्वेग तथा कषाय भावों हो सेवाधर्मका प्रधान लक्ष्य है, उद्देश्य है अथवा की उत्पत्तिका काइ कारण हा नहा रहता; भार ध्येय है।
इसलिये सहज ही में आत्मविकास सध जाता है।
ऐसे लोग यदि किसीको दान भी करते हैं तो नीचे मनुष्यका लक्ष्य जब तक शुद्ध नहीं होता नयन करके करते हैं और उसमें अपना कर्तृत्व तब तक सेवाधर्म उसे कुछ कठिन और कष्टकर नहीं मानते । किसीने पूछा "श्राप ऐमा क्यों करते जरूर प्रतीत होता है, वह सेवा करकं अपना हैं ?" तो वे उत्तर देते हैंअहसान जतलाता है, प्रतिसंवाकी-प्रत्युपकार की-वांछा करता है, अथवा अपनी तथा दूसरों
देनेवाला और है मैं समरथ नहिं देन । की संवाकी मापतौल किया करता है और जब लोग भरम मी करत हैं याते नीचे नैन ॥ उसकी मापतौल ठीक नहीं उतरती-अपनी संवा अर्थात्---दनेवाला कोई और ही है और वह से दूसरेकी सेवा कम जान पड़ती है-अथवा इसका भाग्योदय है-मैं खुद कुछ भी देने के लिये उसकी वह वांछा ही पूरी नहीं होती और न समर्थ नहीं हूँ । यदि मैं दाता होता तो इसे पहले से दूसरा आदमी उसका अहसान ही मानता है, तो क्यों न देता? लोग भ्रमवश मुझे व्यर्थ ही दाता सवह एकदम सुंझला उठता है, खेदखिन्न होता है, मझते हैं, इससे मुझे शरम आती है और मैं नीचे दुःख मानता है, सेवा करना छोड़ देता है और नयन किये रहता हूँ। देखिये, कितना ऊँचा भाव