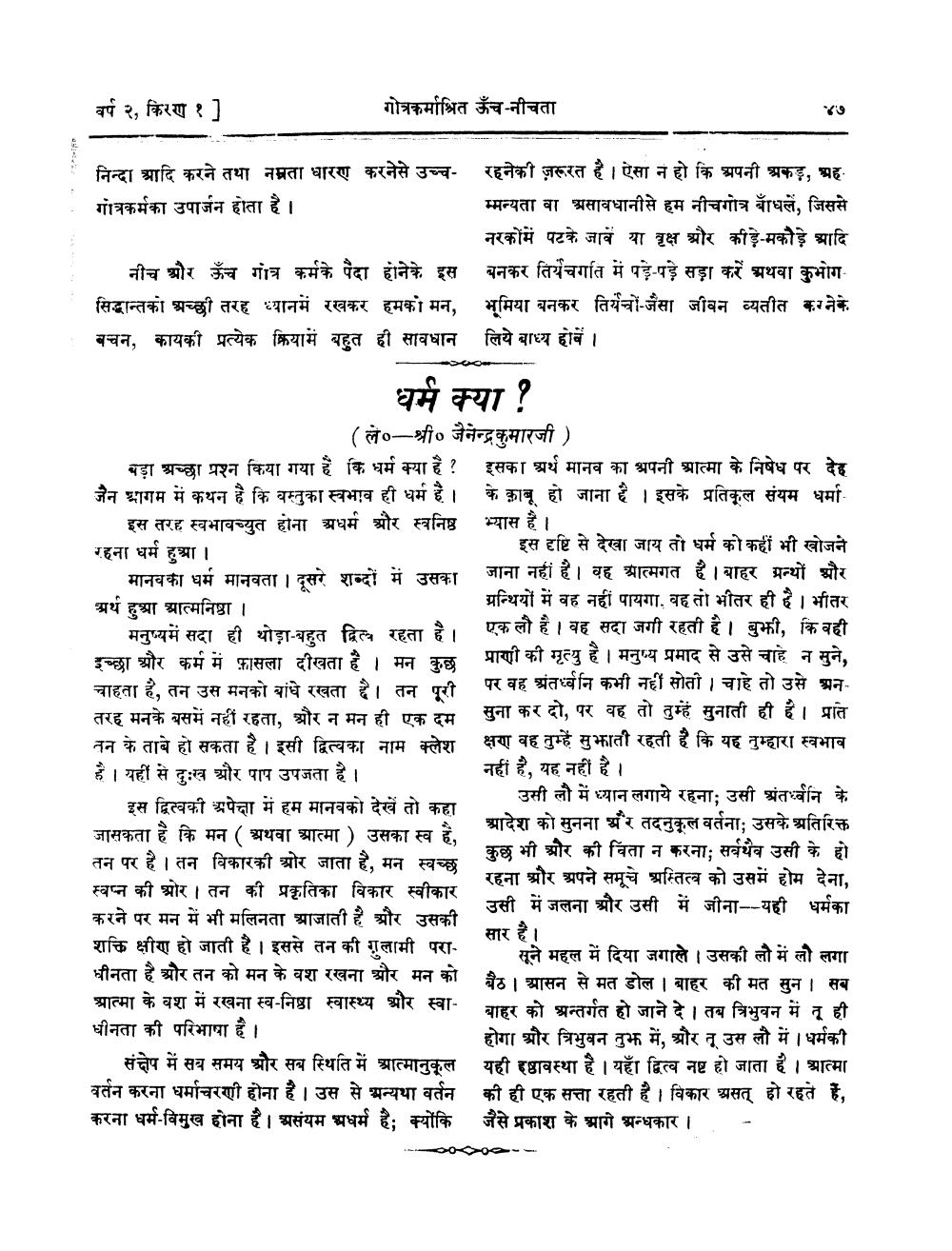________________
वर्ष २, किरण १]
गोत्रकर्माश्रित ऊँच-नीचता
४७
निन्दा आदि करने तथा नम्रता धारण करनेसे उच्च- रहनेकी ज़रूरत है । ऐसा न हो कि अपनी अकड़, अहगोत्रकर्मका उपार्जन होता है।
म्मन्यता वा असावधानीसे हम नीचगोत्र बाँधले, जिससे
नरकोंमें पटके जावे या वृक्ष और कीड़े-मकौड़े आदि नीच और ऊँच गोत्र कर्मके पैदा होनेके इस बनकर तिर्यचति में पड़े-पड़े सड़ा करें अथवा कुभोग सिद्धान्तको अच्छी तरह ध्यानमें रखकर हमको मन, भूमिया बनकर तिर्यचों-जैसा जीवन व्यतीत करनेके वचन, कायकी प्रत्येक क्रियामें बहुत ही सावधान लिये बाध्य होवें ।
धर्म क्या ?
(ले०-श्री जैनेन्द्रकुमारजी ) बड़ा अच्छा प्रश्न किया गया है कि धर्म क्या है ? इसका अर्थ मानव का अपनी आत्मा के निषेध पर देह जैन श्रागम में कथन है कि वस्तुका स्वभाव ही धर्म है। के काबू हो जाना है । इसके प्रतिकूल संयम धर्मा
इस तरह स्वभावच्युत होना अधर्म और स्वनिष्ठ भ्यास है। रहना धर्म हुआ।
__इस दृष्टि से देखा जाय तो धर्म को कहीं भी खोजने मानवका धर्म मानवता । दसरे शब्दों में उसका जाना नहीं है। वह आत्मगत है। बाहर ग्रन्थों और अर्थ हुआ आत्मनिष्ठा ।
ग्रन्थियों में वह नहीं पायगा, वह तो भीतर ही है। भीतर मनुष्यमें सदा ही थोड़ा-बहुत द्वित्व रहता है। एक लौ है । वह सदा जगी रहती है। बुझी, कि वही इच्छा और कर्म में फासला दीखता है। मन कल प्राणी की मृत्यु है । मनुष्य प्रमाद से उसे चाहे न सने. चाहता है, तन उस मनको बांधे रखता है। तन पूरी पर वह अतध्वान कभा नहा सा
पर वह अंतर्ध्वनि कभी नहीं सोती । चाहे तो उसे अनतरह मनके बसमें नहीं रहता, और न मन ही एक दम सुना कर दो, पर वह तो तुम्हें मुनाती ही है। प्रात नन के ताबे हो सकता है। इसी द्वित्वका नाम क्लेश क्षण वह तुम्हें सुझाती रहती है कि यह तुम्हारा स्वभाव है। यहीं से दुःख और पाप उपजता है।
नहीं है, यह नहीं है।
उसी लौ में ध्यान लगाये रहना: उसी अंतर्ध्वनि के इस द्वित्वकी अपेक्षा में हम मानवको देखें तो कहा जासकता है कि मन (अथवा आत्मा ) उसका स्व है,
आदेश को सुनना और तदनुकूल वर्तना; उसके अतिरिक्त
कुछ भी और की चिंता न करना; सर्वथैव उसी के हो तन पर है । तन विकारकी ओर जाता है, मन स्वच्छ
रहना और अपने समूचे अस्तित्व को उसमें होम देना, स्वप्न की ओर । तन की प्रकृतिका विकार स्वीकार
उसी में जलना और उसी में जीना--यही धर्मका करने पर मन में भी मलिनता आजाती है और उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है । इससे तन की गुलामी परा
सूने महल में दिया जगाले । उसकी लौ में लौ लगा धीनता है और तन को मन के वश रखना और मन को
बैठ। आसन से मत डोल । बाहर की मत सुन । सब आत्मा के वश में रखना स्व-निष्ठा स्वास्थ्य और स्वा- बाहर को अन्तर्गत हो जाने दे। तब त्रिभुवन में तू ही धीनता की परिभाषा है।
होगा और त्रिभुवन तुझ में, और तू उस लौ में । धर्मकी संक्षेप में सब समय और सब स्थिति में आत्मानुकूल यही इष्ठावस्था है । यहाँ द्वित्व नष्ट हो जाता है । आत्मा वर्तन करना धर्माचरणी होना है। उस से अन्यथा वर्तन की ही एक सत्ता रहती है। विकार असत् हो रहते हैं, करना धर्म-विमुख होना है। असंयम अधर्म है; क्योंकि जैसे प्रकाश के आगे अन्धकार ।
सार है।