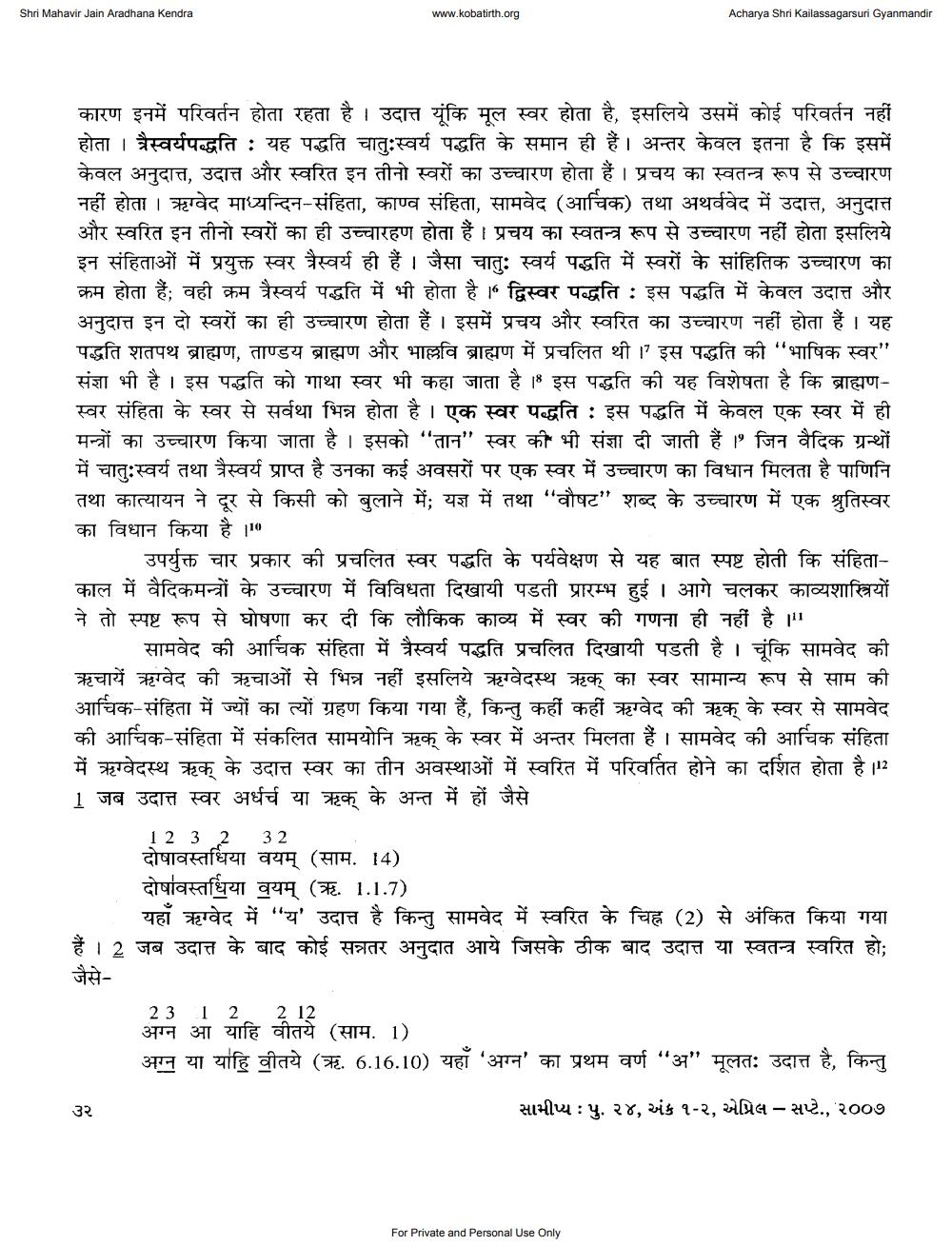________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
कारण इनमें परिवर्तन होता रहता है । उदात्त यूंकि मूल स्वर होता है, इसलिये उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता । स्वर्यपद्धति : यह पद्धति चातुः स्वर्य पद्धति के समान ही हैं । अन्तर केवल इतना है कि इसमें केवल अनुदात्त, उदात्त और स्वरित इन तीनो स्वरों का उच्चारण होता हैं । प्रचय का स्वतन्त्र रूप से उच्चारण नहीं होता । ऋग्वेद माध्यन्दिन - संहिता, काण्व संहिता, सामवेद (आर्चिक) तथा अथर्ववेद में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इन तीनों स्वरों का ही उच्चारहण होता हैं । प्रचय का स्वतन्त्र रूप से उच्चारण नहीं होता इसलिये इन संहिताओं में प्रयुक्त स्वर त्रैस्वर्य ही हैं । जैसा चातुः स्वर्य पद्धति में स्वरों के सांहितिक उच्चारण का क्रम होता हैं; वही क्रम त्रैस्वर्य पद्धति में भी होता है ।" द्विस्वर पद्धति : इस पद्धति में केवल उदात्त और अनुदात्त इन दो स्वरों का ही उच्चारण होता हैं । इसमें प्रचय और स्वरित का उच्चारण नहीं होता हैं । यह पद्धति शतपथ ब्राह्मण, ताण्डय ब्राह्मण और भाल्लवि ब्राह्मण में प्रचलित थी । इस पद्धति की " भाषिक स्वर" संज्ञा भी है । इस पद्धति को गाथा स्वर भी कहा जाता है । इस पद्धति की यह विशेषता है कि ब्राह्मणस्वर संहिता के स्वर से सर्वथा भिन्न होता है । एक स्वर पद्धति : इस पद्धति में केवल एक स्वर में ही मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है । इसको "तान" स्वर की भी संज्ञा दी जाती हैं । जिन वैदिक ग्रन्थों में चातु:स्वर्य तथा त्रैस्वर्य प्राप्त है उनका कई अवसरों पर एक स्वर में उच्चारण का विधान मिलता है पाणिनि तथा कात्यायन ने दूर से किसी को बुलाने में; यज्ञ में तथा "वौषट" शब्द के उच्चारण में एक श्रुतिस्वर का विधान किया है ।"
उपर्युक्त चार प्रकार की प्रचलित स्वर पद्धति के पर्यवेक्षण से यह बात स्पष्ट होती कि संहिता - काल में वैदिकमन्त्रों के उच्चारण में विविधता दिखायी पडती प्रारम्भ हुई । आगे चलकर काव्यशास्त्रियों ने तो स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि लौकिक काव्य में स्वर की गणना ही नहीं है ।"
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
सामवेद की आर्चिक संहिता में त्रैस्वर्य पद्धति प्रचलित दिखायी पडती है । चूंकि सामवेद की ऋचायें ऋग्वेद की ऋचाओं से भिन्न नहीं इसलिये ऋग्वेदस्थ ऋक् का स्वर सामान्य रूप से साम की आर्चिक-संहिता में ज्यों का त्यों ग्रहण किया गया हैं, किन्तु कहीं कहीं ऋग्वेद की ऋक् के स्वर से सामवेद की आर्चिक - संहिता में संकलित सामयोनि ऋक् के स्वर में अन्तर मिलता हैं । सामवेद की आर्चिक संहिता में ऋग्वेदस्थ ऋक् के उदात्त स्वर का तीन अवस्थाओं में स्वरित में परिवर्तित होने का दर्शित होता है | 12 1 जब उदात्त स्वर अर्धर्च या ऋक् के अन्त में हों जैसे
1 2 3 2 32
दोषावस्तर्धिया वयम् (साम. 14 )
૩૨
दोषा॑वस्ता॑धि॒या व॒यम् (ऋ. 1.1.7)
यहाँ ऋग्वेद में "य' उदात्त है किन्तु सामवेद में स्वरित के चिह्न (2) से अंकित किया गया हैं । 2 जब उदात्त के बाद कोई सन्नतर अनुदात आये जिसके ठीक बाद उदात्त या स्वतन्त्र स्वरित हो; जैसे
23 1 2 2 12
अग्न आ याहि वीतये (साम. 1)
अग्न॒ या या॑हि॒ वी॒तये (ऋ. 6.16.10 ) यहाँ 'अग्न' का प्रथम वर्ण "अ" मूलतः उदात्त है, किन्तु
सामीप्य : पु. २४, अंड १ -२, खेप्रिस - सप्टे. २००७
For Private and Personal Use Only