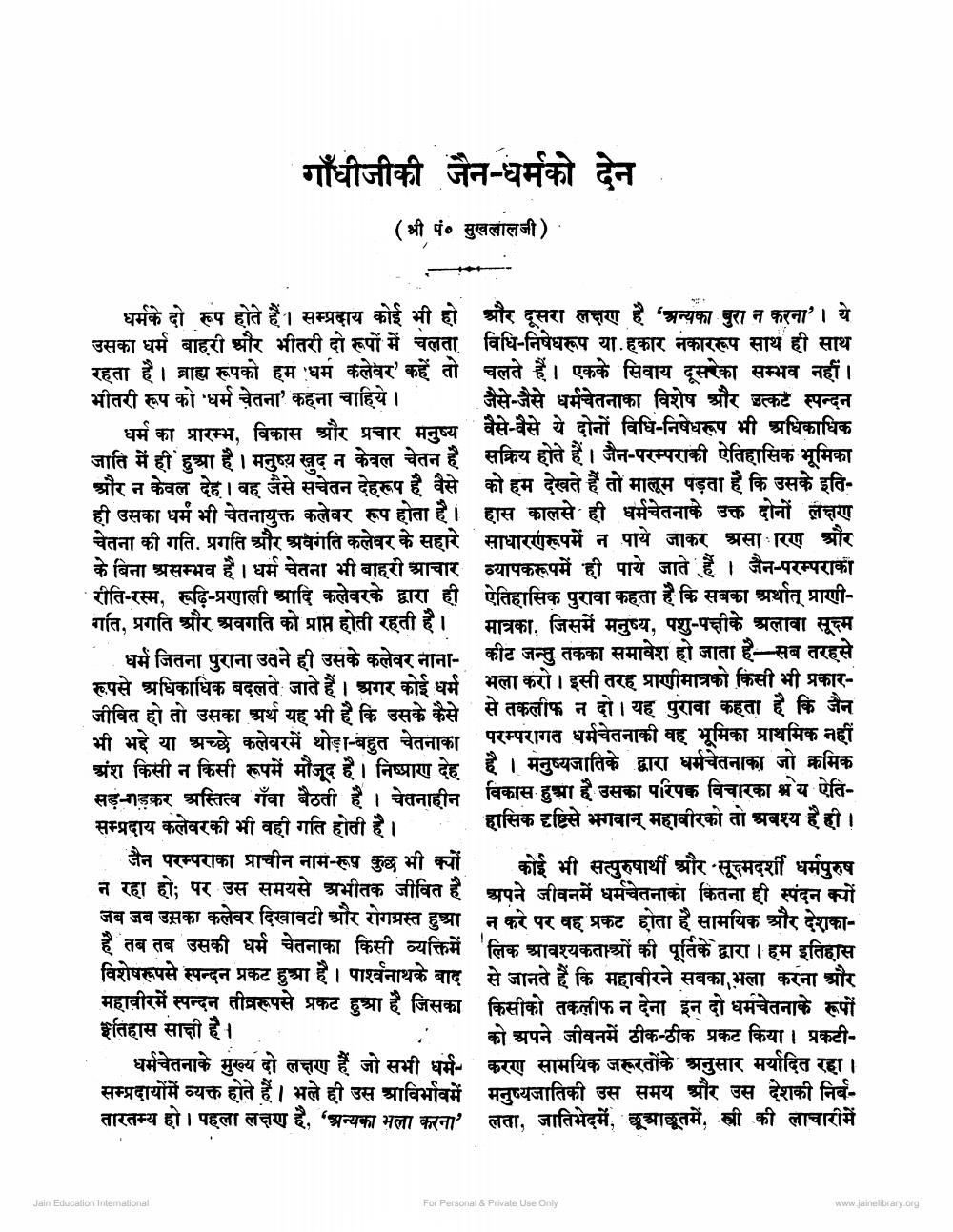________________
गाँधीजीकी जैन-धर्मको देन
(श्री पं० सुखलालजी)
धर्मके दो रूप होते हैं । सम्प्रदाय कोई भी हो उसका धर्म बाहरी और भीतरी दो रूपों में चलता रहता है। ब्राह्म रूपको हम धर्म कलेवर' कहें तो भीतरी रूप को 'धर्म चेतना' कहना चाहिये ।
धर्म का प्रारम्भ, विकास और प्रचार मनुष्य जाति में ही हुआ है। मनुष्य खुद न केवल चेतन है और न केवल देह । वह जैसे सचेतन देहरूप है वैसे ही उसका धर्मं भी चेतनायुक्त कलेवर रूप होता है । चेतना की गति प्रगति और अवगति कलेवर के सहारे के बिना सम्भव है । धर्म चेतना भी बाहरी आचार रीति- रस्म, रूढ़ि - प्रणाली आदि कलेवरके द्वारा ही गति, प्रगति और अवगति को प्राप्त होती रहती है ।
धर्म जितना पुराना उतने ही उसके कलेवर नाना-. रूपसे अधिकाधिक बदलते जाते हैं। अगर कोई धर्म जीवित हो तो उसका अर्थ यह भी है कि उसके कैसे भी भद्दे या अच्छे कलेवरमें थोड़ा-बहुत चेतनाका अंश किसी न किसी रूपमें मौजूद है। निष्प्राण देह सड़-गड़कर अस्तित्व गँवा बैठती है । चेतनाहीन सम्प्रदाय कलेवर की भी वही गति होती है ।
जैन परम्पराका प्राचीन नाम रूप कुछ भी क्यों न रहा हो; पर उस समयसे अभीतक जीवित है जब जब उसका कलेवर दिखावटी और रोगग्रस्त हुआ है तब तब उसकी धर्म चेतनाका किसी व्यक्तिमें विशेषरूपसे स्पन्दन प्रकट हुआ है। पार्श्वनाथके बाद महावीरमें स्पन्दन तीव्ररूपसे प्रकट हुआ है जिसका इतिहास साक्षी है ।
धर्मचेतनाके मुख्य दो लक्षण हैं जो सभी धर्मसम्प्रदायोंमें व्यक्त होते हैं। भले ही उस आविर्भावमें तारतम्य हो । पहला लक्षण है, 'अन्यका भला करना'
Jain Education International
और दूसरा लक्षण है 'अन्यका बुरा न करना' । ये विधि - निषेधरूप या हकार नकाररूप साथ ही साथ चलते हैं । एकके सिवाय दूसरेका सम्भव नहीं । जैसे-जैसे धर्मचेतनाका विशेष और उत्कट स्पन्दन वैसे-वैसे ये दोनों विधि-निषेधरूप भी अधिकाधिक सक्रिय होते हैं । जैन- परम्पराकी ऐतिहासिक भूमिका को हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि उसके इतिहास कालसे ही धर्मचेतनाके उक्त दोनों लक्षण साधारणरूपमें न पाये जाकर असाधरण और व्यापकरूपमें ही पाये जाते हैं । जैन - परम्पराका ऐतिहासिक पुरावा कहता है कि सबका अर्थात् प्राणीमात्रका, जिसमें मनुष्य, पशु-पक्षी के अलावा सूक्ष्म कीट जन्तु तकका समावेश हो जाता है - सब तरहसे भला करो। इसी तरह प्राणीमात्रको किसी भी प्रकारसे
तकलीफ न दो । यह पुरावा कहता है कि जैन परम्परागत धर्मचेतनाकी वह भूमिका प्राथमिक नहीं है । मनुष्यजातिके द्वारा धर्मचेतनाका जो क्रमिक विकास हुआ है उसका परिपक्क विचारका श्नय ऐतिहासिक दृष्टिसे भगवान् महावीरको तो अवश्य है ही ।
कोई भी सत्पुरुषार्थी और सूक्ष्मदर्शी धर्मपुरुष अपने जीवनमें धर्मचेतनाका कितना ही स्पंदन क्यों न करे पर वह प्रकट होता है सामयिक और देशका - लिक आवश्यकताओं की पूर्तिके द्वारा। हम इतिहास
'जानते हैं कि महावीरने सबका भला करना और किसीको तकलीफ न देना इन दो धर्मचेतनाके रूपों को अपने जीवनमें ठीक-ठीक प्रकट किया। प्रकटीकरण सामयिक जरूरतोंके अनुसार मर्यादित रहा । मनुष्यजातिकी उस समय और उस देशकी निर्बलता, जातिभेदमें, छूआछूतमें, स्त्री की लाचारीमें
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org