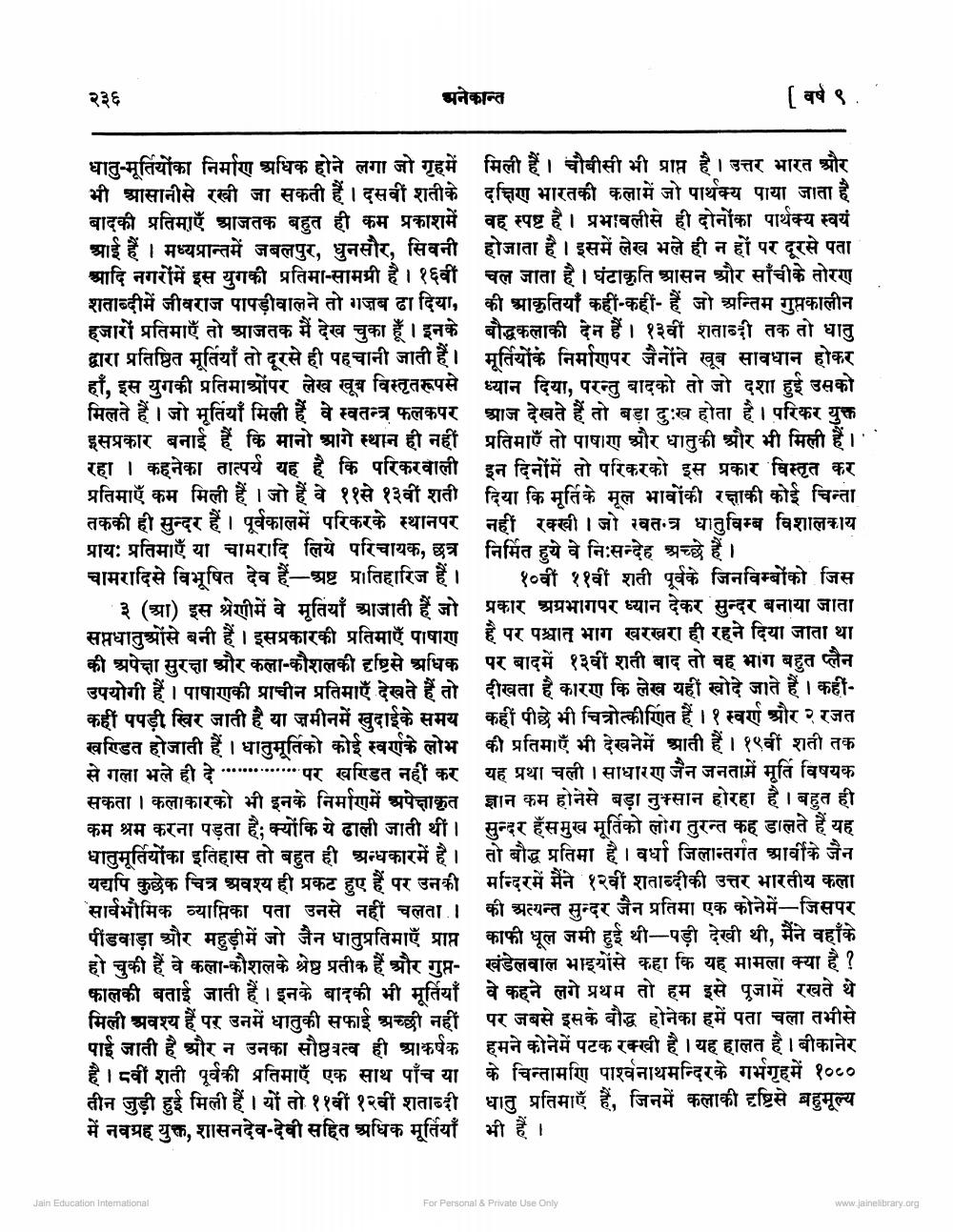________________
२३६
भनेकान्त
[ वर्ष ९.
धातु-मूर्तियोंका निर्माण अधिक होने लगा जो गृहमें मिली हैं। चौबीसी भी प्राप्त है। उत्तर भारत और भी आसानीसे रखी जा सकती हैं । दसवीं शतीके दक्षिण भारतकी कलामें जो पार्थक्य पाया जाता है बादकी प्रतिमाएँ आजतक बहुत ही कम प्रकाशमें वह स्पष्ट है। प्रभावलीसे ही दोनोंका पार्थक्य स्वयं आई हैं । मध्यप्रान्तमें जबलपुर, धुनसौर, सिवनी होजाता है । इसमें लेख भले ही न हों पर दूरसे पता आदि नगरोंमें इस युगकी प्रतिमा-सामग्री है । १६वीं चल जाता है । घंटाकृति आसन और साँचीके तोरण शताब्दीमें जीवराज पापड़ीवालने तो गज़ब ढा दिया, की आकृतियाँ कहीं-कहीं- हैं जो अन्तिम गुप्तकालीन हजारों प्रतिमाएँ तो आजतक मैं देख चुका हूँ । इनके बौद्धकलाकी देन हैं। १३वीं शताब्दी तक तो धातु द्वारा प्रतिष्ठित मतियाँ तो दरसे ही पहचानी जाती हैं। मर्तियोंक निर्माणपर जैनोंने खूब सावधान होकर हाँ, इस युगकी प्रतिमाओंपर लेख खूब विस्तृतरूपसे ध्यान दिया, परन्तु बादको तो जो दशा हुई उसको मिलते हैं । जो मूर्तियाँ मिली हैं वे स्वतन्त्र फलकपर आज देखते हैं तो बड़ा दुःख होता है। परिकर युक्त इसप्रकार बनाई हैं कि मानो आगे स्थान ही नहीं प्रतिमाएँ तो पाषाण और धातुकी और भी मिली हैं। रहा । कहनेका तात्पर्य यह है कि परिकरवाली इन दिनोंमें तो परिकरको इस प्रकार विस्तृत कर प्रतिमाएँ कम मिली हैं । जो है वे ११से १३वीं शती दिया कि मूर्ति के मूल भावोंकी रक्षाकी कोई चिन्ता तककी ही सुन्दर हैं। पूर्वकालमें परिकरके स्थानपर नहीं रक्खी । जो स्वतन्त्र धातुविम्ब विशालकाय प्रायः प्रतिमाएँ या चामरादि लिये परिचायक, छत्र निर्मित हुये वे निःसन्देह अच्छे हैं। चामरादिसे विभूषित देव हैं-अष्ट प्रातिहारिज हैं। १०वी ११वीं शती पूर्वके जिनविम्बोंको जिस
३ (आ) इस श्रेणीमें वे मृतियाँ आजाती हैं जो प्रकार अग्रभागपर ध्यान देकर सुन्दर बनाया जाता सप्तधातुओंसे बनी हैं । इसप्रकारकी प्रतिमाएँ पाषाण है पर पश्चात भाग खरखरा ही रहने दिया जाता था की अपेक्षा सरक्षा और कला-कौशलकी दृष्टिसे अधिक पर बादमें १३वीं शती बाद तो वह भाग बहत प्लैन उपयोगी हैं । पाषाणकी प्राचीन प्रतिमाएँ देखते हैं तो दीखता है कारण कि लेख यहीं खोदे जाते हैं । कहींकहीं पपड़ी खिर जाती है या ज़मीनमें खुदाईके समय कहीं पीछे भी चित्रोत्कीर्णित हैं । १ स्वर्ण और २ रजत खण्डित होजाती हैं । धातुमूर्तिको कोई स्वर्णके लोभ की प्रतिमाएँ भी देखनेमें आती हैं । १९वीं शती तक से गला भले ही दे .............पर खण्डित नहीं कर यह प्रथा चली । साधारण जैन जनतामें मूर्ति विषयक सकता । कलाकारको भी इनके निर्माणमें अपेक्षाकृत ज्ञान कम होनेसे बड़ा नुक्सान होरहा है। बहुत ही कम श्रम करना पड़ता है; क्योंकि ये ढाली जाती थीं। सुन्दर हँसमुख मूर्तिको लोग तुरन्त कह डालते हैं यह धातुमूर्तियोंका इतिहास तो बहुत ही अन्धकारमें है। तो बौद्ध प्रतिमा है। वर्धा जिलान्तर्गत आर्वीके जैन यद्यपि कुछेक चित्र अवश्य ही प्रकट हुए हैं पर उनकी मन्दिरमें मैंने १२वीं शताब्दीकी उत्तर भारतीय कला सार्वभौमिक व्याप्तिका पता उनसे नहीं चलता। की अत्यन्त सुन्दर जैन प्रतिमा एक कोनेमें-जिसपर पीडवाड़ा और महुड़ीमें जो जैन धातुप्रतिमाएँ प्राप्त काफी धूल जमी हुई थी-पड़ी देखी थी, मैंने वहाँके हो चुकी हैं वे कला-कौशलके श्रेष्ठ प्रतीक हैं और गुप्त- खंडेलवाल भाइयोंसे कहा कि यह मामला क्या है ? कालकी बताई जाती हैं। इनके बादकी भी मूर्तियाँ वे कहने लगे प्रथम तो हम इसे पूजामें रखते थे मिली अवश्य हैं पर उनमें धातुकी सफाई अच्छी नहीं पर जबसे इसके बौद्ध होनेका हमें पता चला तभीसे पाई जाती है और न उनका सौष्ठवत्व ही आकर्षक हमने कोने में पटक रक्खी है । यह हालत है । बीकानेर
शती पर्वकी प्रतिमाएँ एक साथ पाँच या के चिन्तामणि पार्श्वनाथमन्दिरके गर्भगृहमें १०८० तीन जुड़ी हुई मिली हैं । यों तो ११वी १२वीं शताब्दी धातु प्रतिमाएँ हैं, जिनमें कलाकी दृष्टिसे बहुमूल्य में नवग्रह युक्त, शासनदेव-देवी सहित अधिक मूर्तियाँ भी हैं ।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org