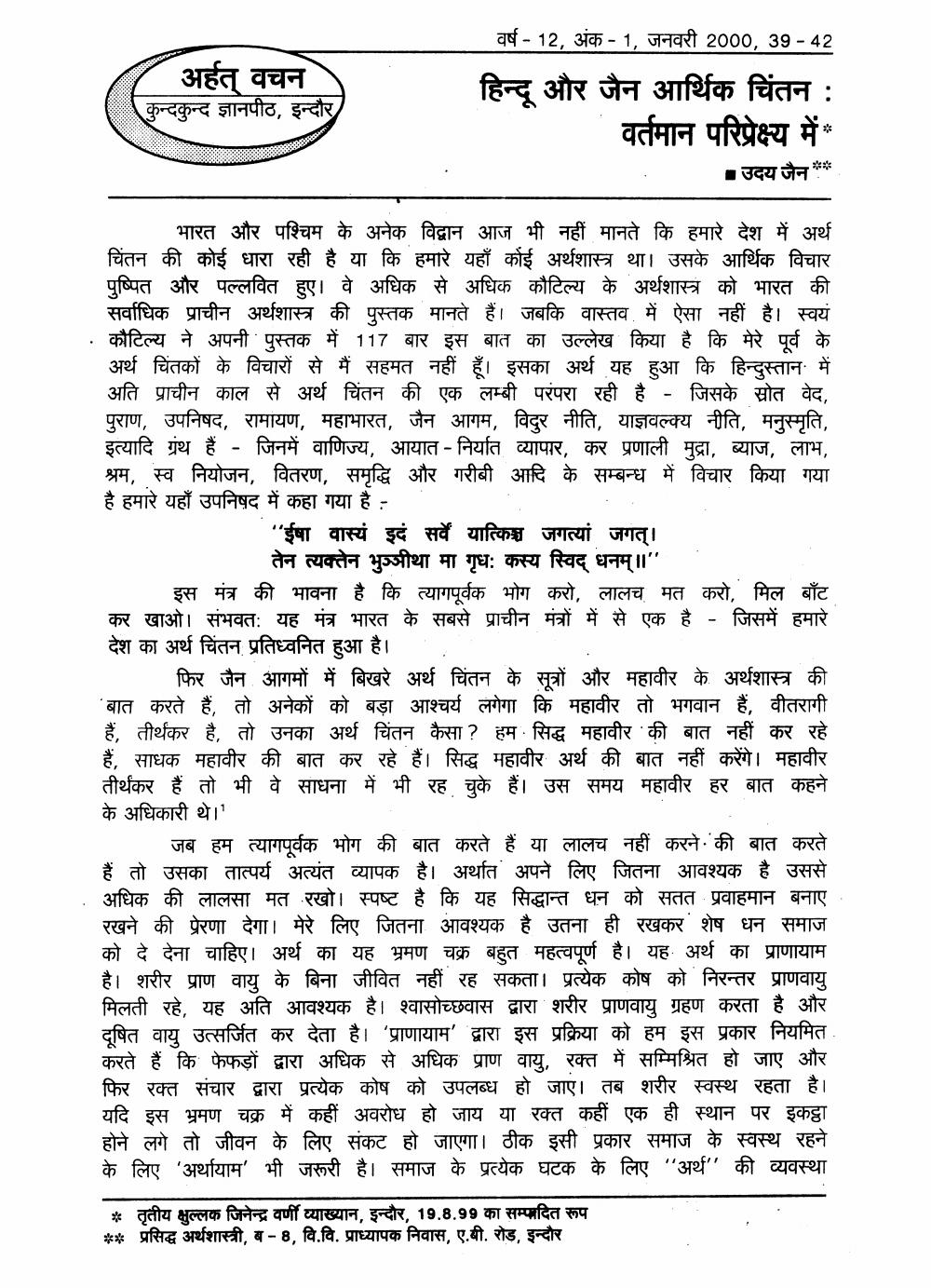________________
अर्हत् वच कुन्दकुन्द ज्ञानपीठ, इन्दौर
वर्ष 12, अंक 1 जनवरी 2000, 39-42
-
-
हिन्दू और जैन आर्थिक चिंतन : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में *
■ उदय जैन **
भारत और पश्चिम के अनेक विद्वान आज भी नहीं मानते कि हमारे देश में अर्थ चिंतन की कोई धारा रही है या कि हमारे यहाँ कोई अर्थशास्त्र था। उसके आर्थिक विचार पुष्पित और पल्लवित हुए। वे अधिक से अधिक कौटिल्य के अर्थशास्त्र को भारत की सर्वाधिक प्राचीन अर्थशास्त्र की पुस्तक मानते हैं। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। स्वयं कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में 117 बार इस बात का उल्लेख किया है कि मेरे पूर्व के अर्थ चिंतकों के विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ। इसका अर्थ यह हुआ कि हिन्दुस्तान में अति प्राचीन काल से अर्थ चिंतन की एक लम्बी परंपरा रही है। जिसके स्रोत वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, जैन आगम, विदुर नीति, याज्ञवल्क्य नीति, मनुस्मृति, इत्यादि ग्रंथ हैं जिनमें वाणिज्य, आयात निर्यात व्यापार, कर प्रणाली मुद्रा, ब्याज, लाभ, श्रम, स्व नियोजन, वितरण, समृद्धि और गरीबी आदि के सम्बन्ध में विचार किया गया है हमारे यहाँ उपनिषद में कहा गया है :
-
"ईषा वास्यं इदं सर्वे यात्किञ्च जगत्यां जगत् । तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद् धनम् ॥"
इस मंत्र की भावना है कि त्यागपूर्वक भोग करो, लालच मत करो, मिल बाँट कर खाओ। संभवत: यह मंत्र भारत के सबसे प्राचीन मंत्रों में से एक है जिसमें हमारे देश का अर्थ चिंतन प्रतिध्वनित हुआ है।
-
फिर जैन आगमों में बिखरे अर्थ चिंतन के सूत्रों और महावीर के अर्थशास्त्र की 'बात करते हैं, तो अनेकों को बड़ा आश्चर्य लगेगा कि महावीर तो भगवान हैं, वीतरागी हैं, तीर्थंकर है, तो उनका अर्थ चिंतन कैसा? हम सिद्ध महावीर की बात नहीं कर रहे हैं, साधक महावीर की बात कर रहे हैं। सिद्ध महावीर अर्थ की बात नहीं करेंगे। महावीर तीर्थंकर हैं तो भी वे साधना में भी रह चुके हैं। उस समय महावीर हर बात कहने के अधिकारी थे । '
जब हम त्यागपूर्वक भोग की बात करते हैं या लालच नहीं करने की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य अत्यंत व्यापक है। अर्थात अपने लिए जितना आवश्यक है उससे अधिक की लालसा मत रखो। स्पष्ट है कि यह सिद्धान्त धन को सतत प्रवाहमान बनाए रखने की प्रेरणा देगा। मेरे लिए जितना आवश्यक है उतना ही रखकर शेष धन समाज को दे देना चाहिए। अर्थ का यह भ्रमण चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। यह अर्थ का प्राणायाम है। शरीर प्राण वायु के बिना जीवित नहीं रह सकता। प्रत्येक कोष को निरन्तर प्राणवायु मिलती रहे, यह अति आवश्यक है। श्वासोच्छवास द्वारा शरीर प्राणवायु ग्रहण करता है और दूषित वायु उत्सर्जित कर देता है। 'प्राणायाम' द्वारा इस प्रक्रिया को हम इस प्रकार नियमित करते हैं कि फेफड़ों द्वारा अधिक से अधिक प्राण वायु रक्त में सम्मिश्रित हो जाए और फिर रक्त संचार द्वारा प्रत्येक कोष को उपलब्ध हो जाए। तब शरीर स्वस्थ रहता है। यदि इस भ्रमण चक्र में कहीं अवरोध हो जाय या रक्त कहीं एक ही स्थान पर इकट्ठा होने लगे तो जीवन के लिए संकट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार समाज के स्वस्थ रहने के लिए 'अर्थायाम' भी जरूरी है। समाज के प्रत्येक घटक के लिए "अर्थ" की व्यवस्था
* तृतीय क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी व्याख्यान, इन्दौर, 19.8.99 का सम्पादित रूप ** प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, ब- 8, वि. वि. प्राध्यापक निवास, ए.बी. रोड, इन्दौर