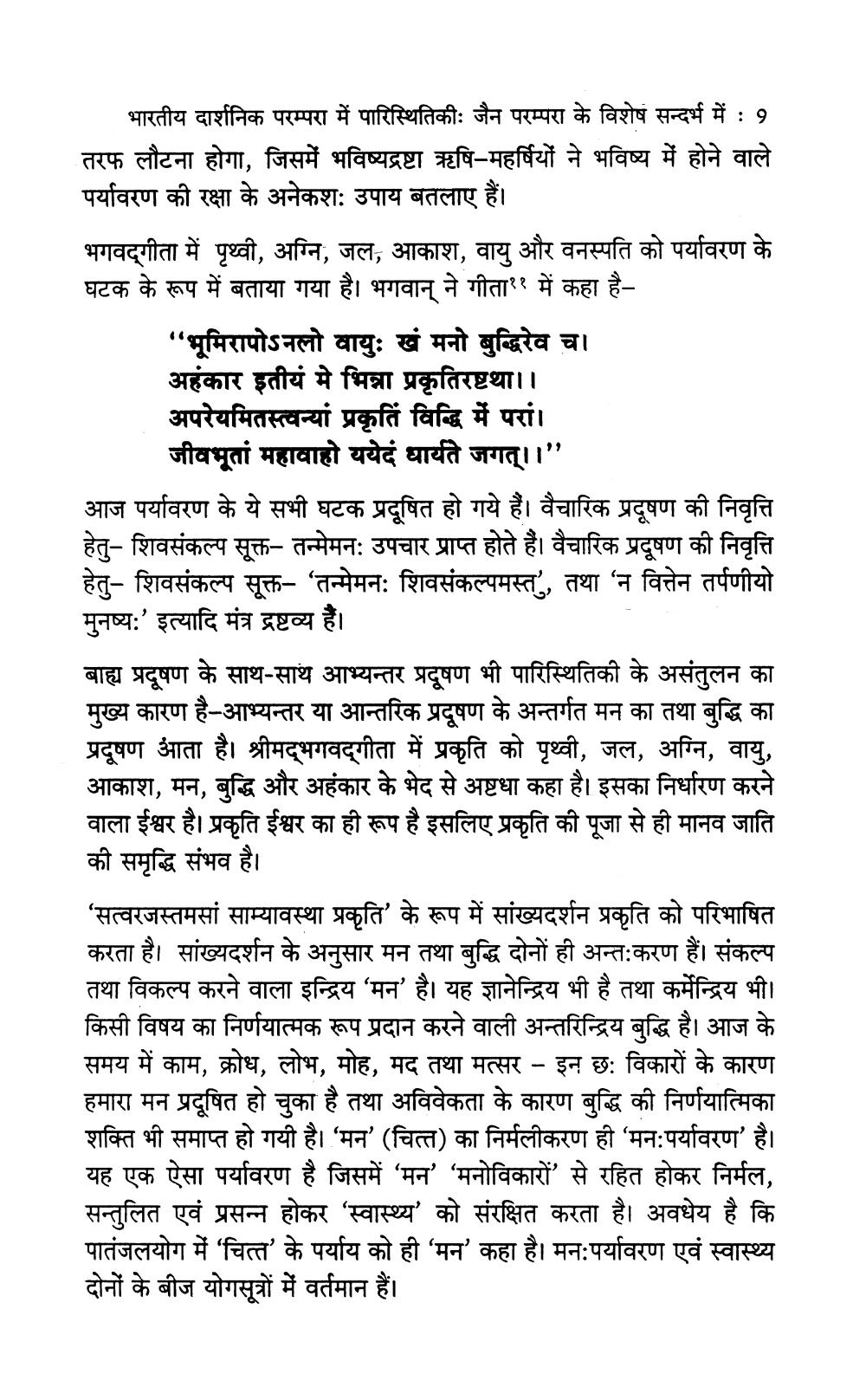________________
भारतीय दार्शनिक परम्परा में पारिस्थितिकीः जैन परम्परा के विशेष सन्दर्भ में : 9 तरफ लौटना होगा, जिसमें भविष्यद्रष्टा ऋषि-महर्षियों ने भविष्य में होने वाले पर्यावरण की रक्षा के अनेकशः उपाय बतलाए हैं। भगवद्गीता में पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु और वनस्पति को पर्यावरण के घटक के रूप में बताया गया है। भगवान् ने गीता११ में कहा है
"भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टथा।। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि में परां।
जीवभूतां महावाहो ययेदं धार्यते जगत्।।" आज पर्यावरण के ये सभी घटक प्रदूषित हो गये हैं। वैचारिक प्रदूषण की निवृत्ति हेतु- शिवसंकल्प सूक्त- तन्मेमन: उपचार प्राप्त होते है। वैचारिक प्रदूषण की निवृत्ति हेतु- शिवसंकल्प सूक्त- 'तन्मेमनः शिवसंकल्पमस्तु', तथा 'न वित्तेन तर्पणीयो मुनष्यः' इत्यादि मंत्र द्रष्टव्य है। बाह्य प्रदूषण के साथ-साथ आभ्यन्तर प्रदूषण भी पारिस्थितिकी के असंतुलन का मुख्य कारण है-आभ्यन्तर या आन्तरिक प्रदूषण के अन्तर्गत मन का तथा बुद्धि का प्रदूषण आता है। श्रीमद्भगवद्गीता में प्रकृति को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार के भेद से अष्टधा कहा है। इसका निर्धारण करने वाला ईश्वर है। प्रकृति ईश्वर का ही रूप है इसलिए प्रकृति की पूजा से ही मानव जाति की समृद्धि संभव है। 'सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति' के रूप में सांख्यदर्शन प्रकृति को परिभाषित करता है। सांख्यदर्शन के अनुसार मन तथा बुद्धि दोनों ही अन्त:करण हैं। संकल्प तथा विकल्प करने वाला इन्द्रिय 'मन' है। यह ज्ञानेन्द्रिय भी है तथा कर्मेन्द्रिय भी। किसी विषय का निर्णयात्मक रूप प्रदान करने वाली अन्तरिन्द्रिय बुद्धि है। आज के समय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मत्सर - इन छ: विकारों के कारण हमारा मन प्रदूषित हो चुका है तथा अविवेकता के कारण बुद्धि की निर्णयात्मिका शक्ति भी समाप्त हो गयी है। 'मन' (चित्त) का निर्मलीकरण ही ‘मन:पर्यावरण' है। यह एक ऐसा पर्यावरण है जिसमें 'मन' 'मनोविकारों' से रहित होकर निर्मल, सन्तुलित एवं प्रसन्न होकर 'स्वास्थ्य' को संरक्षित करता है। अवधेय है कि पातंजलयोग में 'चित्त' के पर्याय को ही 'मन' कहा है। मन:पर्यावरण एवं स्वास्थ्य दोनों के बीज योगसूत्रों में वर्तमान हैं।