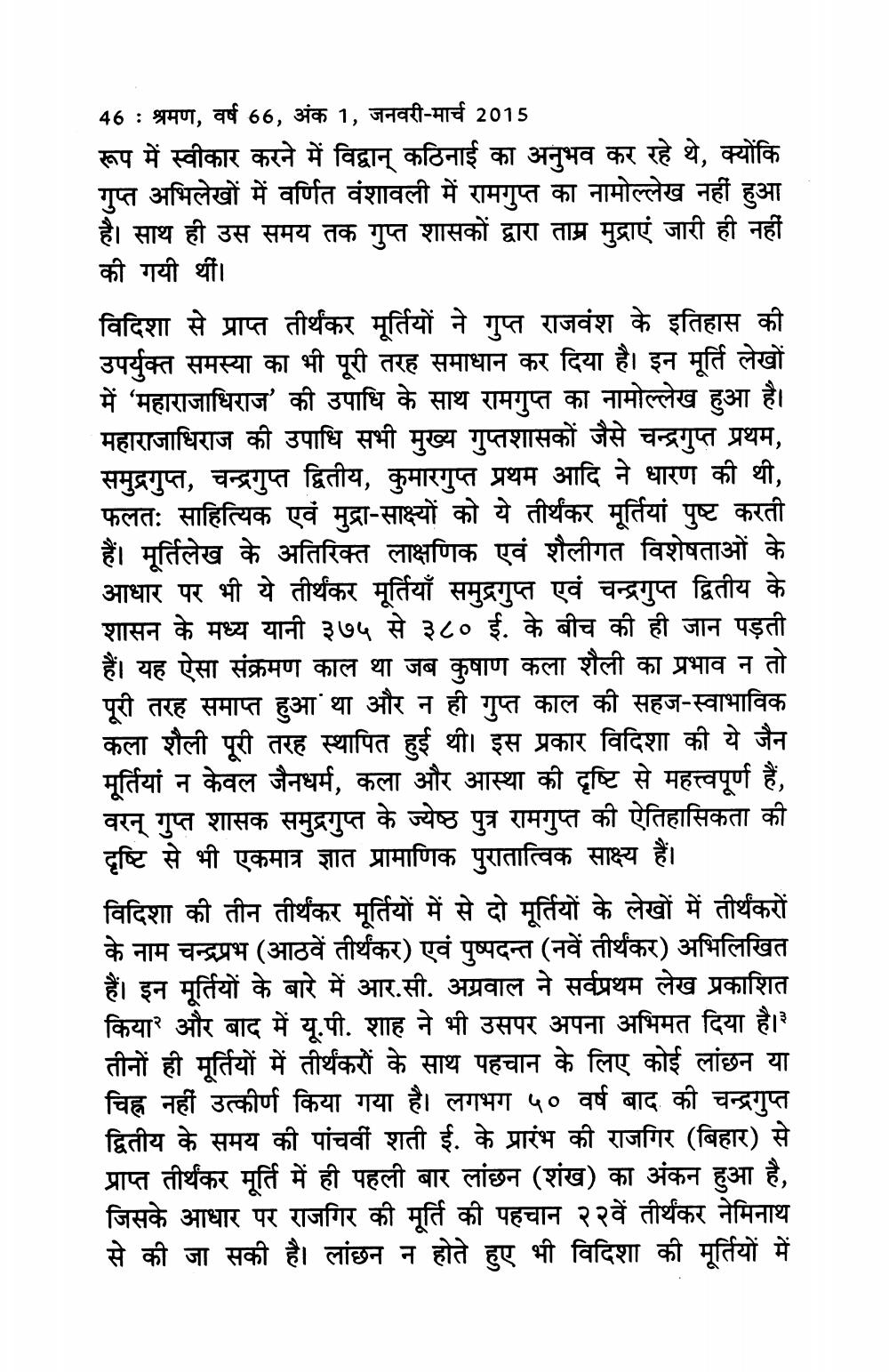________________
46 : श्रमण, वर्ष 66, अंक 1, जनवरी-मार्च 2015 रूप में स्वीकार करने में विद्वान् कठिनाई का अनुभव कर रहे थे, क्योंकि गुप्त अभिलेखों में वर्णित वंशावली में रामगुप्त का नामोल्लेख नहीं हुआ है। साथ ही उस समय तक गुप्त शासकों द्वारा ताम्र मुद्राएं जारी ही नहीं की गयी थीं। विदिशा से प्राप्त तीर्थंकर मूर्तियों ने गुप्त राजवंश के इतिहास की उपर्युक्त समस्या का भी पूरी तरह समाधान कर दिया है। इन मूर्ति लेखों में 'महाराजाधिराज' की उपाधि के साथ रामगुप्त का नामोल्लेख हुआ है। महाराजाधिराज की उपाधि सभी मुख्य गुप्तशासकों जैसे चन्द्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम आदि ने धारण की थी, फलतः साहित्यिक एवं मुद्रा-साक्ष्यों को ये तीर्थंकर मूर्तियां पुष्ट करती हैं। मूर्तिलेख के अतिरिक्त लाक्षणिक एवं शैलीगत विशेषताओं के आधार पर भी ये तीर्थंकर मूर्तियाँ समुद्रगुप्त एवं चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन के मध्य यानी ३७५ से ३८० ई. के बीच की ही जान पड़ती हैं। यह ऐसा संक्रमण काल था जब कुषाण कला शैली का प्रभाव न तो पूरी तरह समाप्त हुआ था और न ही गुप्त काल की सहज-स्वाभाविक कला शैली पूरी तरह स्थापित हुई थी। इस प्रकार विदिशा की ये जैन मूर्तियां न केवल जैनधर्म, कला और आस्था की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं, वरन् गुप्त शासक समुद्रगुप्त के ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त की ऐतिहासिकता की दृष्टि से भी एकमात्र ज्ञात प्रामाणिक पुरातात्विक साक्ष्य हैं। विदिशा की तीन तीर्थंकर मूर्तियों में से दो मूर्तियों के लेखों में तीर्थंकरों के नाम चन्द्रप्रभ (आठवें तीर्थंकर) एवं पुष्पदन्त (नवें तीर्थंकर) अभिलिखित हैं। इन मूर्तियों के बारे में आर.सी. अग्रवाल ने सर्वप्रथम लेख प्रकाशित किया और बाद में यू.पी. शाह ने भी उसपर अपना अभिमत दिया है।३ तीनों ही मूर्तियों में तीर्थंकरों के साथ पहचान के लिए कोई लांछन या चिह्न नहीं उत्कीर्ण किया गया है। लगभग ५० वर्ष बाद की चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय की पांचवीं शती ई. के प्रारंभ की राजगिर (बिहार) से प्राप्त तीर्थंकर मूर्ति में ही पहली बार लांछन (शंख) का अंकन हुआ है, जिसके आधार पर राजगिर की मूर्ति की पहचान २२वें तीर्थंकर नेमिनाथ से की जा सकी है। लांछन न होते हुए भी विदिशा की मूर्तियों में