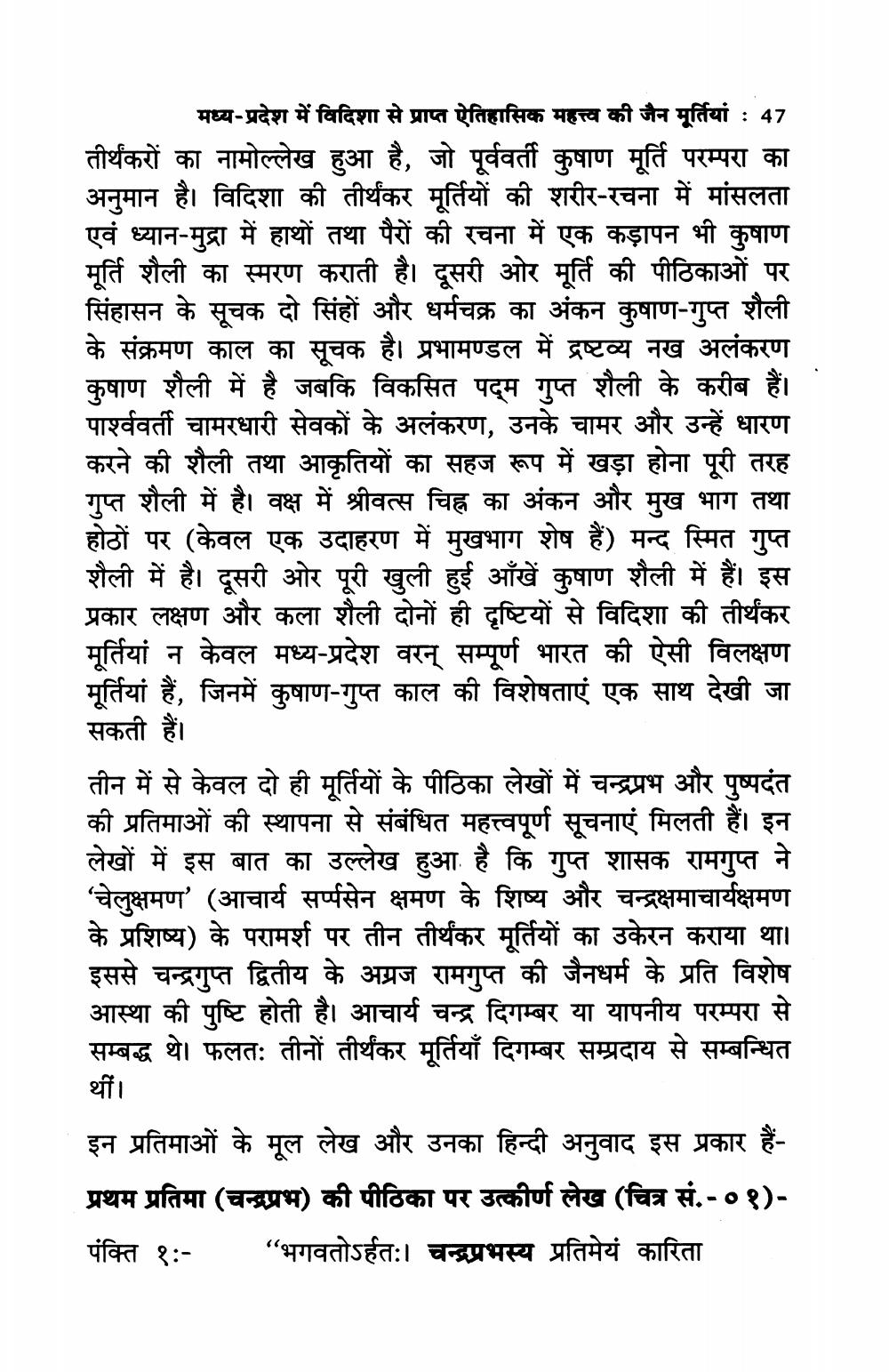________________
मध्य-प्रदेश में विदिशा से प्राप्त ऐतिहासिक महत्त्व की जैन मूर्तियां : 47 तीर्थंकरों का नामोल्लेख हुआ है, जो पूर्ववर्ती कुषाण मूर्ति परम्परा का अनुमान है। विदिशा की तीर्थंकर मूर्तियों की शरीर-रचना में मांसलता एवं ध्यान-मद्रा में हाथों तथा पैरों की रचना में एक कड़ापन भी कुषाण मूर्ति शैली का स्मरण कराती है। दूसरी ओर मूर्ति की पीठिकाओं पर सिंहासन के सूचक दो सिंहों और धर्मचक्र का अंकन कुषाण-गुप्त शैली के संक्रमण काल का सूचक है। प्रभामण्डल में द्रष्टव्य नख अलंकरण कुषाण शैली में है जबकि विकसित पद्म गुप्त शैली के करीब हैं। पार्श्ववर्ती चामरधारी सेवकों के अलंकरण, उनके चामर और उन्हें धारण करने की शैली तथा आकृतियों का सहज रूप में खड़ा होना पूरी तरह गुप्त शैली में है। वक्ष में श्रीवत्स चिह्न का अंकन और मुख भाग तथा होठों पर (केवल एक उदाहरण में मुखभाग शेष हैं) मन्द स्मित गुप्त शैली में है। दूसरी ओर पूरी खुली हुई आँखें कुषाण शैली में हैं। इस प्रकार लक्षण और कला शैली दोनों ही दृष्टियों से विदिशा की तीर्थंकर मूर्तियां न केवल मध्य-प्रदेश वरन् सम्पूर्ण भारत की ऐसी विलक्षण मूर्तियां हैं, जिनमें कुषाण-गुप्त काल की विशेषताएं एक साथ देखी जा सकती हैं। तीन में से केवल दो ही मूर्तियों के पीठिका लेखों में चन्द्रप्रभ और पुष्पदंत की प्रतिमाओं की स्थापना से संबंधित महत्त्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। इन लेखों में इस बात का उल्लेख हुआ है कि गुप्त शासक रामगुप्त ने 'चेलुक्षमण' (आचार्य सर्पसेन क्षमण के शिष्य और चन्द्रक्षमाचार्यक्षमण के प्रशिष्य) के परामर्श पर तीन तीर्थंकर मूर्तियों का उकेरन कराया था। इससे चन्द्रगुप्त द्वितीय के अग्रज रामगुप्त की जैनधर्म के प्रति विशेष आस्था की पुष्टि होती है। आचार्य चन्द्र दिगम्बर या यापनीय परम्परा से सम्बद्ध थे। फलत: तीनों तीर्थंकर मूर्तियाँ दिगम्बर सम्प्रदाय से सम्बन्धित थीं। इन प्रतिमाओं के मूल लेख और उनका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार हैंप्रथम प्रतिमा (चन्द्रप्रभ) की पीठिका पर उत्कीर्ण लेख (चित्र सं.-०१)पंक्ति १:- “भगवतोऽर्हतः। चन्द्रप्रभस्य प्रतिमेयं कारिता