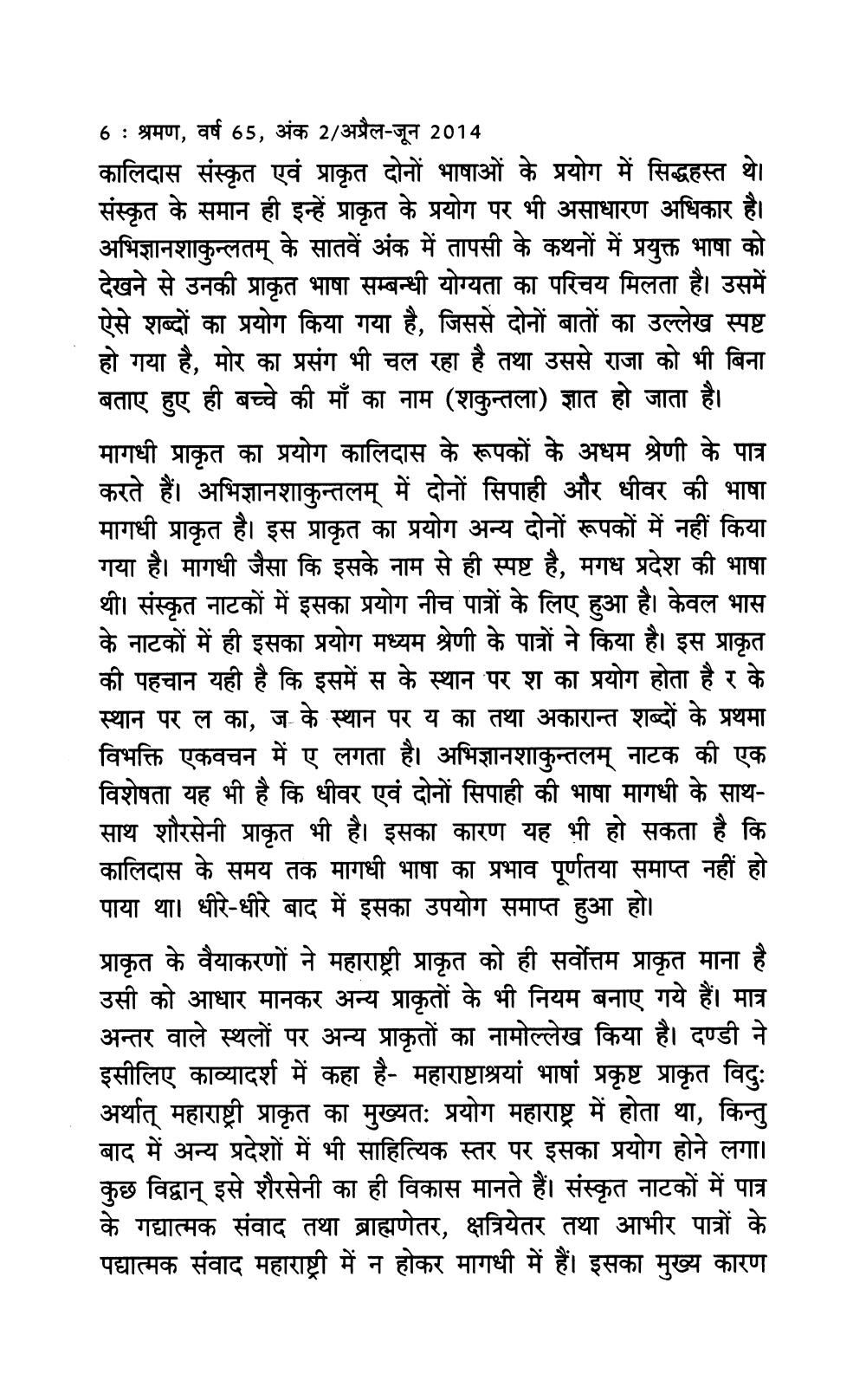________________
6 : श्रमण, वर्ष 65, अंक 2/अप्रैल-जून 2014 कालिदास संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाओं के प्रयोग में सिद्धहस्त थे। संस्कृत के समान ही इन्हें प्राकृत के प्रयोग पर भी असाधारण अधिकार है। अभिज्ञानशाकुन्लतम् के सातवें अंक में तापसी के कथनों में प्रयुक्त भाषा को देखने से उनकी प्राकृत भाषा सम्बन्धी योग्यता का परिचय मिलता है। उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे दोनों बातों का उल्लेख स्पष्ट हो गया है, मोर का प्रसंग भी चल रहा है तथा उससे राजा को भी बिना बताए हुए ही बच्चे की माँ का नाम (शकुन्तला) ज्ञात हो जाता है। मागधी प्राकृत का प्रयोग कालिदास के रूपकों के अधम श्रेणी के पात्र करते हैं। अभिज्ञानशाकुन्तलम् में दोनों सिपाही और धीवर की भाषा मागधी प्राकृत है। इस प्राकृत का प्रयोग अन्य दोनों रूपकों में नहीं किया गया है। मागधी जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, मगध प्रदेश की भाषा थी। संस्कृत नाटकों में इसका प्रयोग नीच पात्रों के लिए हुआ है। केवल भास के नाटकों में ही इसका प्रयोग मध्यम श्रेणी के पात्रों ने किया है। इस प्राकृत की पहचान यही है कि इसमें स के स्थान पर श का प्रयोग होता है र के स्थान पर ल का, ज के स्थान पर य का तथा अकारान्त शब्दों के प्रथमा विभक्ति एकवचन में ए लगता है। अभिज्ञानशाकुन्तलम् नाटक की एक विशेषता यह भी है कि धीवर एवं दोनों सिपाही की भाषा मागधी के साथसाथ शौरसेनी प्राकृत भी है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि कालिदास के समय तक मागधी भाषा का प्रभाव पूर्णतया समाप्त नहीं हो पाया था। धीरे-धीरे बाद में इसका उपयोग समाप्त हुआ हो। प्राकृत के वैयाकरणों ने महाराष्ट्री प्राकृत को ही सर्वोत्तम प्राकृत माना है उसी को आधार मानकर अन्य प्राकृतों के भी नियम बनाए गये हैं। मात्र अन्तर वाले स्थलों पर अन्य प्राकृतों का नामोल्लेख किया है। दण्डी ने इसीलिए काव्यादर्श में कहा है- महाराष्टाश्रयां भाषां प्रकृष्ट प्राकृत विदुः अर्थात् महाराष्ट्री प्राकृत का मुख्यत: प्रयोग महाराष्ट्र में होता था, किन्तु बाद में अन्य प्रदेशों में भी साहित्यिक स्तर पर इसका प्रयोग होने लगा। कुछ विद्वान् इसे शैरसेनी का ही विकास मानते हैं। संस्कृत नाटकों में पात्र के गद्यात्मक संवाद तथा ब्राह्मणेतर, क्षत्रियेतर तथा आभीर पात्रों के पद्यात्मक संवाद महाराष्ट्री में न होकर मागधी में हैं। इसका मुख्य कारण