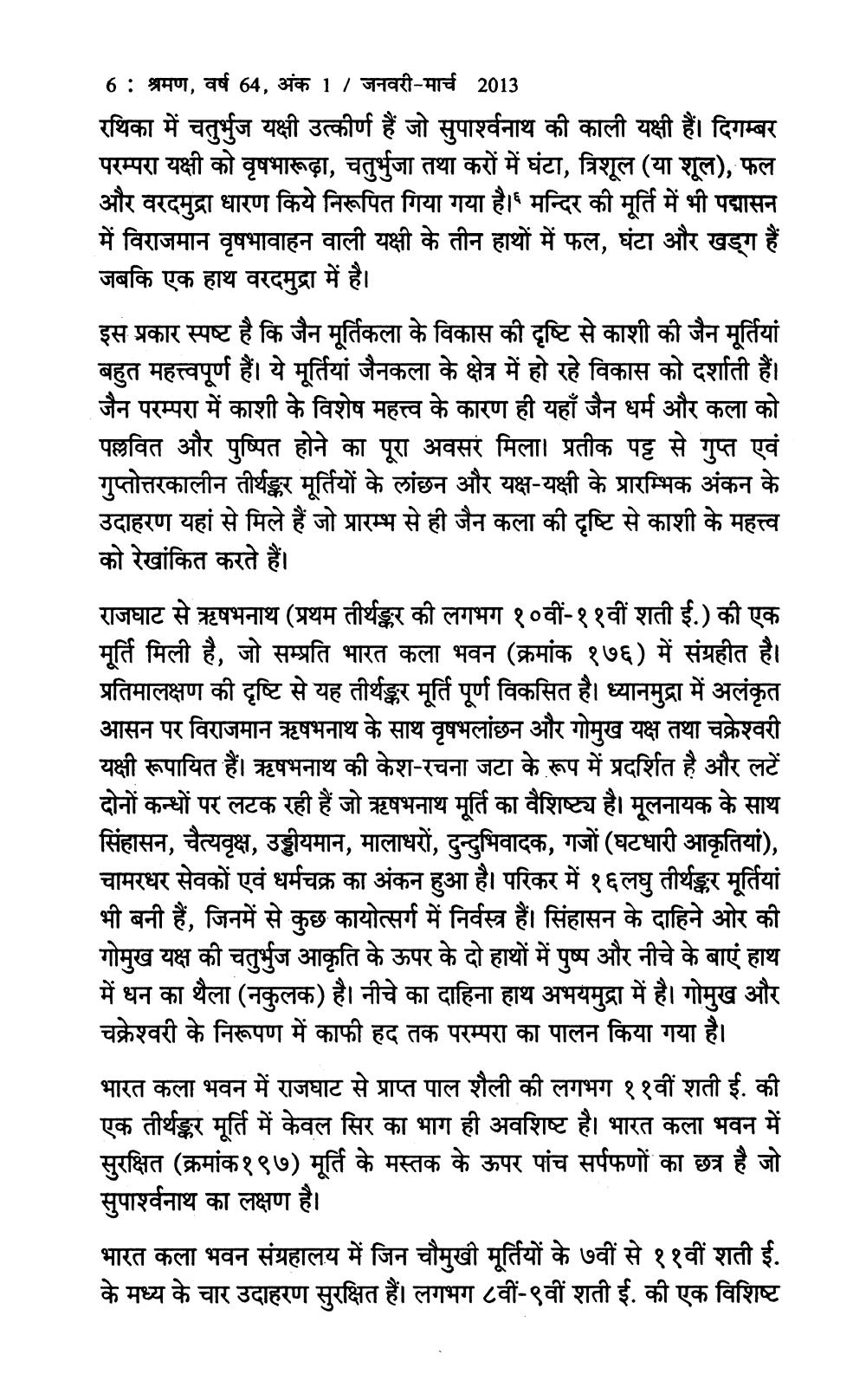________________
6 : श्रमण, वर्ष 64, अंक 1 / जनवरी-मार्च 2013 रथिका में चतुर्भुज यक्षी उत्कीर्ण हैं जो सुपार्श्वनाथ की काली यक्षी हैं। दिगम्बर परम्परा यक्षी को वृषभारूढ़ा, चतुर्भुजा तथा करों में घंटा, त्रिशूल (या शूल), फल
और वरदमुद्रा धारण किये निरूपित गिया गया है। मन्दिर की मूर्ति में भी पद्मासन में विराजमान वृषभावाहन वाली यक्षी के तीन हाथों में फल, घंटा और खड्ग हैं जबकि एक हाथ वरदमुद्रा में है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जैन मूर्तिकला के विकास की दृष्टि से काशी की जैन मूर्तियां बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। ये मूर्तियां जैनकला के क्षेत्र में हो रहे विकास को दर्शाती हैं। जैन परम्परा में काशी के विशेष महत्त्व के कारण ही यहाँ जैन धर्म और कला को पल्लवित और पुष्पित होने का पूरा अवसर मिला। प्रतीक पट्ट से गुप्त एवं गुप्तोत्तरकालीन तीर्थङ्कर मूर्तियों के लांछन और यक्ष-यक्षी के प्रारम्भिक अंकन के उदाहरण यहां से मिले हैं जो प्रारम्भ से ही जैन कला की दृष्टि से काशी के महत्त्व को रेखांकित करते हैं। राजघाट से ऋषभनाथ (प्रथम तीर्थङ्कर की लगभग १०वीं-११वीं शती ई.) की एक मूर्ति मिली है, जो सम्प्रति भारत कला भवन (क्रमांक १७६) में संग्रहीत है। प्रतिमालक्षण की दृष्टि से यह तीर्थङ्कर मूर्ति पूर्ण विकसित है। ध्यानमुद्रा में अलंकृत आसन पर विराजमान ऋषभनाथ के साथ वृषभलांछन और गोमुख यक्ष तथा चक्रेश्वरी यक्षी रूपायित हैं। ऋषभनाथ की केश-रचना जटा के रूप में प्रदर्शित है और लटें दोनों कन्धों पर लटक रही हैं जो ऋषभनाथ मूर्ति का वैशिष्ट्य है। मूलनायक के साथ सिंहासन, चैत्यवृक्ष, उड्डीयमान, मालाधरों, दुन्दुभिवादक, गजों (घटधारी आकृतियां), चामरधर सेवकों एवं धर्मचक्र का अंकन हुआ है। परिकर में १६लघु तीर्थङ्कर मूर्तियां भी बनी हैं, जिनमें से कुछ कायोत्सर्ग में निर्वस्त्र हैं। सिंहासन के दाहिने ओर की गोमुख यक्ष की चतुर्भुज आकृति के ऊपर के दो हाथों में पुष्प और नीचे के बाएं हाथ में धन का थैला (नकुलक) है। नीचे का दाहिना हाथ अभयमुद्रा में है। गोमुख और चक्रेश्वरी के निरूपण में काफी हद तक परम्परा का पालन किया गया है। भारत कला भवन में राजघाट से प्राप्त पाल शैली की लगभग ११वीं शती ई. की एक तीर्थङ्कर मूर्ति में केवल सिर का भाग ही अवशिष्ट है। भारत कला भवन में सुरक्षित (क्रमांक १९७) मूर्ति के मस्तक के ऊपर पांच सर्पफणों का छत्र है जो सुपार्श्वनाथ का लक्षण है। भारत कला भवन संग्रहालय में जिन चौमुखी मूर्तियों के ७वीं से ११वीं शती ई. के मध्य के चार उदाहरण सुरक्षित हैं। लगभग ८वीं-९वीं शती ई. की एक विशिष्ट