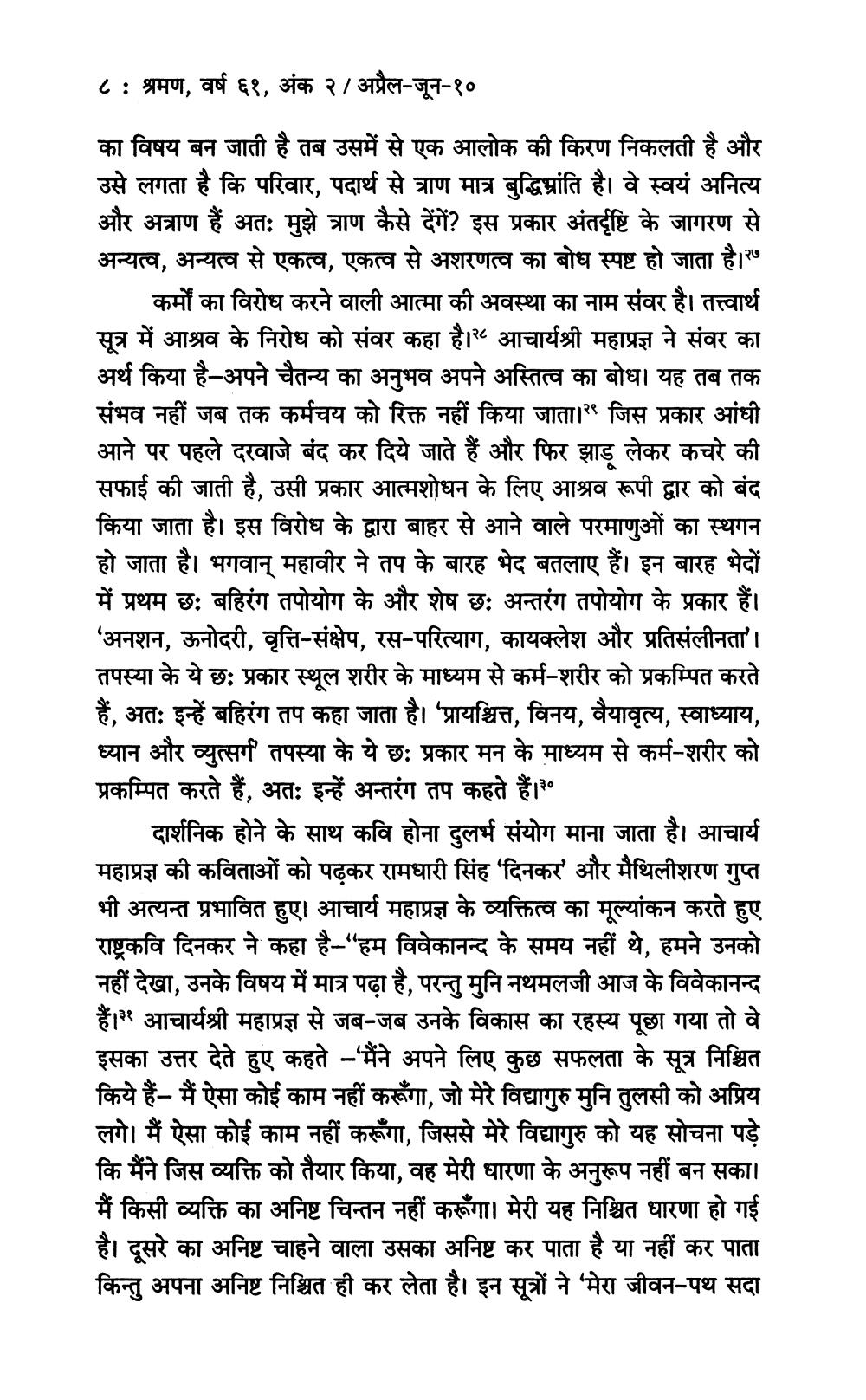________________
८ : श्रमण, वर्ष ६१, अंक २ / अप्रैल-जून-१०
का विषय बन जाती है तब उसमें से एक आलोक की किरण निकलती है और उसे लगता है कि परिवार, पदार्थ से त्राण मात्र बुद्धिभ्रांति है। वे स्वयं अनित्य
और अत्राण हैं अतः मुझे त्राण कैसे देंगें? इस प्रकार अंतर्दृष्टि के जागरण से अन्यत्व, अन्यत्व से एकत्व, एकत्व से अशरणत्व का बोध स्पष्ट हो जाता है।"
कर्मों का विरोध करने वाली आत्मा की अवस्था का नाम संवर है। तत्त्वार्थ सूत्र में आश्रव के निरोध को संवर कहा है।८ आचार्यश्री महाप्रज्ञ ने संवर का अर्थ किया है-अपने चैतन्य का अनुभव अपने अस्तित्व का बोध। यह तब तक संभव नहीं जब तक कर्मचय को रिक्त नहीं किया जाता।२९ जिस प्रकार आंधी आने पर पहले दरवाजे बंद कर दिये जाते हैं और फिर झाड़ लेकर कचरे की सफाई की जाती है, उसी प्रकार आत्मशोधन के लिए आश्रव रूपी द्वार को बंद किया जाता है। इस विरोध के द्वारा बाहर से आने वाले परमाणुओं का स्थगन हो जाता है। भगवान् महावीर ने तप के बारह भेद बतलाए हैं। इन बारह भेदों में प्रथम छः बहिरंग तपोयोग के और शेष छः अन्तरंग तपोयोग के प्रकार हैं। 'अनशन, ऊनोदरी, वृत्ति-संक्षेप, रस-परित्याग, कायक्लेश और प्रतिसंलीनता'। तपस्या के ये छः प्रकार स्थूल शरीर के माध्यम से कर्म-शरीर को प्रकम्पित करते हैं, अतः इन्हें बहिरंग तप कहा जाता है। 'प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग तपस्या के ये छः प्रकार मन के माध्यम से कर्म-शरीर को प्रकम्पित करते हैं, अतः इन्हें अन्तरंग तप कहते हैं।
दार्शनिक होने के साथ कवि होना दुलर्भ संयोग माना जाता है। आचार्य महाप्रज्ञ की कविताओं को पढ़कर रामधारी सिंह 'दिनकर' और मैथिलीशरण गुप्त भी अत्यन्त प्रभावित हुए। आचार्य महाप्रज्ञ के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हुए राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है-"हम विवेकानन्द के समय नहीं थे, हमने उनको नहीं देखा, उनके विषय में मात्र पढ़ा है, परन्तु मुनि नथमलजी आज के विवेकानन्द हैं। आचार्यश्री महाप्रज्ञ से जब-जब उनके विकास का रहस्य पूछा गया तो वे इसका उत्तर देते हुए कहते –'मैंने अपने लिए कुछ सफलता के सूत्र निश्चित किये हैं- मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, जो मेरे विद्यागुरु मुनि तुलसी को अप्रिय लगे। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, जिससे मेरे विद्यागुरु को यह सोचना पड़े कि मैंने जिस व्यक्ति को तैयार किया, वह मेरी धारणा के अनुरूप नहीं बन सका। मैं किसी व्यक्ति का अनिष्ट चिन्तन नहीं करूंगा। मेरी यह निश्चित धारणा हो गई है। दूसरे का अनिष्ट चाहने वाला उसका अनिष्ट कर पाता है या नहीं कर पाता किन्तु अपना अनिष्ट निश्चित ही कर लेता है। इन सूत्रों ने 'मेरा जीवन-पथ सदा