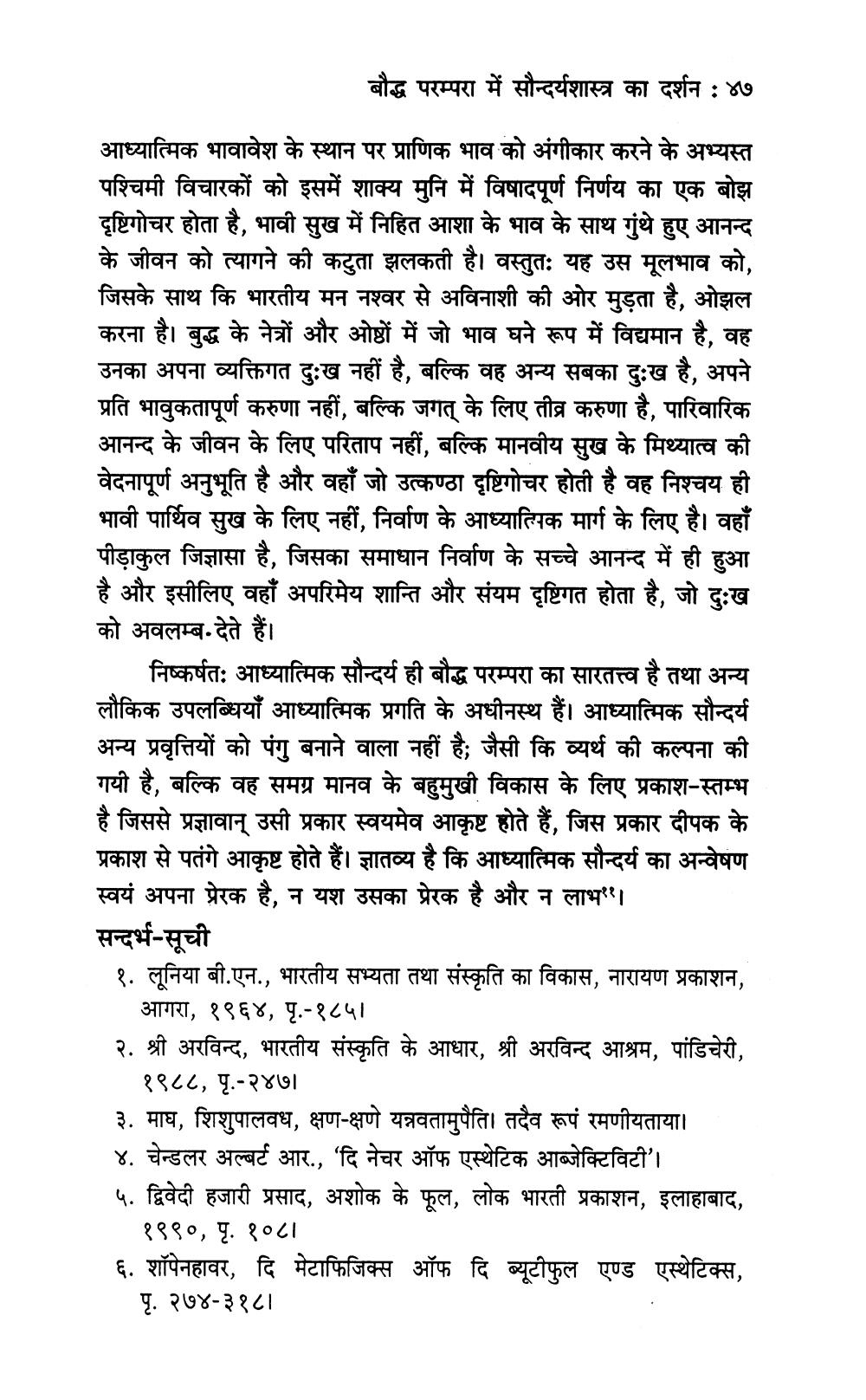________________
बौद्ध परम्परा में सौन्दर्यशास्त्र का दर्शन : ४७
आध्यात्मिक भावावेश के स्थान पर प्राणिक भाव को अंगीकार करने के अभ्यस्त पश्चिमी विचारकों को इसमें शाक्य मुनि में विषादपूर्ण निर्णय का एक बोझ दृष्टिगोचर होता है, भावी सुख में निहित आशा के भाव के साथ गुंथे हुए आनन्द के जीवन को त्यागने की कटुता झलकती है। वस्तुतः यह उस मूलभाव को, जिसके साथ कि भारतीय मन नश्वर से अविनाशी की ओर मुड़ता है, ओझल करना है। बुद्ध के नेत्रों और ओष्ठों में जो भाव घने रूप में विद्यमान है, वह उनका अपना व्यक्तिगत दुःख नहीं है, बल्कि वह अन्य सबका दुःख है, अपने प्रति भावुकतापूर्ण करुणा नहीं, बल्कि जगत् के लिए तीव्र करुणा है, पारिवारिक आनन्द के जीवन के लिए परिताप नहीं, बल्कि मानवीय सुख के मिथ्यात्व की वेदनापूर्ण अनुभूति है और वहाँ जो उत्कण्ठा दृष्टिगोचर होती है वह निश्चय ही भावी पार्थिव सुख लिए नहीं, निर्वाण के आध्यात्मिक मार्ग के लिए है । वहाँ पीड़ाकुल जिज्ञासा है, जिसका समाधान निर्वाण के सच्चे आनन्द में ही हुआ है और इसीलिए वहाँ अपरिमेय शान्ति और संयम दृष्टिगत होता है, जो दुःख को अवलम्ब देते हैं।
निष्कर्षतः आध्यात्मिक सौन्दर्य ही बौद्ध परम्परा का सारतत्त्व है तथा अन्य लौकिक उपलब्धियाँ आध्यात्मिक प्रगति के अधीनस्थ हैं। आध्यात्मिक सौन्दर्य अन्य प्रवृत्तियों को पंगु बनाने वाला नहीं है; जैसी कि व्यर्थ की कल्पना की गयी है, बल्कि वह समग्र मानव के बहुमुखी विकास के लिए प्रकाश स्तम्भ है जिससे प्रज्ञावान् उसी प्रकार स्वयमेव आकृष्ट होते हैं, जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से पतंगे आकृष्ट होते हैं। ज्ञातव्य है कि आध्यात्मिक सौन्दर्य का अन्वेषण स्वयं अपना प्रेरक है, न यश उसका प्रेरक है और न लाभ " ।
सन्दर्भ - सूची
,
१. लूनिया बी. एन. भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का विकास, नारायण प्रकाशन, आगरा, १९६४, पृ. १८५
२. श्री अरविन्द, भारतीय संस्कृति के आधार, श्री अरविन्द आश्रम, पांडिचेरी, १९८८, पृ. - २४७
३. माघ, शिशुपालवध, क्षण-क्षणे यन्नवतामुपैति । तदैव रूपं रमणीयताया।
४. चेन्डलर अल्बर्ट आर., 'दि नेचर ऑफ एस्थेटिक आब्जेक्टिविटी' ।
५. द्विवेदी हजारी प्रसाद, अशोक के फूल, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद,
१९९०, पृ. १०८
६. शॉपेनहावर, दि मेटाफिजिक्स ऑफ दि ब्यूटीफुल एण्ड एस्थेटिक्स, पृ. २७४-३१८।