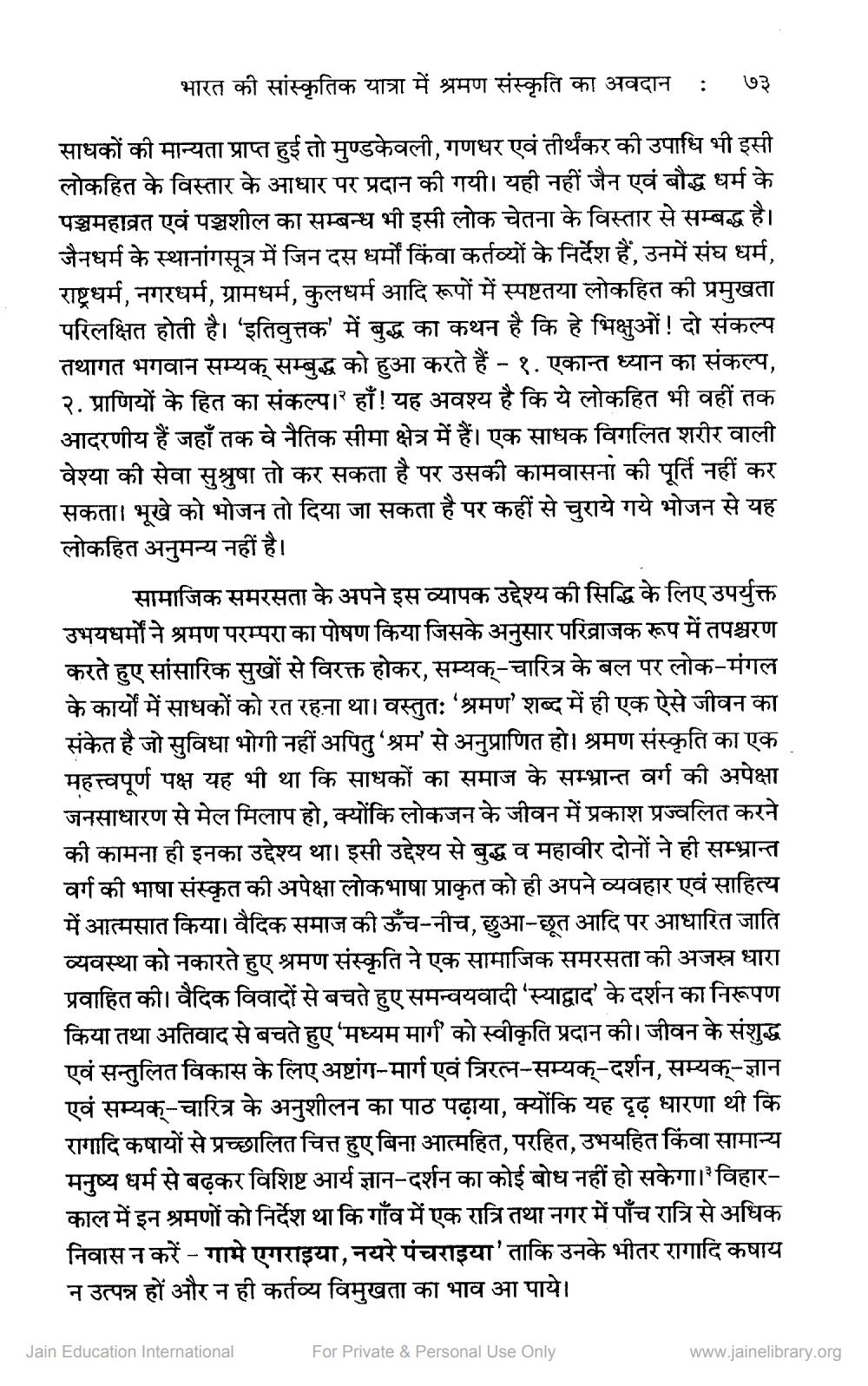________________
भारत की सांस्कृतिक यात्रा में श्रमण संस्कृति का अवदान : ७३
साधकों की मान्यता प्राप्त हुई तो मुण्डकेवली, गणधर एवं तीर्थंकर की उपाधि भी इसी लोकहित के विस्तार के आधार पर प्रदान की गयी। यही नहीं जैन एवं बौद्ध धर्म के पञ्चमहाव्रत एवं पञ्चशील का सम्बन्ध भी इसी लोक चेतना के विस्तार से सम्बद्ध है। जैनधर्म के स्थानांगसूत्र में जिन दस धर्मों किंवा कर्तव्यों के निर्देश हैं, उनमें संघ धर्म, राष्ट्रधर्म, नगरधर्म, ग्रामधर्म, कुलधर्म आदि रूपों में स्पष्टतया लोकहित की प्रमुखता परिलक्षित होती है। 'इतिवृत्तक' में बुद्ध का कथन है कि हे भिक्षुओं! दो संकल्प तथागत भगवान सम्यक् सम्बुद्ध को हुआ करते हैं - १. एकान्त ध्यान का संकल्प, २. प्राणियों के हित का संकल्पा हाँ! यह अवश्य है कि ये लोकहित भी वहीं तक आदरणीय हैं जहाँ तक वे नैतिक सीमा क्षेत्र में हैं। एक साधक विगलित शरीर वाली वेश्या की सेवा सुश्रुषा तो कर सकता है पर उसकी कामवासना की पूर्ति नहीं कर सकता। भूखे को भोजन तो दिया जा सकता है पर कहीं से चुराये गये भोजन से यह लोकहित अनुमन्य नहीं है।
सामाजिक समरसता के अपने इस व्यापक उद्देश्य की सिद्धि के लिए उपर्युक्त उभयधर्मों ने श्रमण परम्परा का पोषण किया जिसके अनुसार परिव्राजक रूप में तपश्चरण करते हुए सांसारिक सुखों से विरक्त होकर, सम्यक्-चारित्र के बल पर लोक-मंगल के कार्यों में साधकों को रत रहना था। वस्तुतः 'श्रमण' शब्द में ही एक ऐसे जीवन का संकेत है जो सुविधा भोगी नहीं अपितु श्रम' से अनुप्राणित हो। श्रमण संस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह भी था कि साधकों का समाज के सम्भ्रान्त वर्ग की अपेक्षा जनसाधारण से मेल मिलाप हो, क्योंकि लोकजन के जीवन में प्रकाश प्रज्वलित करने की कामना ही इनका उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से बुद्ध व महावीर दोनों ने ही सम्भ्रान्त वर्ग की भाषा संस्कृत की अपेक्षा लोकभाषा प्राकृत को ही अपने व्यवहार एवं साहित्य में आत्मसात किया। वैदिक समाज की ऊँच-नीच, छुआ-छूत आदि पर आधारित जाति व्यवस्था को नकारते हुए श्रमण संस्कृति ने एक सामाजिक समरसता की अजस्त्र धारा प्रवाहित की। वैदिक विवादों से बचते हुए समन्वयवादी 'स्याद्वाद' के दर्शन का निरूपण किया तथा अतिवाद से बचते हुए 'मध्यम मार्ग को स्वीकृति प्रदान की। जीवन के संशुद्ध एवं सन्तुलित विकास के लिए अष्टांग-मार्ग एवं त्रिरत्न-सम्यक्-दर्शन, सम्यक्-ज्ञान एवं सम्यक्-चारित्र के अनुशीलन का पाठ पढ़ाया, क्योंकि यह दृढ़ धारणा थी कि रागादि कषायों से प्रच्छालित चित्त हुए बिना आत्महित, परहित, उभयहित किंवा सामान्य मनुष्य धर्म से बढ़कर विशिष्ट आर्य ज्ञान-दर्शन का कोई बोध नहीं हो सकेगा। विहारकाल में इन श्रमणों को निर्देश था कि गाँव में एक रात्रि तथा नगर में पाँच रात्रि से अधिक निवास न करें - गामे एगराइया, नयरे पंचराइया' ताकि उनके भीतर रागादि कषाय न उत्पन्न हों और न ही कर्तव्य विमुखता का भाव आ पाये।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org