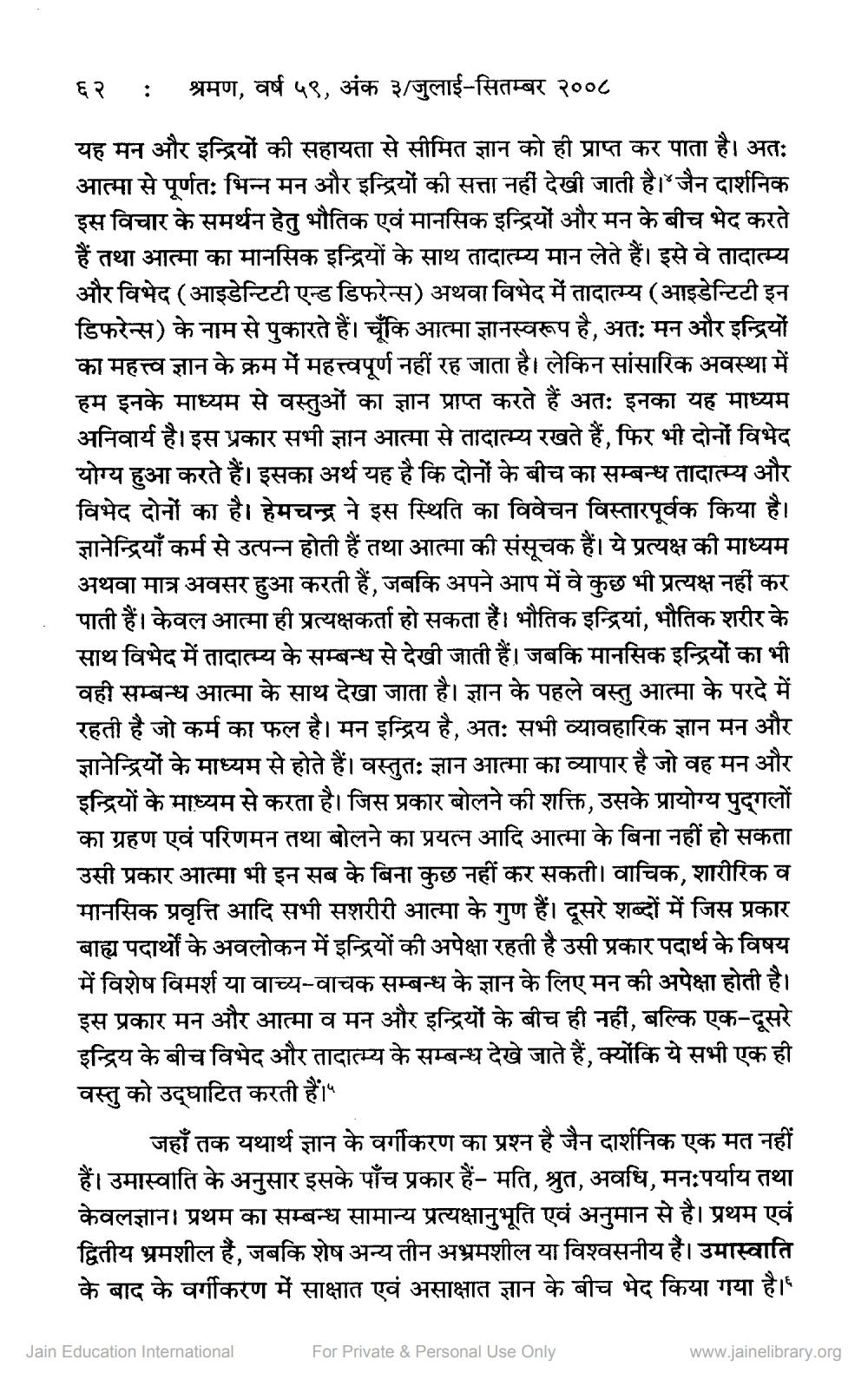________________
६२ : श्रमण, वर्ष ५९, अंक ३ / जुलाई-सितम्बर २००८
यह मन और इन्द्रियों की सहायता से सीमित ज्ञान को ही प्राप्त कर पाता है। अतः आत्मा से पूर्णतः भिन्न मन और इन्द्रियों की सत्ता नहीं देखी जाती है।' जैन दार्शनिक इस विचार के समर्थन हेतु भौतिक एवं मानसिक इन्द्रियों और मन के बीच भेद करते हैं तथा आत्मा का मानसिक इन्द्रियों के साथ तादात्म्य मान लेते हैं। इसे वे तादात्म्य और विभेद (आइडेन्टिटी एन्ड डिफरेन्स) अथवा विभेद में तादात्म्य (आइडेन्टिटी इन डिफरेन्स) के नाम से पुकारते हैं। चूँकि आत्मा ज्ञानस्वरूप है, अतः मन और इन्द्रियों का महत्त्व ज्ञान के क्रम में महत्त्वपूर्ण नहीं रह जाता है। लेकिन सांसारिक अवस्था में हम इनके माध्यम से वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं अतः इनका यह माध्यम अनिवार्य है । इस प्रकार सभी ज्ञान आत्मा से तादात्म्य रखते हैं, फिर भी दोनों विभेद योग्य हुआ करते हैं। इसका अर्थ यह है कि दोनों के बीच का सम्बन्ध तादात्म्य और विभेद दोनों का है। हेमचन्द्र ने इस स्थिति का विवेचन विस्तारपूर्वक किया है। ज्ञानेन्द्रियाँ कर्म से उत्पन्न होती हैं तथा आत्मा की संसूचक हैं। ये प्रत्यक्ष की माध्यम अथवा मात्र अवसर हुआ करती हैं, जबकि अपने आप में वे कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं कर पाती हैं। केवल आत्मा ही प्रत्यक्षकर्ता हो सकता हैं। भौतिक इन्द्रियां, भौतिक शरीर के साथ विभेद में तादात्म्य के सम्बन्ध से देखी जाती हैं। जबकि मानसिक इन्द्रियों का भी वही सम्बन्ध आत्मा के साथ देखा जाता है। ज्ञान के पहले वस्तु आत्मा के परदे में रहती है जो कर्म का फल है। मन इन्द्रिय है, अतः सभी व्यावहारिक ज्ञान मन और ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से होते हैं। वस्तुत: ज्ञान आत्मा का व्यापार है जो वह मन और इन्द्रियों के माध्यम से करता है । जिस प्रकार बोलने की शक्ति, उसके प्रायोग्य पुद्गलों का ग्रहण एवं परिणमन तथा बोलने का प्रयत्न आदि आत्मा के बिना नहीं हो सकता उसी प्रकार आत्मा भी इन सब के बिना कुछ नहीं कर सकती । वाचिक, शारीरिक व मानसिक प्रवृत्ति आदि सभी सशरीरी आत्मा के गुण हैं। दूसरे शब्दों में जिस प्रकार बाह्य पदार्थों के अवलोकन में इन्द्रियों की अपेक्षा रहती है उसी प्रकार पदार्थ के विषय में विशेष विमर्श या वाच्य वाचक सम्बन्ध के ज्ञान के लिए मन की अपेक्षा होती है। इस प्रकार मन और आत्मा व मन और इन्द्रियों के बीच ही नहीं, बल्कि एक-दूसरे इन्द्रिय के बीच विभेद और तादात्म्य के सम्बन्ध देखे जाते हैं, क्योंकि ये सभी एक ही वस्तु को उद्घाटित करती हैं।"
जहाँ तक यथार्थ ज्ञान के वर्गीकरण का प्रश्न है जैन दार्शनिक एक मत नहीं हैं। उमास्वाति के अनुसार इसके पाँच प्रकार हैं- मति, श्रुत, अवधि, मन: पर्याय तथा केवलज्ञान। प्रथम का सम्बन्ध सामान्य प्रत्यक्षानुभूति एवं अनुमान से है। प्रथम एवं द्वितीय भ्रमशील है, जबकि शेष अन्य तीन अभ्रमशील या विश्वसनीय है । उमास्वाति के बाद के वर्गीकरण में साक्षात एवं असाक्षात ज्ञान के बीच भेद किया गया है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org