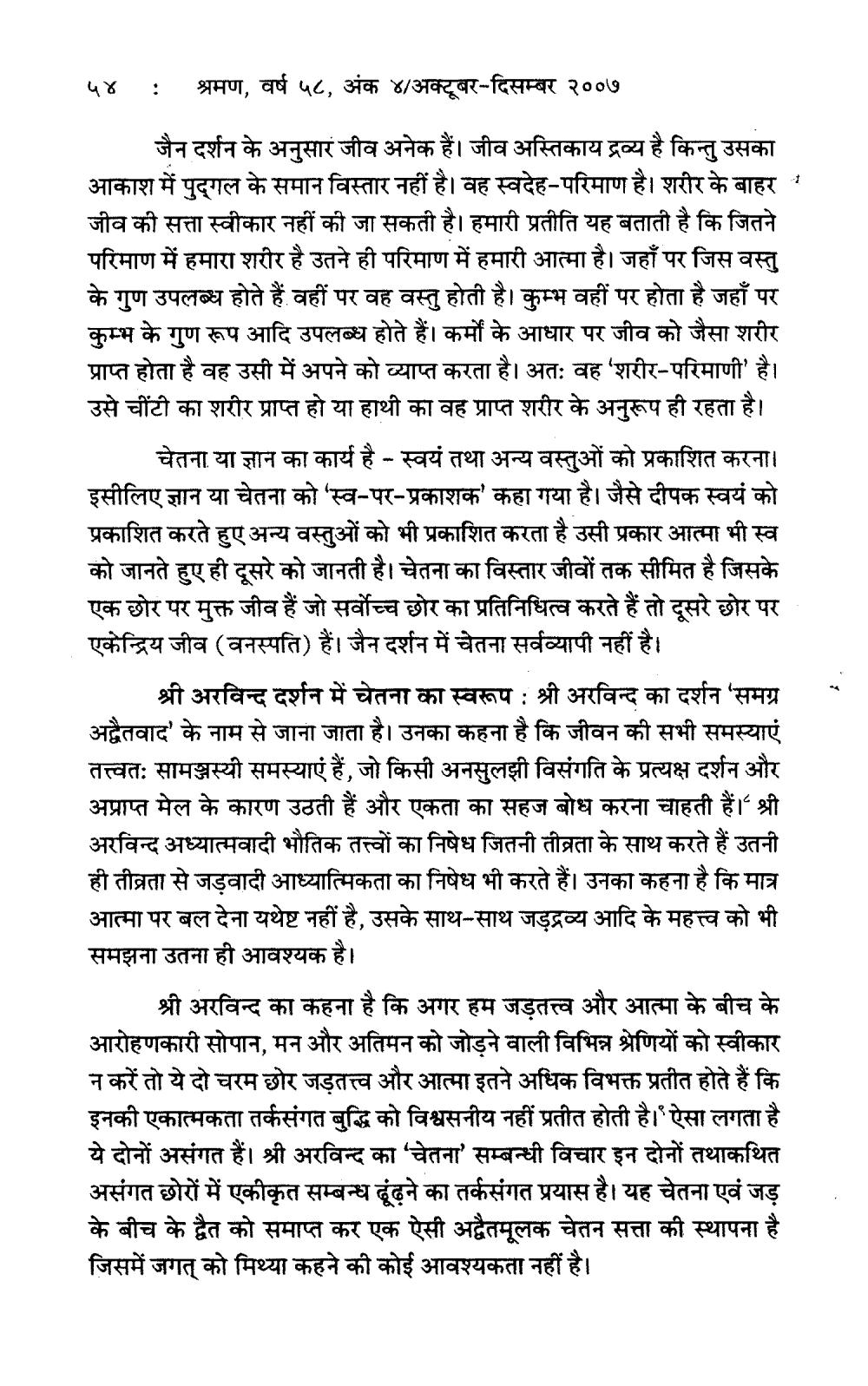________________
५४ : श्रमण, वर्ष ५८, अंक ४/अक्टूबर-दिसम्बर २००७
जैन दर्शन के अनुसार जीव अनेक हैं। जीव अस्तिकाय द्रव्य है किन्तु उसका आकाश में पुद्गल के समान विस्तार नहीं है। वह स्वदेह-परिमाण है। शरीर के बाहर । जीव की सत्ता स्वीकार नहीं की जा सकती है। हमारी प्रतीति यह बताती है कि जितने परिमाण में हमारा शरीर है उतने ही परिमाण में हमारी आत्मा है। जहाँ पर जिस वस्तु के गुण उपलब्ध होते हैं वहीं पर वह वस्तु होती है। कुम्भ वहीं पर होता है जहाँ पर कुम्भ के गुण रूप आदि उपलब्ध होते हैं। कर्मों के आधार पर जीव को जैसा शरीर प्राप्त होता है वह उसी में अपने को व्याप्त करता है। अत: वह 'शरीर-परिमाणी' है। उसे चींटी का शरीर प्राप्त हो या हाथी का वह प्राप्त शरीर के अनुरूप ही रहता है।
चेतना या ज्ञान का कार्य है - स्वयं तथा अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करना। इसीलिए ज्ञान या चेतना को 'स्व-पर-प्रकाशक' कहा गया है। जैसे दीपक स्वयं को प्रकाशित करते हुए अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है उसी प्रकार आत्मा भी स्व को जानते हुए ही दूसरे को जानती है। चेतना का विस्तार जीवों तक सीमित है जिसके एक छोर पर मुक्त जीव हैं जो सर्वोच्च छोर का प्रतिनिधित्व करते हैं तो दूसरे छोर पर एकेन्द्रिय जीव (वनस्पति) हैं। जैन दर्शन में चेतना सर्वव्यापी नहीं है।
श्री अरविन्द दर्शन में चेतना का स्वरूप : श्री अरविन्द का दर्शन 'समग्र अद्वैतवाद' के नाम से जाना जाता है। उनका कहना है कि जीवन की सभी समस्याएं तत्त्वतः सामञ्जस्यी समस्याएं हैं, जो किसी अनसुलझी विसंगति के प्रत्यक्ष दर्शन और अप्राप्त मेल के कारण उठती हैं और एकता का सहज बोध करना चाहती हैं। श्री अरविन्द अध्यात्मवादी भौतिक तत्त्वों का निषेध जितनी तीव्रता के साथ करते हैं उतनी ही तीव्रता से जड़वादी आध्यात्मिकता का निषेध भी करते हैं। उनका कहना है कि मात्र आत्मा पर बल देना यथेष्ट नहीं है, उसके साथ-साथ जड़द्रव्य आदि के महत्त्व को भी समझना उतना ही आवश्यक है।
श्री अरविन्द का कहना है कि अगर हम जड़तत्त्व और आत्मा के बीच के आरोहणकारी सोपान, मन और अतिमन को जोड़ने वाली विभिन्न श्रेणियों को स्वीकार न करें तो ये दो चरम छोर जड़तत्त्व और आत्मा इतने अधिक विभक्त प्रतीत होते हैं कि इनकी एकात्मकता तर्कसंगत बुद्धि को विश्वसनीय नहीं प्रतीत होती है। ऐसा लगता है ये दोनों असंगत हैं। श्री अरविन्द का 'चेतना' सम्बन्धी विचार इन दोनों तथाकथित असंगत छोरों में एकीकृत सम्बन्ध ढूंढ़ने का तर्कसंगत प्रयास है। यह चेतना एवं जड़ के बीच के द्वैत को समाप्त कर एक ऐसी अद्वैतमूलक चेतन सत्ता की स्थापना है जिसमें जगत् को मिथ्या कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।
-