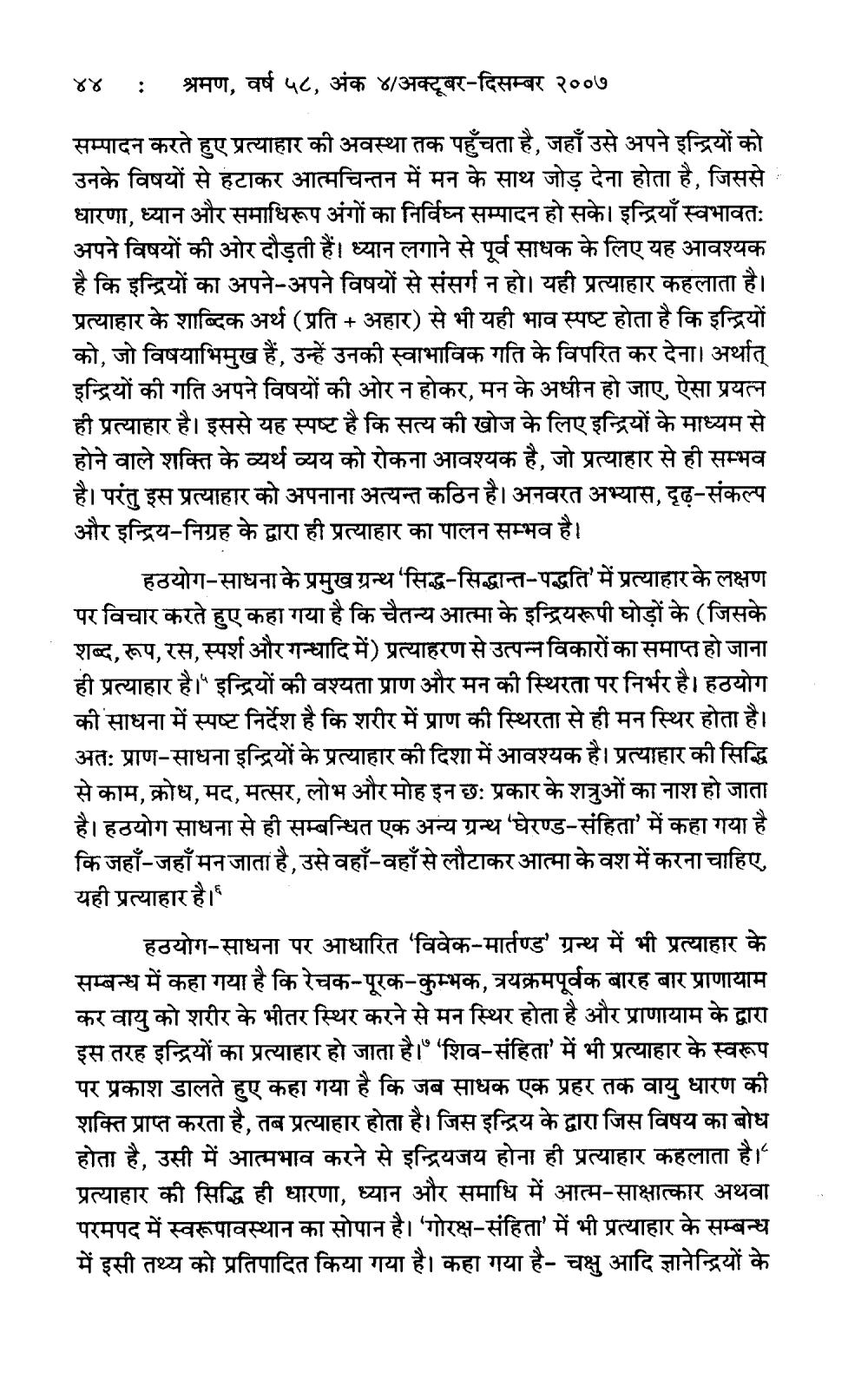________________
४४ :
श्रमण, वर्ष ५८, अंक ४/अक्टूबर-दिसम्बर २००७
सम्पादन करते हुए प्रत्याहार की अवस्था तक पहुँचता है, जहाँ उसे अपने इन्द्रियों को उनके विषयों से हटाकर आत्मचिन्तन में मन के साथ जोड़ देना होता है, जिससे धारणा, ध्यान और समाधिरूप अंगों का निर्विघ्न सम्पादन हो सके। इन्द्रियाँ स्वभावत: अपने विषयों की ओर दौड़ती हैं। ध्यान लगाने से पूर्व साधक के लिए यह आवश्यक है कि इन्द्रियों का अपने-अपने विषयों से संसर्ग न हो। यही प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार के शाब्दिक अर्थ (प्रति + अहार) से भी यही भाव स्पष्ट होता है कि इन्द्रियों को, जो विषयाभिमुख हैं, उन्हें उनकी स्वाभाविक गति के विपरित कर देना। अर्थात् इन्द्रियों की गति अपने विषयों की ओर न होकर, मन के अधीन हो जाए, ऐसा प्रयत्न ही प्रत्याहार है। इससे यह स्पष्ट है कि सत्य की खोज के लिए इन्द्रियों के माध्यम से होने वाले शक्ति के व्यर्थ व्यय को रोकना आवश्यक है, जो प्रत्याहार से ही सम्भव है। परंतु इस प्रत्याहार को अपनाना अत्यन्त कठिन है। अनवरत अभ्यास, दृढ़-संकल्प और इन्द्रिय-निग्रह के द्वारा ही प्रत्याहार का पालन सम्भव है।
हठयोग-साधना के प्रमुख ग्रन्थ सिद्ध-सिद्धान्त-पद्धति' में प्रत्याहार के लक्षण पर विचार करते हुए कहा गया है कि चैतन्य आत्मा के इन्द्रियरूपी घोड़ों के (जिसके शब्द,रूप, रस, स्पर्श और गन्धादि में) प्रत्याहरण से उत्पन्न विकारों का समाप्त हो जाना ही प्रत्याहार है।" इन्द्रियों की वश्यता प्राण और मन की स्थिरता पर निर्भर है। हठयोग की साधना में स्पष्ट निर्देश है कि शरीर में प्राण की स्थिरता से ही मन स्थिर होता है। अतः प्राण-साधना इन्द्रियों के प्रत्याहार की दिशा में आवश्यक है। प्रत्याहार की सिद्धि से काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ और मोह इन छ: प्रकार के शत्रुओं का नाश हो जाता है। हठयोग साधना से ही सम्बन्धित एक अन्य ग्रन्थ 'घेरण्ड-संहिता' में कहा गया है कि जहाँ-जहाँ मनजाता है, उसे वहाँ-वहाँ से लौटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए, यही प्रत्याहार है।
__ हठयोग-साधना पर आधारित 'विवेक-मार्तण्ड' ग्रन्थ में भी प्रत्याहार के सम्बन्ध में कहा गया है कि रेचक-पूरक-कुम्भक, त्रयक्रमपूर्वक बारह बार प्राणायाम कर वायु को शरीर के भीतर स्थिर करने से मन स्थिर होता है और प्राणायाम के द्वारा इस तरह इन्द्रियों का प्रत्याहार हो जाता है। 'शिव-संहिता' में भी प्रत्याहार के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि जब साधक एक प्रहर तक वायु धारण की शक्ति प्राप्त करता है, तब प्रत्याहार होता है। जिस इन्द्रिय के द्वारा जिस विषय का बोध होता है, उसी में आत्मभाव करने से इन्द्रियजय होना ही प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार की सिद्धि ही धारणा, ध्यान और समाधि में आत्म-साक्षात्कार अथवा परमपद में स्वरूपावस्थान का सोपान है। 'गोरक्ष-संहिता' में भी प्रत्याहार के सम्बन्ध में इसी तथ्य को प्रतिपादित किया गया है। कहा गया है- चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियों के