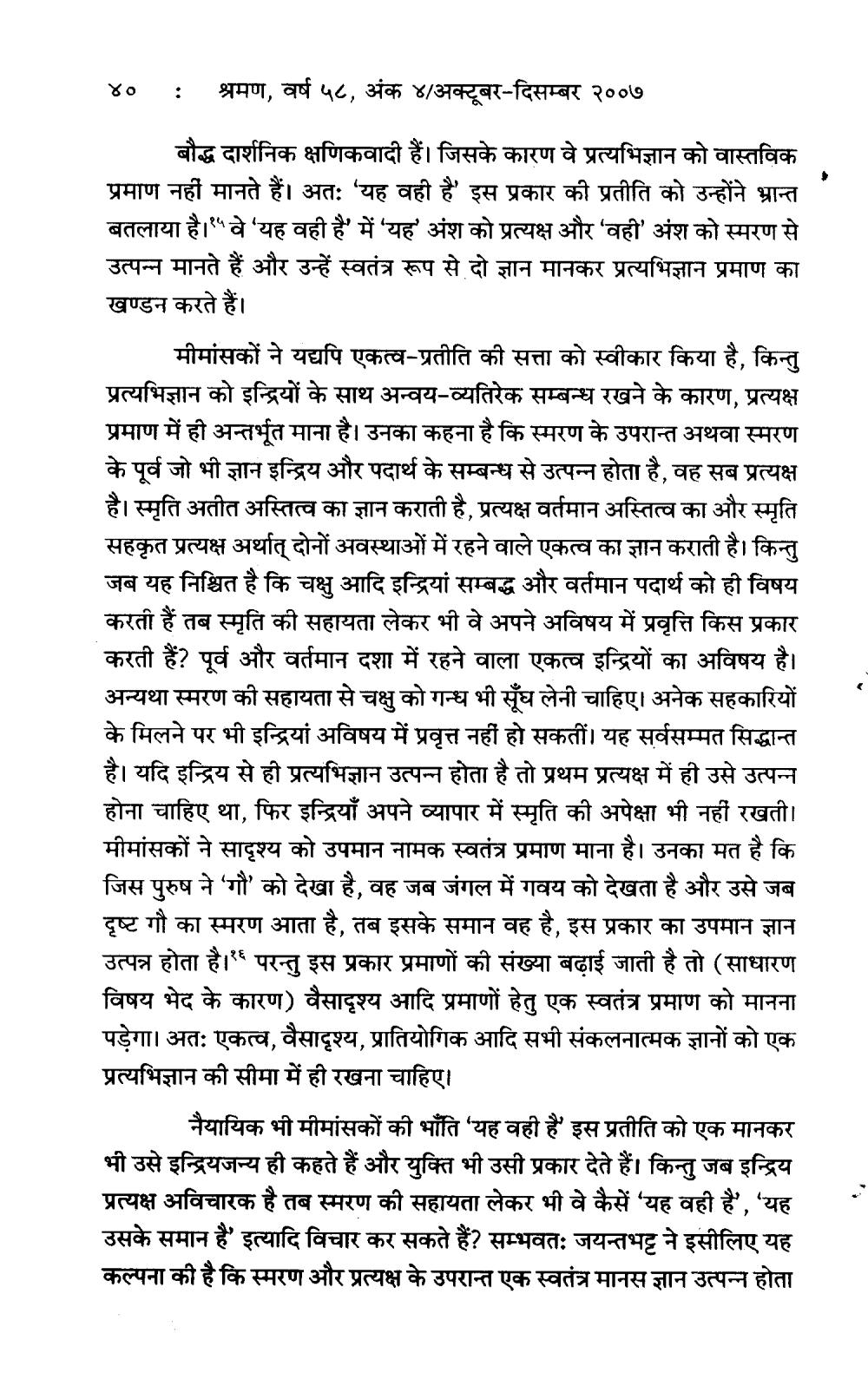________________
४०
:
श्रमण, वर्ष ५८, अंक ४/अक्टूबर-दिसम्बर २००७
बौद्ध दार्शनिक क्षणिकवादी हैं। जिसके कारण वे प्रत्यभिज्ञान को वास्तविक प्रमाण नहीं मानते हैं। अत: 'यह वही है। इस प्रकार की प्रतीति को उन्होंने भ्रान्त बतलाया है।५ वे 'यह वही है' में 'यह अंश को प्रत्यक्ष और 'वही' अंश को स्मरण से उत्पन्न मानते हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से दो ज्ञान मानकर प्रत्यभिज्ञान प्रमाण का खण्डन करते हैं।
मीमांसकों ने यद्यपि एकत्व-प्रतीति की सत्ता को स्वीकार किया है, किन्तु प्रत्यभिज्ञान को इन्द्रियों के साथ अन्वय-व्यतिरेक सम्बन्ध रखने के कारण, प्रत्यक्ष प्रमाण में ही अन्तर्भूत माना है। उनका कहना है कि स्मरण के उपरान्त अथवा स्मरण के पूर्व जो भी ज्ञान इन्द्रिय और पदार्थ के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है, वह सब प्रत्यक्ष है। स्मृति अतीत अस्तित्व का ज्ञान कराती है, प्रत्यक्ष वर्तमान अस्तित्व का और स्मृति सहकृत प्रत्यक्ष अर्थात् दोनों अवस्थाओं में रहने वाले एकत्व का ज्ञान कराती है। किन्तु जब यह निश्चित है कि चक्षु आदि इन्द्रियां सम्बद्ध और वर्तमान पदार्थ को ही विषय करती हैं तब स्मृति की सहायता लेकर भी वे अपने अविषय में प्रवृत्ति किस प्रकार करती हैं? पूर्व और वर्तमान दशा में रहने वाला एकत्व इन्द्रियों का अविषय है। अन्यथा स्मरण की सहायता से चक्षु को गन्ध भी सूंघ लेनी चाहिए। अनेक सहकारियों के मिलने पर भी इन्द्रियां अविषय में प्रवृत्त नहीं हो सकतीं। यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है। यदि इन्द्रिय से ही प्रत्यभिज्ञान उत्पन्न होता है तो प्रथम प्रत्यक्ष में ही उसे उत्पन्न होना चाहिए था, फिर इन्द्रियाँ अपने व्यापार में स्मृति की अपेक्षा भी नहीं रखती। मीमांसकों ने सादृश्य को उपमान नामक स्वतंत्र प्रमाण माना है। उनका मत है कि जिस पुरुष ने 'गौ' को देखा है, वह जब जंगल में गवय को देखता है और उसे जब दृष्ट गौ का स्मरण आता है, तब इसके समान वह है, इस प्रकार का उपमान ज्ञान उत्पन्न होता है। परन्तु इस प्रकार प्रमाणों की संख्या बढ़ाई जाती है तो (साधारण विषय भेद के कारण) वैसादृश्य आदि प्रमाणों हेतु एक स्वतंत्र प्रमाण को मानना पड़ेगा। अत: एकत्व, वैसादृश्य, प्रातियोगिक आदि सभी संकलनात्मक ज्ञानों को एक प्रत्यभिज्ञान की सीमा में ही रखना चाहिए।
नैयायिक भी मीमांसकों की भाँति 'यह वही हैं इस प्रतीति को एक मानकर भी उसे इन्द्रियजन्य ही कहते हैं और युक्ति भी उसी प्रकार देते हैं। किन्तु जब इन्द्रिय प्रत्यक्ष अविचारक है तब स्मरण की सहायता लेकर भी वे कैसें 'यह वही है', 'यह उसके समान है' इत्यादि विचार कर सकते हैं? सम्भवतः जयन्तभट्ट ने इसीलिए यह कल्पना की है कि स्मरण और प्रत्यक्ष के उपरान्त एक स्वतंत्र मानस ज्ञान उत्पन्न होता