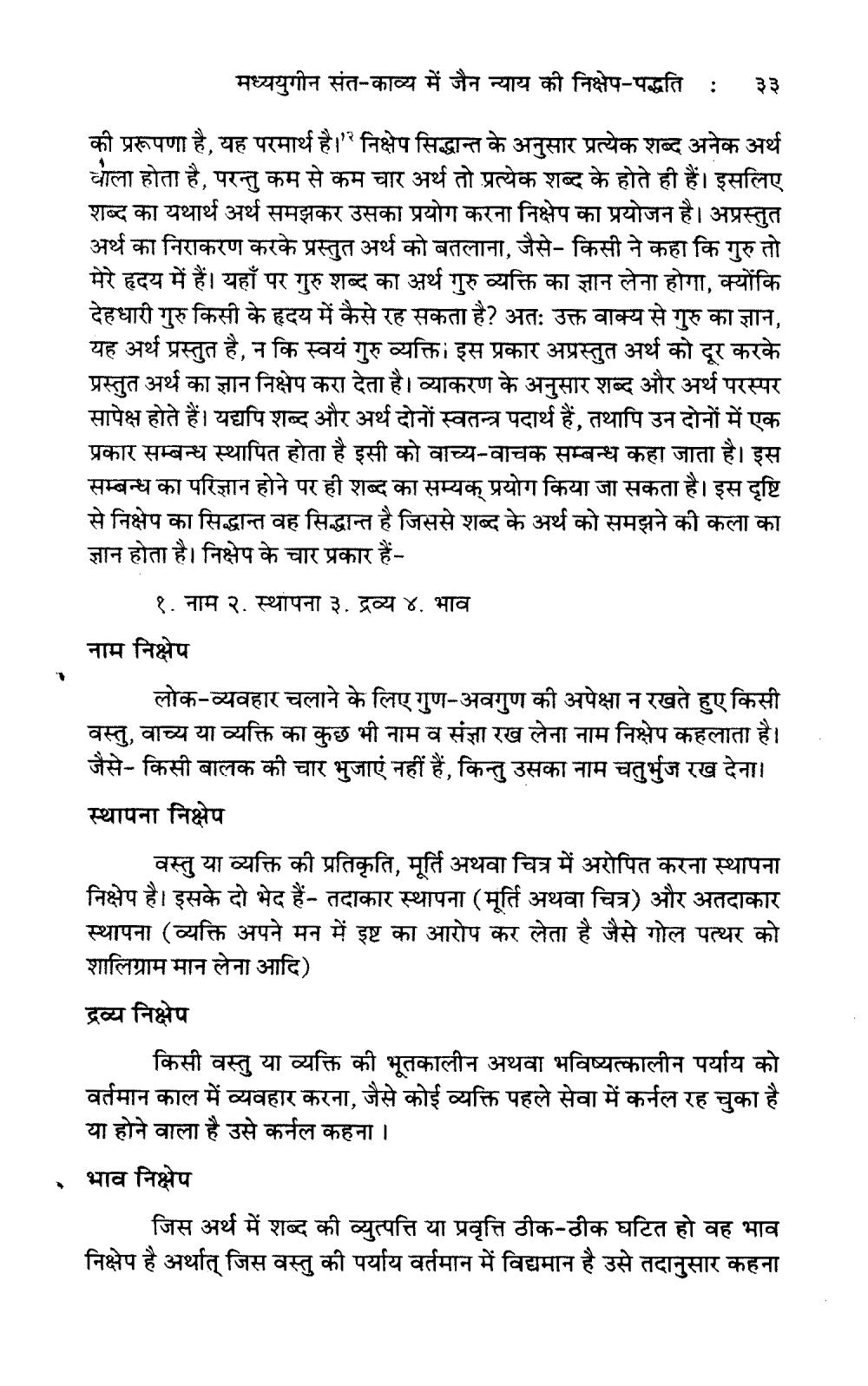________________
•
मध्ययुगीन संत-काव्य में जैन न्याय की निक्षेप-पद्धति
की प्ररूपणा है, यह परमार्थ है।" निक्षेप सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक शब्द अनेक अर्थ वाला होता है, परन्तु कम से कम चार अर्थ तो प्रत्येक शब्द के होते ही हैं। इसलिए शब्द का यथार्थ अर्थ समझकर उसका प्रयोग करना निक्षेप का प्रयोजन है। अप्रस्तुत अर्थ का निराकरण करके प्रस्तुत अर्थ को बतलाना, जैसे- किसी ने कहा कि गुरु तो मेरे हृदय में हैं। यहाँ पर गुरु शब्द का अर्थ गुरु व्यक्ति का ज्ञान लेना होगा, क्योंकि देहधारी गुरु किसी के हृदय में कैसे रह सकता है? अतः उक्त वाक्य से गुरु का ज्ञान, यह अर्थ प्रस्तुत है, न कि स्वयं गुरु व्यक्ति इस प्रकार अप्रस्तुत अर्थ को दूर करके प्रस्तुत अर्थ का ज्ञान निक्षेप करा देता है। व्याकरण के अनुसार शब्द और अर्थ परस्पर सापेक्ष होते हैं। यद्यपि शब्द और अर्थ दोनों स्वतन्त्र पदार्थ हैं, तथापि उन दोनों में एक प्रकार सम्बन्ध स्थापित होता है इसी को वाच्य वाचक सम्बन्ध कहा जाता है। इस सम्बन्ध का परिज्ञान होने पर ही शब्द का सम्यक् प्रयोग किया जा सकता है । इस दृष्टि से निक्षेप का सिद्धान्त वह सिद्धान्त है जिससे शब्द के अर्थ को समझने की कला का ज्ञान होता है। निक्षेप के चार प्रकार हैं
१. नाम २. स्थापना ३. द्रव्य ४. भाव
नाम निक्षेप
: ३३
लोक-व्यवहार चलाने के लिए गुण-अवगुण की अपेक्षा न रखते हुए किसी वस्तु, वाच्य या व्यक्ति का कुछ भी नाम व संज्ञा रख लेना नाम निक्षेप कहलाता है। जैसे- किसी बालक की चार भुजाएं नहीं हैं, किन्तु उसका नाम चतुर्भुज रख देना। स्थापना निक्षेप
वस्तु या व्यक्ति की प्रतिकृति, मूर्ति अथवा चित्र में अरोपित करना स्थापना निक्षेप है। इसके दो भेद हैं- तदाकार स्थापना (मूर्ति अथवा चित्र) और अतदाकार स्थापना (व्यक्ति अपने मन में इष्ट का आरोप कर लेता है जैसे गोल पत्थर को शालिग्राम मान लेना आदि)
द्रव्य निक्षेप
किसी वस्तु या व्यक्ति की भूतकालीन अथवा भविष्यत्कालीन पर्याय को वर्तमान काल में व्यवहार करना, जैसे कोई व्यक्ति पहले सेवा में कर्नल रह चुका है या होने वाला है उसे कर्नल कहना ।
भाव निक्षेप
जिस अर्थ में शब्द की व्युत्पत्ति या प्रवृत्ति ठीक-ठीक घटित हो वह भाव निक्षेप है अर्थात् जिस वस्तु की पर्याय वर्तमान में विद्यमान है उसे तदानुसार कहना