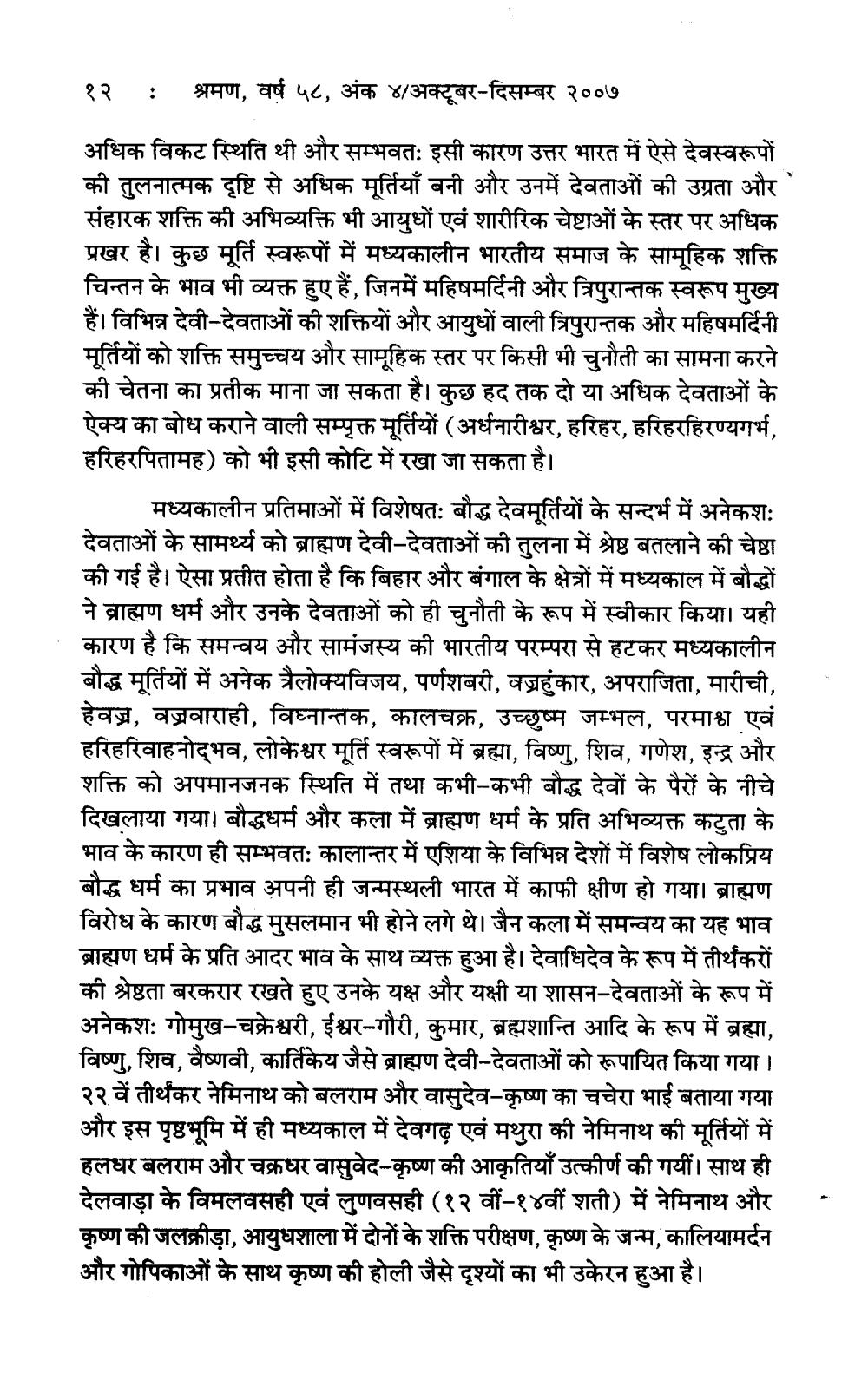________________
१२ :
श्रमण, वर्ष ५८, अंक ४/अक्टूबर-दिसम्बर २००७
अधिक विकट स्थिति थी और सम्भवत: इसी कारण उत्तर भारत में ऐसे देवस्वरूपों की तुलनात्मक दृष्टि से अधिक मूर्तियाँ बनी और उनमें देवताओं की उग्रता और संहारक शक्ति की अभिव्यक्ति भी आयुधों एवं शारीरिक चेष्टाओं के स्तर पर अधिक प्रखर है। कुछ मूर्ति स्वरूपों में मध्यकालीन भारतीय समाज के सामूहिक शक्ति चिन्तन के भाव भी व्यक्त हुए हैं, जिनमें महिषमर्दिनी और त्रिपुरान्तक स्वरूप मुख्य हैं। विभिन्न देवी-देवताओं की शक्तियों और आयुधों वाली त्रिपुरान्तक और महिषमर्दिनी मूर्तियों को शक्ति समुच्चय और सामूहिक स्तर पर किसी भी चुनौती का सामना करने की चेतना का प्रतीक माना जा सकता है। कुछ हद तक दो या अधिक देवताओं के ऐक्य का बोध कराने वाली सम्पृक्त मूर्तियों (अर्धनारीश्वर, हरिहर, हरिहरहिरण्यगर्भ, हरिहरपितामह) को भी इसी कोटि में रखा जा सकता है।
मध्यकालीन प्रतिमाओं में विशेषत: बौद्ध देवमूर्तियों के सन्दर्भ में अनेकशः देवताओं के सामर्थ्य को ब्राह्मण देवी-देवताओं की तुलना में श्रेष्ठ बतलाने की चेष्ठा की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में मध्यकाल में बौद्धों ने ब्राह्मण धर्म और उनके देवताओं को ही चुनौती के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि समन्वय और सामंजस्य की भारतीय परम्परा से हटकर मध्यकालीन बौद्ध मूर्तियों में अनेक त्रैलोक्यविजय, पर्णशबरी, वज्रहुंकार, अपराजिता, मारीची, हेवज्र, वज्रवाराही, विघ्नान्तक, कालचक्र, उच्छुष्म जम्भल, परमाश्वा एवं हरिहरिवाहनोद्भव, लोकेश्वर मूर्ति स्वरूपों में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, इन्द्र और शक्ति को अपमानजनक स्थिति में तथा कभी-कभी बौद्ध देवों के पैरों के नीचे दिखलाया गया। बौद्धधर्म और कला में ब्राह्मण धर्म के प्रति अभिव्यक्त कटुता के भाव के कारण ही सम्भवत: कालान्तर में एशिया के विभिन्न देशों में विशेष लोकप्रिय बौद्ध धर्म का प्रभाव अपनी ही जन्मस्थली भारत में काफी क्षीण हो गया। ब्राह्मण विरोध के कारण बौद्ध मुसलमान भी होने लगे थे। जैन कला में समन्वय का यह भाव ब्राह्मण धर्म के प्रति आदर भाव के साथ व्यक्त हुआ है। देवाधिदेव के रूप में तीर्थंकरों की श्रेष्ठता बरकरार रखते हुए उनके यक्ष और यक्षी या शासन-देवताओं के रूप में अनेकश: गोमुख-चक्रेश्वरी, ईश्वर-गौरी, कुमार, ब्रह्मशान्ति आदि के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, वैष्णवी, कार्तिकेय जैसे ब्राह्मण देवी-देवताओं को रूपायित किया गया। २२ वें तीर्थंकर नेमिनाथ को बलराम और वासुदेव-कृष्ण का चचेरा भाई बताया गया और इस पृष्ठभूमि में ही मध्यकाल में देवगढ़ एवं मथुरा की नेमिनाथ की मूर्तियों में हलधर बलराम और चक्रधर वासुवेद-कृष्ण की आकृतियाँ उत्कीर्ण की गयीं। साथ ही देलवाड़ा के विमलवसही एवं लुणवसही (१२ वीं-१४वीं शती) में नेमिनाथ और कृष्ण की जलक्रीड़ा, आयुधशाला में दोनों के शक्ति परीक्षण, कृष्ण के जन्म, कालियामर्दन और गोपिकाओं के साथ कृष्ण की होली जैसे दृश्यों का भी उकेरन हुआ है।