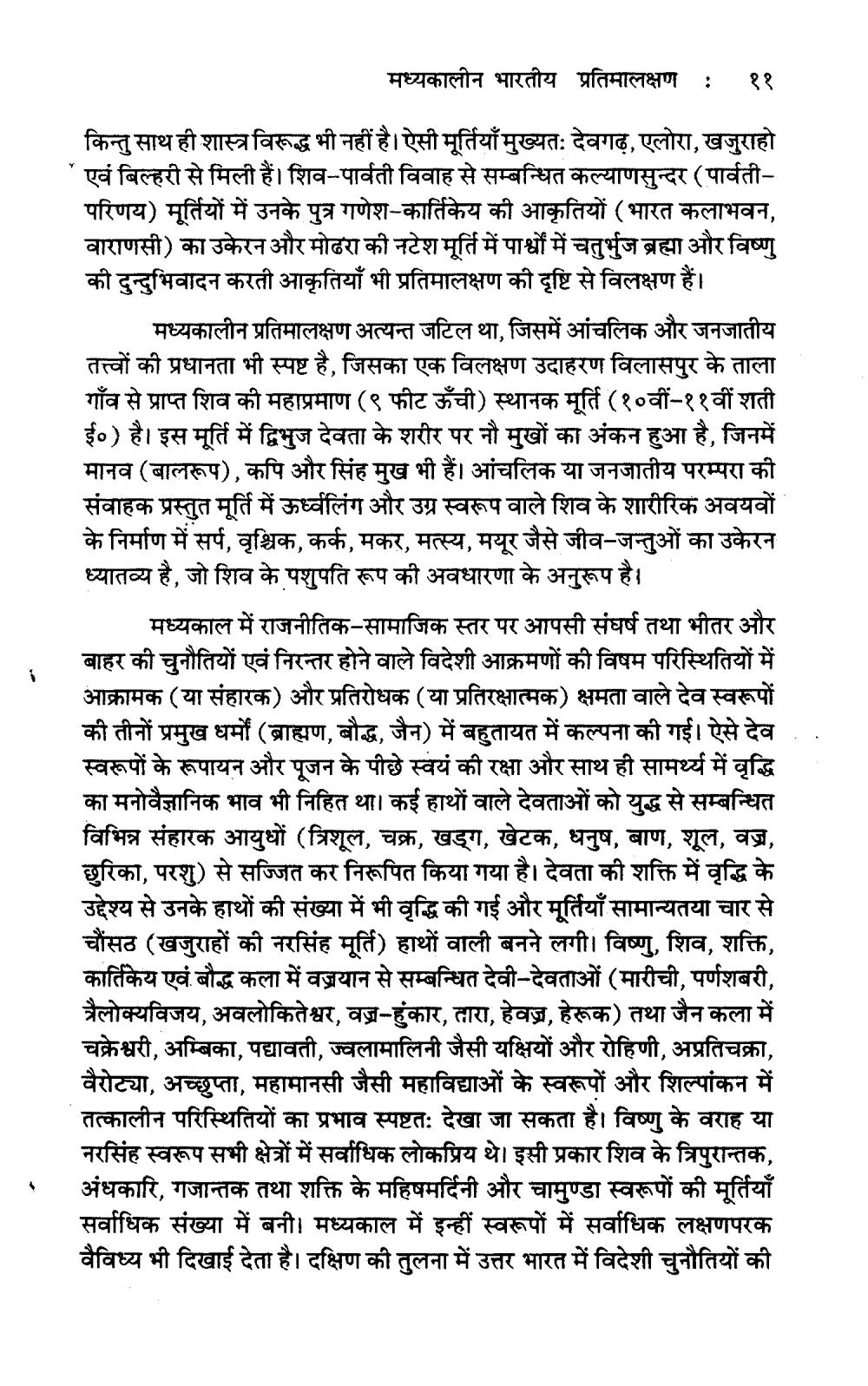________________
i
मध्यकालीन भारतीय प्रतिमालक्षण : ११
किन्तु साथ ही शास्त्र विरूद्ध भी नहीं है। ऐसी मूर्तियाँ मुख्यतः देवगढ़, एलोरा, खजुराहो एवं बिल्हरी से मिली हैं। शिव-पार्वती विवाह से सम्बन्धित कल्याणसुन्दर (पार्वतीपरिणय) मूर्तियों में उनके पुत्र गणेश - कार्तिकेय की आकृतियों (भारत कलाभवन, वाराणसी) का उकेरन और मोढरा की नटेश मूर्ति में पार्श्वों में चतुर्भुज ब्रह्मा और विष्णु की दुन्दुभिवादन करती आकृतियाँ भी प्रतिमालक्षण की दृष्टि से विलक्षण हैं।
मध्यकालीन प्रतिमालक्षण अत्यन्त जटिल था, जिसमें आंचलिक और जनजातीय तत्त्वों की प्रधानता भी स्पष्ट है, जिसका एक विलक्षण उदाहरण विलासपुर के ताला गाँव से प्राप्त शिव की महाप्रमाण (९ फीट ऊँची) स्थानक मूर्ति (१०वीं - ११वीं शती ई०) है। इस मूर्ति में द्विभुज देवता के शरीर पर नौ मुखों का अंकन हुआ है, जिनमें मानव (बालरूप), कपि और सिंह मुख भी हैं। आंचलिक या जनजातीय परम्परा की संवाहक प्रस्तुत मूर्ति में ऊर्ध्वलिंग और उग्र स्वरूप वाले शिव के शारीरिक अवयवों के निर्माण में सर्प, वृश्चिक, कर्क, मकर, मत्स्य, मयूर जैसे जीव-जन्तुओं का उकेरन ध्यातव्य है, जो शिव के पशुपति रूप की अवधारणा के अनुरूप है।
मध्यकाल में राजनीतिक-सामाजिक स्तर पर आपसी संघर्ष तथा भीतर और बाहर की चुनौतियों एवं निरन्तर होने वाले विदेशी आक्रमणों की विषम परिस्थितियों में आक्रामक (या संहारक) और प्रतिरोधक (या प्रतिरक्षात्मक) क्षमता वाले देव स्वरूपों की तीनों प्रमुख धर्मों (ब्राह्मण, बौद्ध, जैन) में बहुतायत में कल्पना की गई। ऐसे देव स्वरूपों के रूपायन और पूजन के पीछे स्वयं की रक्षा और साथ ही सामर्थ्य में वृद्धि का मनोवैज्ञानिक भाव भी निहित था । कई हाथों वाले देवताओं को युद्ध से सम्बन्धित विभिन्न संहारक आयुधों (त्रिशूल, चक्र, खड्ग, खेटक, धनुष, बाण, शूल, वज्र, छुरिका, परशु) से सज्जित कर निरूपित किया गया है। देवता की शक्ति में वृद्धि के उद्देश्य से उनके हाथों की संख्या में भी वृद्धि की गई और मूर्तियाँ सामान्यतया चार से चौंसठ (खजुराहों की नरसिंह मूर्ति) हाथों वाली बनने लगी। विष्णु, शिव, शक्ति, कार्तिकेय एवं बौद्ध कला में वज्रयान से सम्बन्धित देवी-देवताओं (मारीची, पर्णशबरी, त्रैलोक्यविजय, अवलोकितेश्वर, वज्र- हुंकार, तारा, हेवज्र, हेरूक) तथा जैन कला में चक्रेश्वरी, अम्बिका, पद्यावती, ज्वलामालिनी जैसी यक्षियों और रोहिणी, अप्रतिचक्रा, वैरोट्या, अच्छुप्ता, महामानसी जैसी महाविद्याओं के स्वरूपों और शिल्पांकन में तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्टतः देखा जा सकता है। विष्णु के वराह या नरसिंह स्वरूप सभी क्षेत्रों में सर्वाधिक लोकप्रिय थे। इसी प्रकार शिव के त्रिपुरान्तक, अंधकार, गजान्तक तथा शक्ति के महिषमर्दिनी और चामुण्डा स्वरूपों की मूर्तियाँ सर्वाधिक संख्या में बनी। मध्यकाल में इन्हीं स्वरूपों में सर्वाधिक लक्षणपरक वैविध्य भी दिखाई देता है। दक्षिण की तुलना में उत्तर भारत में विदेशी चुनौतियों की