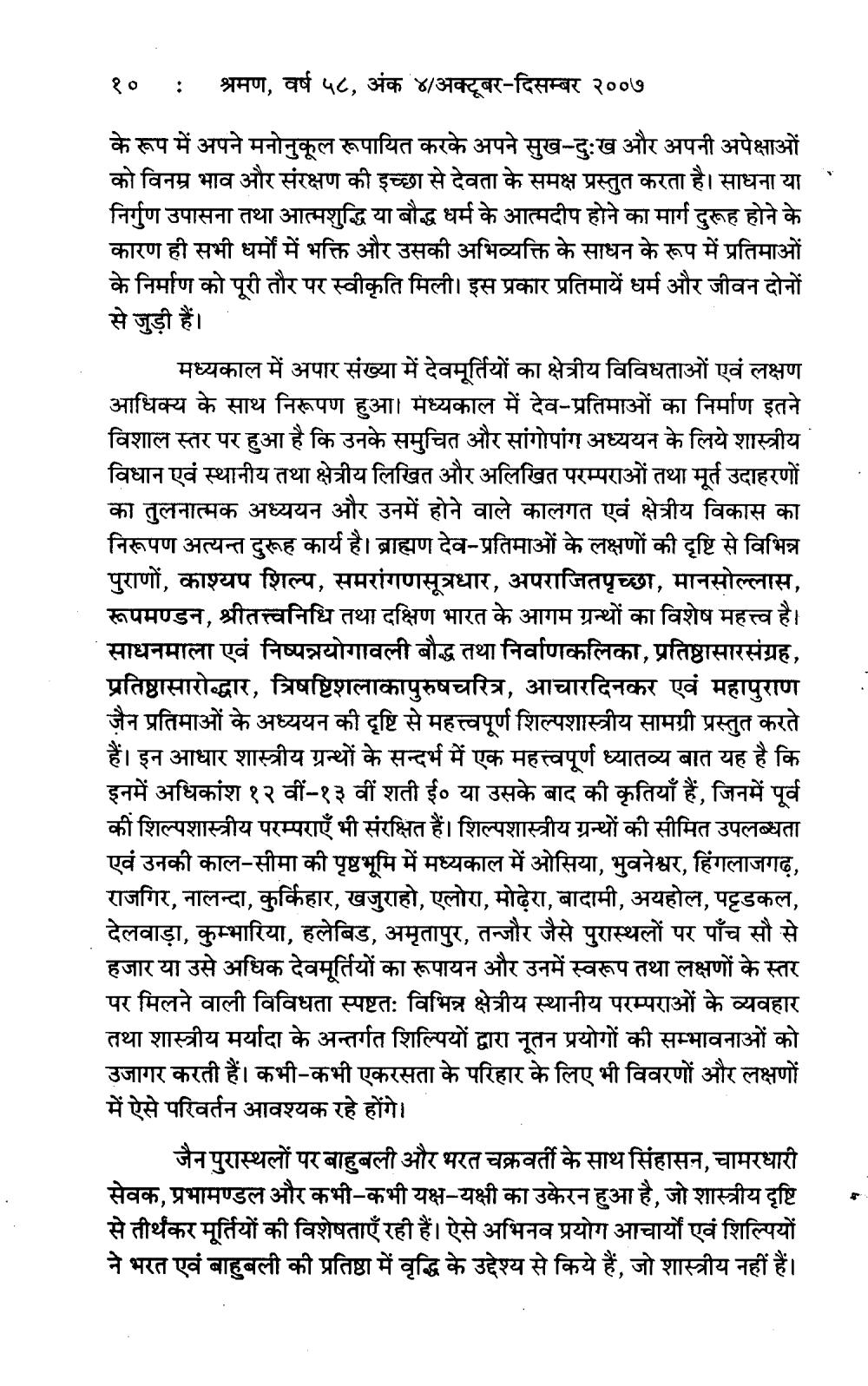________________
१० :
श्रमण, वर्ष ५८, अंक ४/अक्टूबर-दिसम्बर २००७
के रूप में अपने मनोनुकूल रूपायित करके अपने सुख-दुःख और अपनी अपेक्षाओं को विनम्र भाव और संरक्षण की इच्छा से देवता के समक्ष प्रस्तुत करता है। साधना या । निर्गुण उपासना तथा आत्मशुद्धि या बौद्ध धर्म के आत्मदीप होने का मार्ग दुरूह होने के कारण ही सभी धर्मों में भक्ति और उसकी अभिव्यक्ति के साधन के रूप में प्रतिमाओं के निर्माण को पूरी तौर पर स्वीकृति मिली। इस प्रकार प्रतिमायें धर्म और जीवन दोनों से जुड़ी हैं।
मध्यकाल में अपार संख्या में देवमूर्तियों का क्षेत्रीय विविधताओं एवं लक्षण आधिक्य के साथ निरूपण हुआ। मध्यकाल में देव-प्रतिमाओं का निर्माण इतने विशाल स्तर पर हुआ है कि उनके समुचित और सांगोपांग अध्ययन के लिये शास्त्रीय विधान एवं स्थानीय तथा क्षेत्रीय लिखित और अलिखित परम्पराओं तथा मूर्त उदाहरणों का तुलनात्मक अध्ययन और उनमें होने वाले कालगत एवं क्षेत्रीय विकास का निरूपण अत्यन्त दुरूह कार्य है। ब्राह्मण देव-प्रतिमाओं के लक्षणों की दृष्टि से विभिन्न पुराणों, काश्यप शिल्प, समरांगणसूत्रधार, अपराजितपृच्छा, मानसोल्लास, रूपमण्डन, श्रीतत्त्वनिधि तथा दक्षिण भारत के आगम ग्रन्थों का विशेष महत्त्व है। साधनमाला एवं निष्पन्नयोगावली बौद्ध तथा निर्वाणकलिका, प्रतिष्ठासारसंग्रह, प्रतिष्ठासारोद्धार, त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, आचारदिनकर एवं महापुराण जैन प्रतिमाओं के अध्ययन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण शिल्पशास्त्रीय सामग्री प्रस्तुत करते हैं। इन आधार शास्त्रीय ग्रन्थों के सन्दर्भ में एक महत्त्वपूर्ण ध्यातव्य बात यह है कि इनमें अधिकांश १२ वीं-१३ वीं शती ई० या उसके बाद की कृतियाँ हैं, जिनमें पूर्व की शिल्पशास्त्रीय परम्पराएँ भी संरक्षित हैं। शिल्पशास्त्रीय ग्रन्थों की सीमित उपलब्धता एवं उनकी काल-सीमा की पृष्ठभूमि में मध्यकाल में ओसिया, भुवनेश्वर, हिंगलाजगढ़, राजगिर, नालन्दा, कुर्किहार, खजुराहो, एलोरा, मोढेरा, बादामी, अयहोल, पट्टडकल, देलवाड़ा, कुम्भारिया, हलेबिड, अमृतापुर, तन्जौर जैसे पुरास्थलों पर पाँच सौ से हजार या उसे अधिक देवमूर्तियों का रूपायन और उनमें स्वरूप तथा लक्षणों के स्तर पर मिलने वाली विविधता स्पष्टत: विभिन्न क्षेत्रीय स्थानीय परम्पराओं के व्यवहार तथा शास्त्रीय मर्यादा के अन्तर्गत शिल्पियों द्वारा नूतन प्रयोगों की सम्भावनाओं को उजागर करती हैं। कभी-कभी एकरसता के परिहार के लिए भी विवरणों और लक्षणों में ऐसे परिवर्तन आवश्यक रहे होंगे।
जैन पुरास्थलों पर बाहुबली और भरत चक्रवर्ती के साथ सिंहासन, चामरधारी सेवक, प्रभामण्डल और कभी-कभी यक्ष-यक्षी का उकेरन हुआ है, जो शास्त्रीय दृष्टि से तीर्थंकर मूर्तियों की विशेषताएँ रही हैं। ऐसे अभिनव प्रयोग आचार्यों एवं शिल्पियों ने भरत एवं बाहुबली की प्रतिष्ठा में वृद्धि के उद्देश्य से किये हैं, जो शास्त्रीय नहीं हैं।