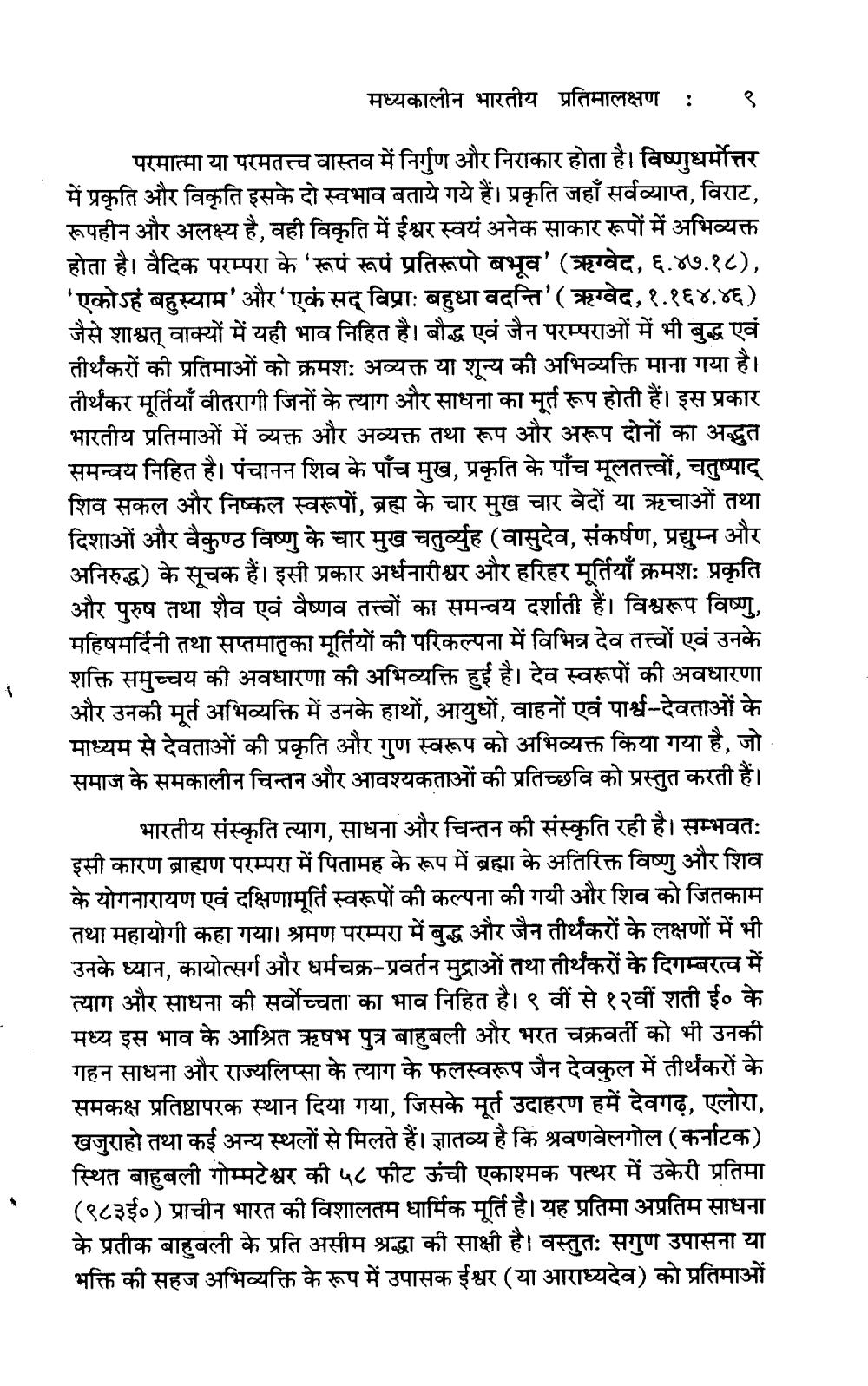________________
मध्यकालीन भारतीय प्रतिमालक्षण :
९
परमात्मा या परमतत्त्व वास्तव में निर्गुण और निराकार होता है। विष्णुधर्मोत्तर में प्रकृति और विकृति इसके दो स्वभाव बताये गये हैं। प्रकृति जहाँ सर्वव्याप्त, विराट, रूपहीन और अलक्ष्य है, वही विकृति में ईश्वर स्वयं अनेक साकार रूपों में अभिव्यक्त होता है। वैदिक परम्परा के 'रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव' (ऋग्वेद, ६.४७.१८), 'एकोऽहं बहुस्याम' और 'एकंसद् विप्राः बहुधा वदन्ति' (ऋग्वेद,१.१६४.४६) जैसे शाश्वत् वाक्यों में यही भाव निहित है। बौद्ध एवं जैन परम्पराओं में भी बुद्ध एवं तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को क्रमश: अव्यक्त या शून्य की अभिव्यक्ति माना गया है। तीर्थंकर मूर्तियाँ वीतरागी जिनों के त्याग और साधना का मूर्त रूप होती हैं। इस प्रकार भारतीय प्रतिमाओं में व्यक्त और अव्यक्त तथा रूप और अरूप दोनों का अद्भुत समन्वय निहित है। पंचानन शिव के पाँच मुख, प्रकृति के पाँच मूलतत्त्वों, चतुष्पाद् शिव सकल और निष्कल स्वरूपों, ब्रह्म के चार मुख चार वेदों या ऋचाओं तथा दिशाओं और वैकुण्ठ विष्णु के चार मुख चतुर्युह (वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध) के सूचक हैं। इसी प्रकार अर्धनारीश्वर और हरिहर मूर्तियाँ क्रमशः प्रकृति और पुरुष तथा शैव एवं वैष्णव तत्त्वों का समन्वय दर्शाती हैं। विश्वरूप विष्णु, महिषमर्दिनी तथा सप्तमातृका मूर्तियों की परिकल्पना में विभिन्न देव तत्त्वों एवं उनके शक्ति समुच्चय की अवधारणा की अभिव्यक्ति हुई है। देव स्वरूपों की अवधारणा
और उनकी मूर्त अभिव्यक्ति में उनके हाथों, आयुधों, वाहनों एवं पार्श्व-देवताओं के माध्यम से देवताओं की प्रकृति और गुण स्वरूप को अभिव्यक्त किया गया है, जो समाज के समकालीन चिन्तन और आवश्यकताओं की प्रतिच्छवि को प्रस्तुत करती हैं।
भारतीय संस्कृति त्याग, साधना और चिन्तन की संस्कृति रही है। सम्भवतः इसी कारण ब्राह्मण परम्परा में पितामह के रूप में ब्रह्मा के अतिरिक्त विष्णु और शिव के योगनारायण एवं दक्षिणामूर्ति स्वरूपों की कल्पना की गयी और शिव को जितकाम तथा महायोगी कहा गया। श्रमण परम्परा में बुद्ध और जैन तीर्थंकरों के लक्षणों में भी उनके ध्यान, कायोत्सर्ग और धर्मचक्र-प्रवर्तन मुद्राओं तथा तीर्थंकरों के दिगम्बरत्व में त्याग और साधना की सर्वोच्चता का भाव निहित है। ९ वीं से १२वीं शती ई० के मध्य इस भाव के आश्रित ऋषभ पुत्र बाहुबली और भरत चक्रवर्ती को भी उनकी गहन साधना और राज्यलिप्सा के त्याग के फलस्वरूप जैन देवकुल में तीर्थंकरों के समकक्ष प्रतिष्ठापरक स्थान दिया गया, जिसके मूर्त उदाहरण हमें देवगढ़, एलोरा, खजुराहो तथा कई अन्य स्थलों से मिलते हैं। ज्ञातव्य है कि श्रवणवेलगोल (कर्नाटक) स्थित बाहुबली गोम्मटेश्वर की ५८ फीट ऊंची एकाश्मक पत्थर में उकेरी प्रतिमा (९८३ई०) प्राचीन भारत की विशालतम धार्मिक मूर्ति है। यह प्रतिमा अप्रतिम साधना के प्रतीक बाहुबली के प्रति असीम श्रद्धा की साक्षी है। वस्तुत: सगुण उपासना या भक्ति की सहज अभिव्यक्ति के रूप में उपासक ईश्वर (या आराध्यदेव) को प्रतिमाओं