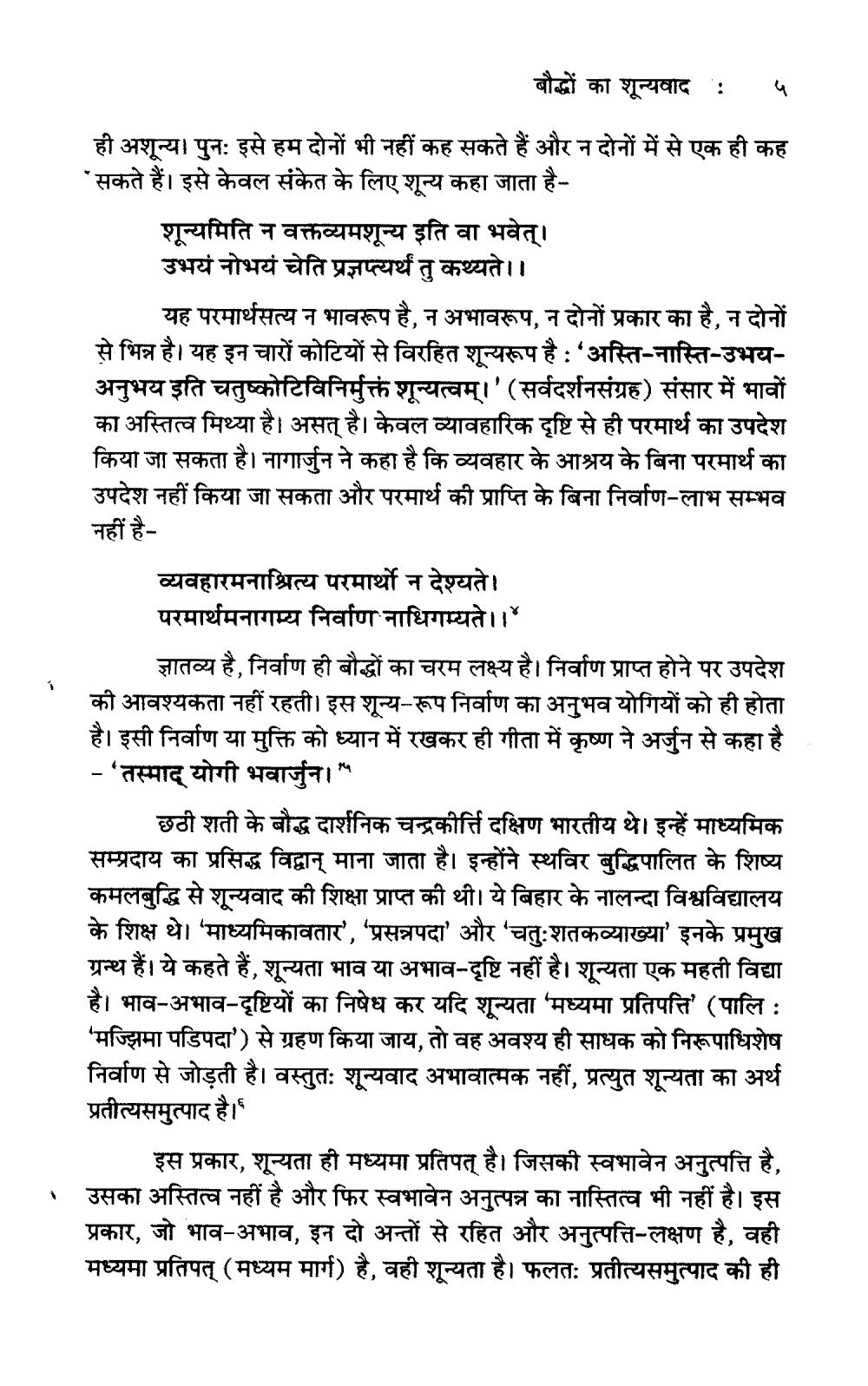________________
बौद्धों का शून्यवाद :
५
ही अशून्य। पुन: इसे हम दोनों भी नहीं कह सकते हैं और न दोनों में से एक ही कह "सकते हैं। इसे केवल संकेत के लिए शून्य कहा जाता है
शून्यमिति न वक्तव्यमशून्य इति वा भवेत्। उभय नोभयं चेति प्रज्ञप्त्यर्थं तु कथ्यते।।
यह परमार्थसत्य न भावरूप है, न अभावरूप, न दोनों प्रकार का है, न दोनों से भिन्न है। यह इन चारों कोटियों से विरहित शून्यरूप है : 'अस्ति-नास्ति-उभयअनुभय इति चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं शून्यत्वम्।' (सर्वदर्शनसंग्रह) संसार में भावों का अस्तित्व मिथ्या है। असत् है। केवल व्यावहारिक दृष्टि से ही परमार्थ का उपदेश किया जा सकता है। नागार्जुन ने कहा है कि व्यवहार के आश्रय के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं किया जा सकता और परमार्थ की प्राप्ति के बिना निर्वाण-लाभ सम्भव नहीं है
व्यवहारमनाश्रित्य परमार्थो न देश्यते। परमार्थमनागम्य निर्वाण नाधिगम्यते।।
ज्ञातव्य है, निर्वाण ही बौद्धों का चरम लक्ष्य है। निर्वाण प्राप्त होने पर उपदेश की आवश्यकता नहीं रहती। इस शून्य-रूप निर्वाण का अनुभव योगियों को ही होता है। इसी निर्वाण या मुक्ति को ध्यान में रखकर ही गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा है - 'तस्माद् योगी भवार्जुन।
छठी शती के बौद्ध दार्शनिक चन्द्रकीर्ति दक्षिण भारतीय थे। इन्हें माध्यमिक सम्प्रदाय का प्रसिद्ध विद्वान् माना जाता है। इन्होंने स्थविर बुद्धिपालित के शिष्य कमलबुद्धि से शून्यवाद की शिक्षा प्राप्त की थी। ये बिहार के नालन्दा विश्वविद्यालय के शिक्ष थे। 'माध्यमिकावतार', 'प्रसन्नपदा' और 'चतु:शतकव्याख्या' इनके प्रमुख ग्रन्थ हैं। ये कहते हैं, शून्यता भाव या अभाव-दृष्टि नहीं है। शून्यता एक महती विद्या है। भाव-अभाव-दृष्टियों का निषेध कर यदि शून्यता 'मध्यमा प्रतिपत्ति' (पालि : 'मज्झिमा पडिपदा') से ग्रहण किया जाय, तो वह अवश्य ही साधक को निरूपाधिशेष निर्वाण से जोड़ती है। वस्तुत: शून्यवाद अभावात्मक नहीं, प्रत्युत शून्यता का अर्थ प्रतीत्यसमुत्पाद है।
इस प्रकार, शून्यता ही मध्यमा प्रतिपत् है। जिसकी स्वभावेन अनुत्पत्ति है, । उसका अस्तित्व नहीं है और फिर स्वभावेन अनुत्पन्न का नास्तित्व भी नहीं है। इस
प्रकार, जो भाव-अभाव, इन दो अन्तों से रहित और अनुत्पत्ति-लक्षण है, वही मध्यमा प्रतिपत् (मध्यम मार्ग) है, वही शून्यता है। फलत: प्रतीत्यसमुत्पाद की ही