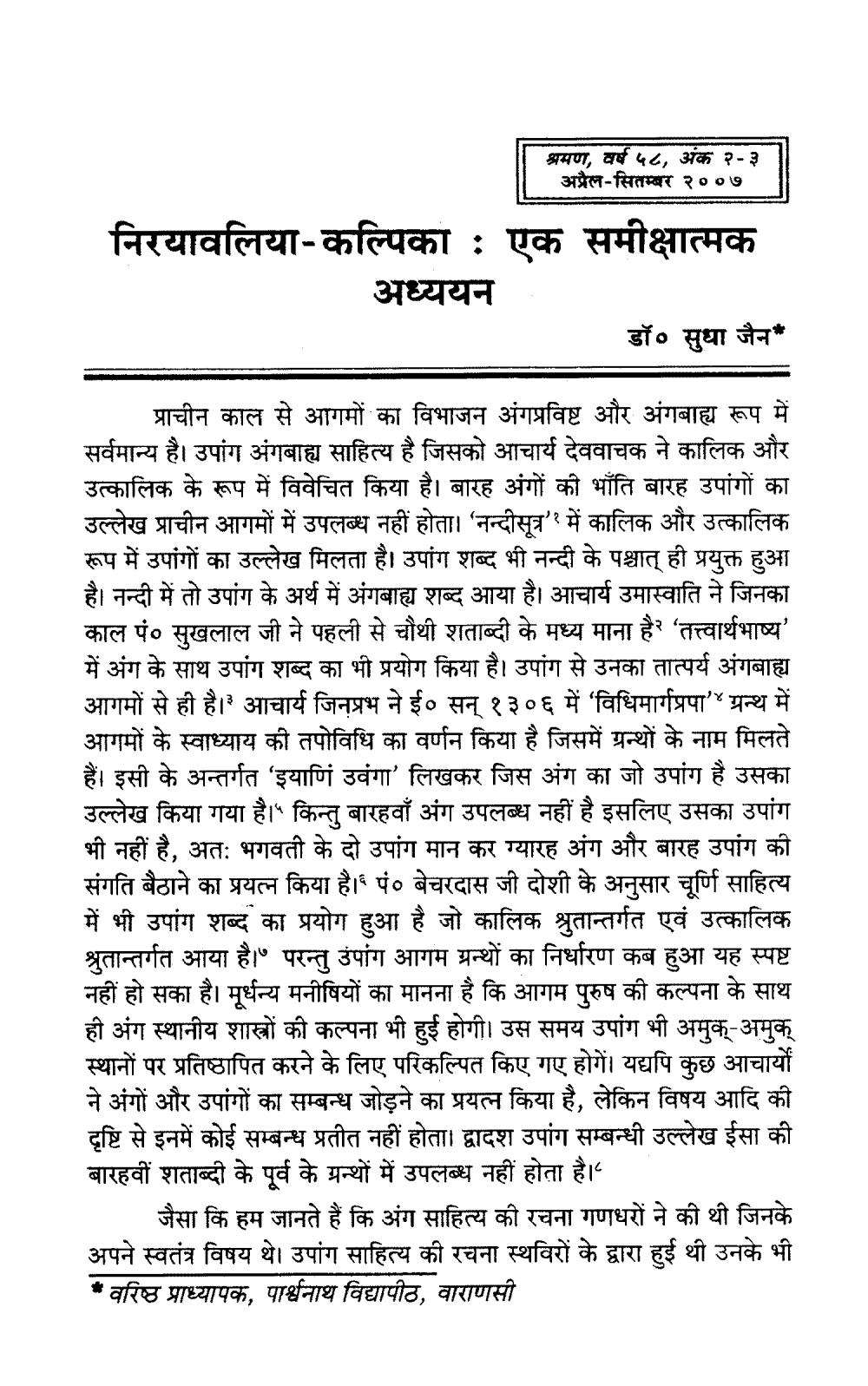________________
श्रमण, वर्ष ५८, अंक २-३ अप्रैल-सितम्बर २००७
निरयावलिया-कल्पिका : एक समीक्षात्मक अध्ययन
डॉ० सुधा जैन*
प्राचीन काल से आगमों का विभाजन अंगप्रविष्ट और अंगबाह्य रूप में सर्वमान्य है। उपांग अंगबाह्य साहित्य है जिसको आचार्य देववाचक ने कालिक और उत्कालिक के रूप में विवेचित किया है। बारह अंगों की भाँति बारह उपांगों का उल्लेख प्राचीन आगमों में उपलब्ध नहीं होता। 'नन्दीसूत्र' में कालिक और उत्कालिक रूप में उपांगों का उल्लेख मिलता है। उपांग शब्द भी नन्दी के पश्चात् ही प्रयुक्त हुआ है। नन्दी में तो उपांग के अर्थ में अंगबाह्य शब्द आया है। आचार्य उमास्वाति ने जिनका काल पं० सुखलाल जी ने पहली से चौथी शताब्दी के मध्य माना है। 'तत्त्वार्थभाष्य' में अंग के साथ उपांग शब्द का भी प्रयोग किया है। उपांग से उनका तात्पर्य अंगबाह्य आगमों से ही है। आचार्य जिनप्रभ ने ई० सन् १३०६ में 'विधिमार्गप्रपा' ग्रन्थ में आगमों के स्वाध्याय की तपोविधि का वर्णन किया है जिसमें ग्रन्थों के नाम मिलते हैं। इसी के अन्तर्गत 'इयाणिं उवंगा' लिखकर जिस अंग का जो उपांग है उसका उल्लेख किया गया है। किन्तु बारहवाँ अंग उपलब्ध नहीं है इसलिए उसका उपांग भी नहीं है, अत: भगवती के दो उपांग मान कर ग्यारह अंग और बारह उपांग की संगति बैठाने का प्रयत्न किया है। पं० बेचरदास जी दोशी के अनुसार चूर्णि साहित्य में भी उपांग शब्द का प्रयोग हुआ है जो कालिक श्रुतान्तर्गत एवं उत्कालिक श्रुतान्तर्गत आया है। परन्तु उपांग आगम ग्रन्थों का निर्धारण कब हुआ यह स्पष्ट नहीं हो सका है। मूर्धन्य मनीषियों का मानना है कि आगम पुरुष की कल्पना के साथ ही अंग स्थानीय शास्त्रों की कल्पना भी हुई होगी। उस समय उपांग भी अमुक-अमुक् स्थानों पर प्रतिष्ठापित करने के लिए परिकल्पित किए गए होगें। यद्यपि कछ आचार्यों ने अंगों और उपांगों का सम्बन्ध जोड़ने का प्रयत्न किया है, लेकिन विषय आदि की दृष्टि से इनमें कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता। द्वादश उपांग सम्बन्धी उल्लेख ईसा की बारहवीं शताब्दी के पूर्व के ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता है।
जैसा कि हम जानते हैं कि अंग साहित्य की रचना गणधरों ने की थी जिनके अपने स्वतंत्र विषय थे। उपांग साहित्य की रचना स्थविरों के द्वारा हुई थी उनके भी * वरिष्ठ प्राध्यापक, पार्श्वनाथ विद्यापीठ, वाराणसी