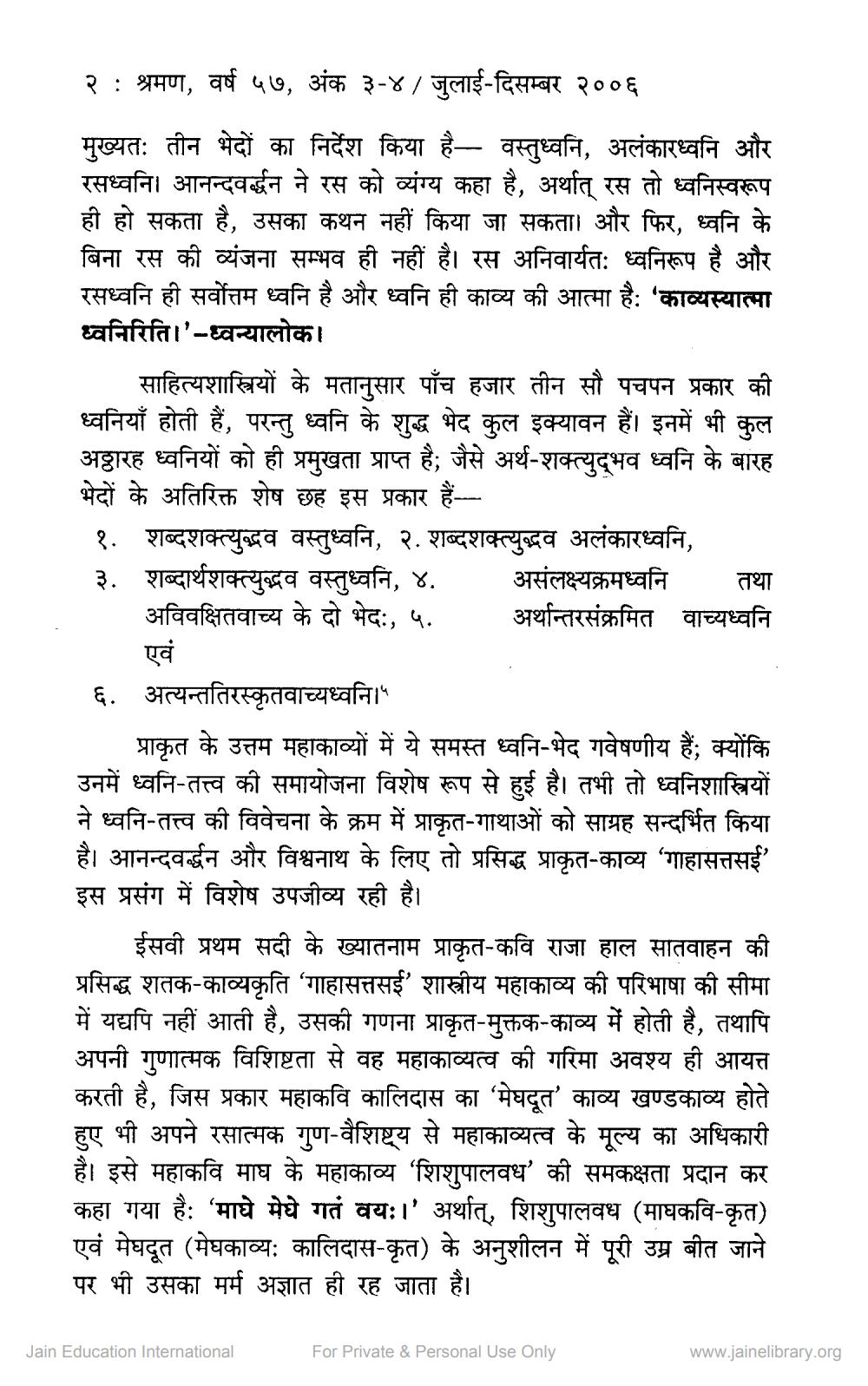________________
२ : श्रमण, वर्ष ५७, अंक ३-४ / जुलाई-दिसम्बर २००६
मुख्यतः तीन भेदों का निर्देश किया है- वस्तुध्वनि, अलंकारध्वनि और रसध्वनि। आनन्दवर्द्धन ने रस को व्यंग्य कहा है, अर्थात् रस तो ध्वनिस्वरूप ही हो सकता है, उसका कथन नहीं किया जा सकता। और फिर, ध्वनि के बिना रस की व्यंजना सम्भव ही नहीं है। रस अनिवार्यतः ध्वनिरूप है और रसध्वनि ही सर्वोत्तम ध्वनि है और ध्वनि ही काव्य की आत्मा है: 'काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति । ' - ध्वन्यालोक ।
साहित्यशास्त्रियों के मतानुसार पाँच हजार तीन सौ पचपन प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, परन्तु ध्वनि के शुद्ध भेद कुल इक्यावन हैं। इनमें भी कुल अठ्ठारह ध्वनियों को ही प्रमुखता प्राप्त है; जैसे अर्थ - शक्त्युद्भव ध्वनि के बारह भेदों के अतिरिक्त शेष छह इस प्रकार हैं---
१. शब्दशक्त्युद्भव वस्तुध्वनि, २. शब्दशक्त्युद्भव अलंकारध्वनि, ३. शब्दार्थशक्त्युद्भव वस्तुध्वनि, ४.
अविवक्षितवाच्य के दो भेदः,
एवं
६. अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि । ५
प्राकृत के उत्तम महाकाव्यों में ये समस्त ध्वनि-भेद गवेषणीय हैं; क्योंकि उनमें ध्वनि-तत्त्व की समायोजना विशेष रूप से हुई है। तभी तो ध्वनिशास्त्रियों ध्वनि-तत्त्व की विवेचना के क्रम में प्राकृत गाथाओं को साग्रह सन्दर्भित किया है। आनन्दवर्द्धन और विश्वनाथ के लिए तो प्रसिद्ध प्राकृत काव्य ' गाहासत्तसई' इस प्रसंग में विशेष उपजीव्य रही है।
तथा
असंलक्ष्यक्रमध्वनि अर्थान्तरसंक्रमित वाच्यध्वनि
ईसवी प्रथम सदी के ख्यातनाम प्राकृत - कवि राजा हाल सातवाहन की प्रसिद्ध शतक-काव्यकृति 'गाहासत्तसई' शास्त्रीय महाकाव्य की परिभाषा की सीमा में यद्यपि नहीं आती है, उसकी गणना प्राकृत- मुक्तक - काव्य में होती है, तथापि अपनी गुणात्मक विशिष्टता से वह महाकाव्यत्व की गरिमा अवश्य ही आयत्त करती है, जिस प्रकार महाकवि कालिदास का 'मेघदूत' काव्य खण्डकाव्य होते हुए भी अपने रसात्मक गुण - वैशिष्ट्य से महाकाव्यत्व के मूल्य का अधिकारी है। इसे महाकवि माघ के महाकाव्य 'शिशुपालवध' की समकक्षता प्रदान कर कहा गया है: 'माघे मेघे गतं वयः ।' अर्थात्, शिशुपालवध ( माघकवि-कृत) एवं मेघदूत (मेघकाव्यः कालिदास कृत) के अनुशीलन में पूरी उम्र बीत जाने पर भी उसका मर्म अज्ञात ही रह जाता है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org