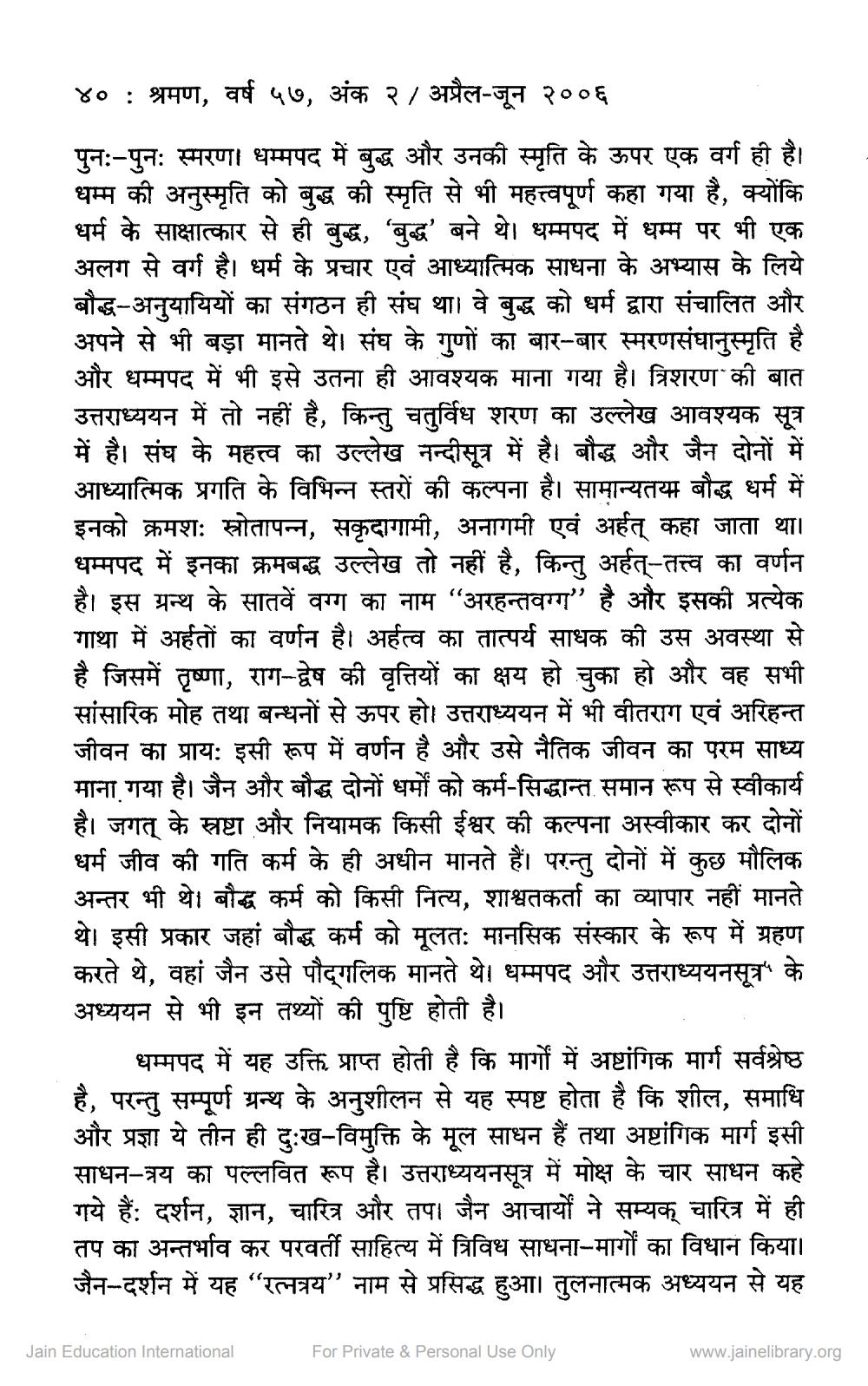________________
४० : श्रमण, वर्ष ५७, अंक २ / अप्रैल-जून २००६
पुनः - पुनः स्मरण । धम्मपद में बुद्ध और उनकी स्मृति के ऊपर एक वर्ग ही है। धम्म की अनुस्मृति को बुद्ध की स्मृति से भी महत्त्वपूर्ण कहा गया है, क्योंकि धर्म के साक्षात्कार से ही बुद्ध, 'बुद्ध' बने थे। धम्मपद में धम्म पर भी एक अलग से वर्ग है। धर्म के प्रचार एवं आध्यात्मिक साधना के अभ्यास के लिये बौद्ध अनुयायियों का संगठन ही संघ था। वे बुद्ध को धर्म द्वारा संचालित और अपने से भी बड़ा मानते थे। संघ के गुणों का बार-बार स्मरणसंघानुस्मृति है और धम्मपद में भी इसे उतना ही आवश्यक माना गया है। त्रिशरण की बात उत्तराध्ययन में तो नहीं है, किन्तु चतुर्विध शरण का उल्लेख आवश्यक सूत्र में है। संघ के महत्त्व का उल्लेख नन्दीसूत्र में है। बौद्ध और जैन दोनों में आध्यात्मिक प्रगति के विभिन्न स्तरों की कल्पना है। सामान्यतया बौद्ध धर्म में इनको क्रमशः स्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागमी एवं अर्हत् कहा जाता था। धम्मपद में इनका क्रमबद्ध उल्लेख तो नहीं है, किन्तु अर्हत्-तत्त्व का वर्णन है । इस ग्रन्थ के सातवें वग्ग का नाम " अरहन्तवग्ग" है और इसकी प्रत्येक गाथा में अर्हतों का वर्णन है । अर्हत्व का तात्पर्य साधक की उस अवस्था से है जिसमें तृष्णा, राग-द्वेष की वृत्तियों का क्षय हो चुका हो और वह सभी सांसारिक मोह तथा बन्धनों से ऊपर हो । उत्तराध्ययन में भी वीतराग एवं अरिहन्त जीवन का प्रायः इसी रूप में वर्णन है और उसे नैतिक जीवन का परम साध्य माना गया है। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों को कर्म- सिद्धान्त समान रूप से स्वीकार्य है । जगत् के स्रष्टा और नियामक किसी ईश्वर की कल्पना अस्वीकार कर दोनों धर्म जीव की गति कर्म के ही अधीन मानते हैं। परन्तु दोनों में कुछ मौलिक अन्तर भी थे। बौद्ध कर्म को किसी नित्य, शाश्वतकर्ता का व्यापार नहीं मानते थे। इसी प्रकार जहां बौद्ध कर्म को मूलतः मानसिक संस्कार के रूप में ग्रहण करते थे, वहां जैन उसे पौद्गलिक मानते थे । धम्मपद और उत्तराध्ययनसूत्र' के अध्ययन से भी इन तथ्यों की पुष्टि होती है।
धम्मपद में यह उक्ति प्राप्त होती है कि मार्गों में अष्टांगिक मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, परन्तु सम्पूर्ण ग्रन्थ के अनुशीलन से यह स्पष्ट होता है कि शील, समाधि और प्रज्ञा ये तीन ही दुःख - विमुक्ति के मूल साधन हैं तथा अष्टांगिक मार्ग इसी साधन-त्रय का पल्लवित रूप है। उत्तराध्ययनसूत्र में मोक्ष के चार साधन कहे गये हैं: दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। जैन आचार्यों ने सम्यक् चारित्र में ही तप का अन्तर्भाव कर परवर्ती साहित्य में त्रिविध साधना - मार्गों का विधान किया। जैन-दर्शन में यह “रत्नत्रय" नाम से प्रसिद्ध हुआ। तुलनात्मक अध्ययन से यह
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org