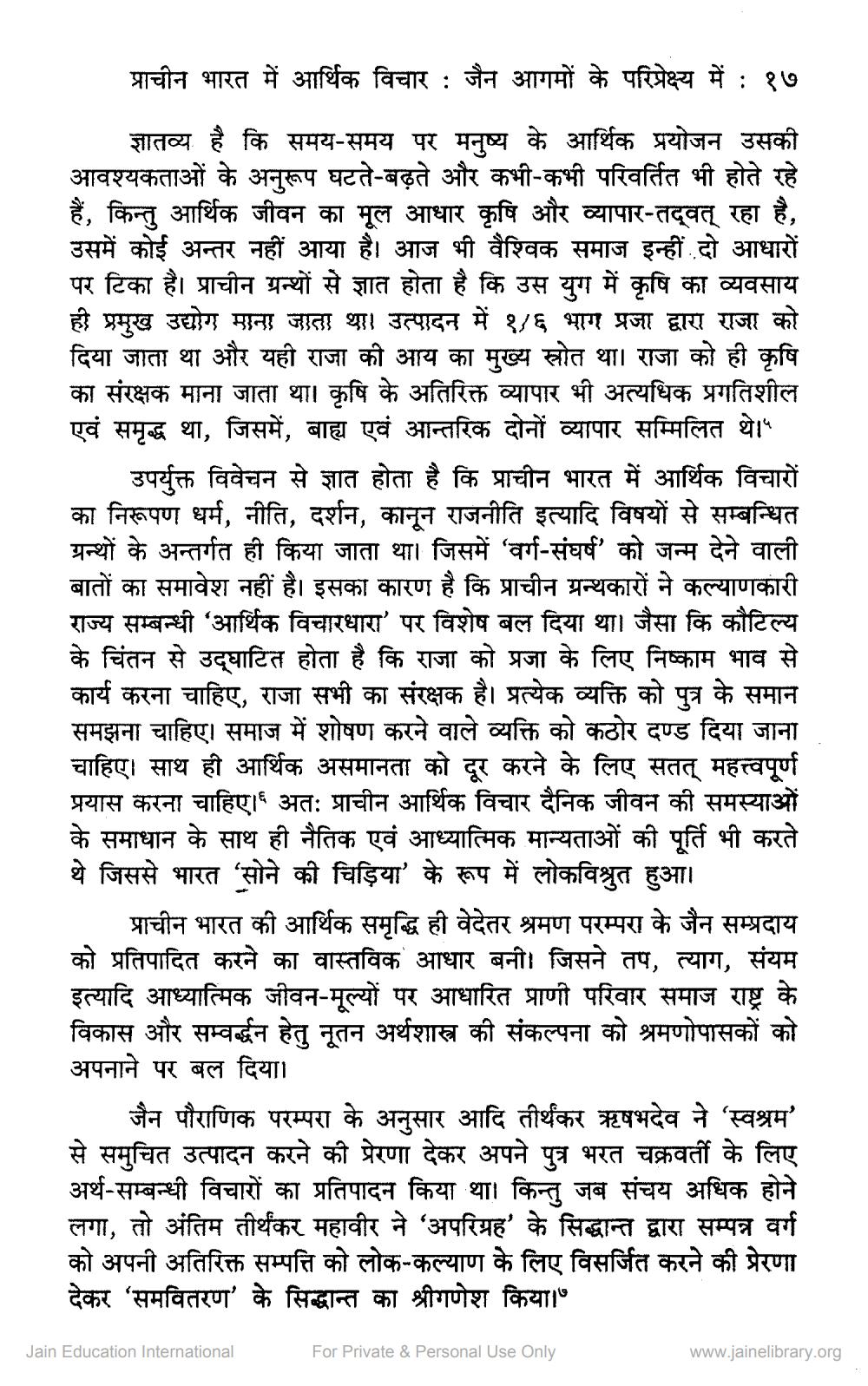________________
प्राचीन भारत में आर्थिक विचार : जैन आगमों के परिप्रेक्ष्य में : १७
ज्ञातव्य है कि समय-समय पर मनुष्य के आर्थिक प्रयोजन उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप घटते-बढ़ते और कभी-कभी परिवर्तित भी होते रहे हैं, किन्तु आर्थिक जीवन का मूल आधार कृषि और व्यापार-तद्वत् रहा है, उसमें कोई अन्तर नहीं आया है। आज भी वैश्विक समाज इन्हीं दो आधारों पर टिका है। प्राचीन ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि उस युग में कृषि का व्यवसाय ही प्रमुख उद्योग माना जाता था। उत्पादन में १/६ भाग प्रजा द्वारा राजा को दिया जाता था और यही राजा की आय का मुख्य स्रोत था। राजा को ही कृषि का संरक्षक माना जाता था। कृषि के अतिरिक्त व्यापार भी अत्यधिक प्रगतिशील एवं समृद्ध था, जिसमें, बाह्य एवं आन्तरिक दोनों व्यापार सम्मिलित थे।
उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में आर्थिक विचारों का निरूपण धर्म, नीति, दर्शन, कानून राजनीति इत्यादि विषयों से सम्बन्धित ग्रन्थों के अन्तर्गत ही किया जाता था। जिसमें 'वर्ग-संघर्ष' को जन्म देने वाली बातों का समावेश नहीं है। इसका कारण है कि प्राचीन ग्रन्थकारों ने कल्याणकारी राज्य सम्बन्धी 'आर्थिक विचारधारा' पर विशेष बल दिया था। जैसा कि कौटिल्य के चिंतन से उद्घाटित होता है कि राजा को प्रजा के लिए निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए, राजा सभी का संरक्षक है। प्रत्येक व्यक्ति को पुत्र के समान समझना चाहिए। समाज में शोषण करने वाले व्यक्ति को कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए। साथ ही आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए सतत् महत्त्वपूर्ण प्रयास करना चाहिए। अतः प्राचीन आर्थिक विचार दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान के साथ ही नैतिक एवं आध्यात्मिक मान्यताओं की पूर्ति भी करते थे जिससे भारत ‘सोने की चिड़िया' के रूप में लोकविश्रुत हुआ।
प्राचीन भारत की आर्थिक समृद्धि ही वेदेतर श्रमण परम्परा के जैन सम्प्रदाय को प्रतिपादित करने का वास्तविक आधार बनी। जिसने तप, त्याग, संयम इत्यादि आध्यात्मिक जीवन-मूल्यों पर आधारित प्राणी परिवार समाज राष्ट्र के विकास और सम्वर्द्धन हेतु नूतन अर्थशास्त्र की संकल्पना को श्रमणोपासकों को अपनाने पर बल दिया।
जैन पौराणिक परम्परा के अनुसार आदि तीर्थंकर ऋषभदेव ने 'स्वश्रम' से समुचित उत्पादन करने की प्रेरणा देकर अपने पुत्र भरत चक्रवर्ती के लिए अर्थ-सम्बन्धी विचारों का प्रतिपादन किया था। किन्तु जब संचय अधिक होने लगा, तो अंतिम तीर्थंकर महावीर ने 'अपरिग्रह' के सिद्धान्त द्वारा सम्पन्न वर्ग को अपनी अतिरिक्त सम्पत्ति को लोक-कल्याण के लिए विसर्जित करने की प्रेरणा देकर 'समवितरण' के सिद्धान्त का श्रीगणेश किया।"
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org