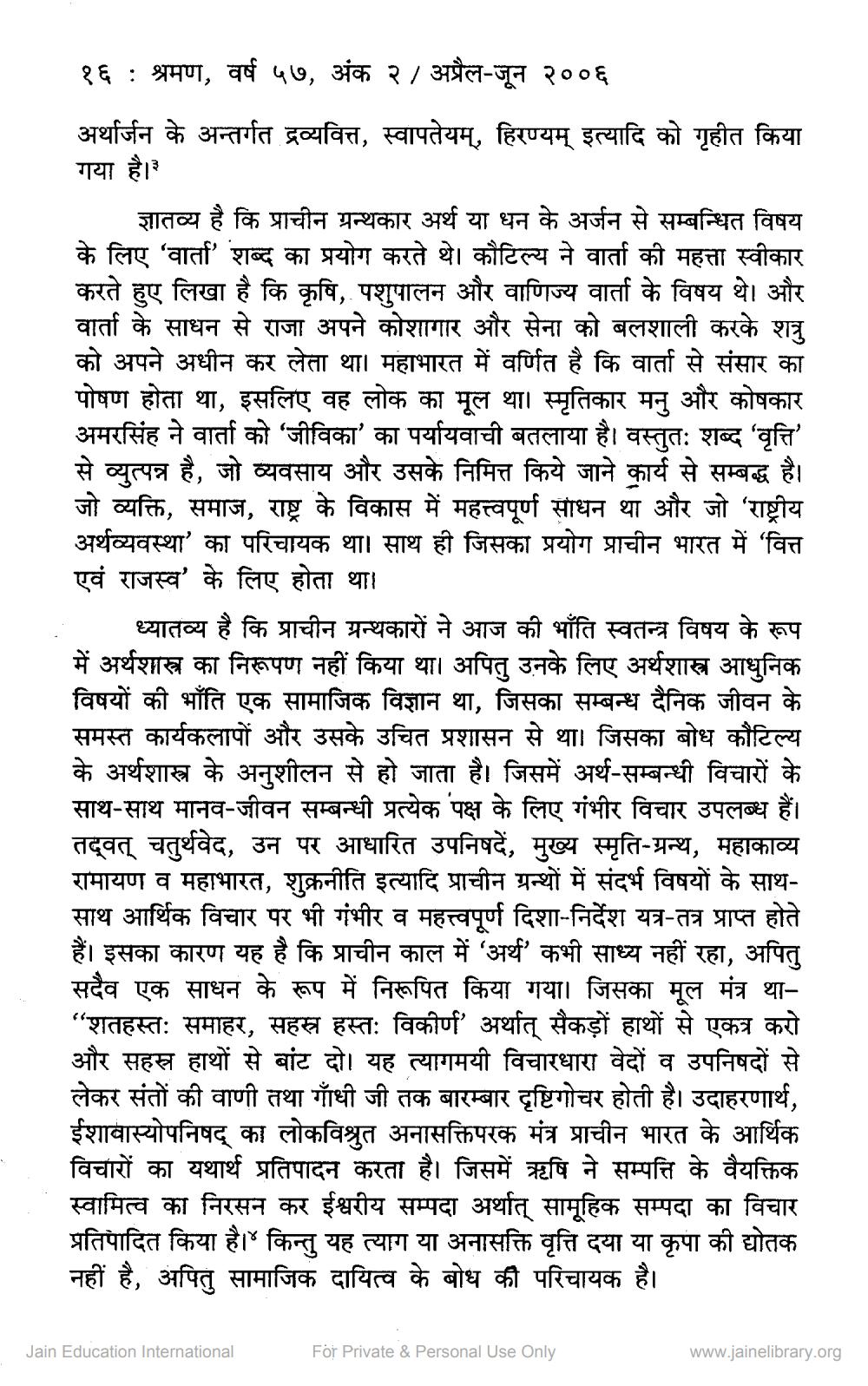________________
१६ : श्रमण, वर्ष ५७, अंक २ / अप्रैल-जून २००६ अर्थार्जन के अन्तर्गत द्रव्यवित्त, स्वापतेयम्, हिरण्यम् इत्यादि को गृहीत किया गया है।
ज्ञातव्य है कि प्राचीन ग्रन्थकार अर्थ या धन के अर्जन से सम्बन्धित विषय के लिए 'वार्ता' शब्द का प्रयोग करते थे। कौटिल्य ने वार्ता की महत्ता स्वीकार करते हुए लिखा है कि कृषि, पशुपालन और वाणिज्य वार्ता के विषय थे। और वार्ता के साधन से राजा अपने कोशागार और सेना को बलशाली करके शत्रु को अपने अधीन कर लेता था। महाभारत में वर्णित है कि वार्ता से संसार का पोषण होता था, इसलिए वह लोक का मूल था। स्मृतिकार मनु और कोषकार अमरसिंह ने वार्ता को 'जीविका' का पर्यायवाची बतलाया है। वस्तुतः शब्द 'वृत्ति' से व्युत्पन्न है, जो व्यवसाय और उसके निमित्त किये जाने कार्य से सम्बद्ध है। जो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के विकास में महत्त्वपूर्ण साधन था और जो 'राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था' का परिचायक था। साथ ही जिसका प्रयोग प्राचीन भारत में 'वित्त एवं राजस्व' के लिए होता था।
ध्यातव्य है कि प्राचीन ग्रन्थकारों ने आज की भाँति स्वतन्त्र विषय के रूप में अर्थशास्त्र का निरूपण नहीं किया था। अपितु उनके लिए अर्थशास्त्र आधुनिक विषयों की भाँति एक सामाजिक विज्ञान था, जिसका सम्बन्ध दैनिक जीवन के समस्त कार्यकलापों और उसके उचित प्रशासन से था। जिसका बोध कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुशीलन से हो जाता है। जिसमें अर्थ-सम्बन्धी विचारों के साथ-साथ मानव-जीवन सम्बन्धी प्रत्येक पक्ष के लिए गंभीर विचार उपलब्ध हैं। तद्वत् चतुर्थवेद, उन पर आधारित उपनिषदें, मुख्य स्मृति-ग्रन्थ, महाकाव्य रामायण व महाभारत, शुक्रनीति इत्यादि प्राचीन ग्रन्थों में संदर्भ विषयों के साथसाथ आर्थिक विचार पर भी गंभीर व महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश यत्र-तत्र प्राप्त होते हैं। इसका कारण यह है कि प्राचीन काल में 'अर्थ' कभी साध्य नहीं रहा, अपितु सदैव एक साधन के रूप में निरूपित किया गया। जिसका मूल मंत्र था"शतहस्त: समाहर, सहस्र हस्त: विकीर्ण' अर्थात् सैकड़ों हाथों से एकत्र करो और सहस्र हाथों से बांट दो। यह त्यागमयी विचारधारा वेदों व उपनिषदों से लेकर संतों की वाणी तथा गाँधी जी तक बारम्बार दृष्टिगोचर होती है। उदाहरणार्थ, ईशावास्योपनिषद् का लोकविश्रुत अनासक्तिपरक मंत्र प्राचीन भारत के आर्थिक विचारों का यथार्थ प्रतिपादन करता है। जिसमें ऋषि ने सम्पत्ति के वैयक्तिक स्वामित्व का निरसन कर ईश्वरीय सम्पदा अर्थात् सामूहिक सम्पदा का विचार प्रतिपादित किया है। किन्तु यह त्याग या अनासक्ति वृत्ति दया या कृपा की द्योतक नहीं है, अपितु सामाजिक दायित्व के बोध की परिचायक है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org